मेरी इन दिनों अपने एक साथी से बातचीत हुई, वे इन दिनों काफी सारी किताबें पढ़ रही है। ये किताबे उसके जीवन मे एक ख़ास जगह बनाने की कोशिश मे है। अपने हर दिन मे घर और परिवार के बीच रहकर भी जो समझ ताज़ा होती है उसके बाद भी हमारे दर्मियाँ वो अहसास छुपा रह जाता है जिसको उन्ही रिश्तों के बीच मे हम तालशते हैं। वे क्या है? परिवार जो अपने बनाये कारणों के तहत ही किसी भी रिश्ते अथवा परिवार के सदस्य को सोचता है। वे बेहद ठोस होता है। जिसमे अपने लिए जगह बनाना किसी ना दिखने वाली लड़ाई की ही तरह से होता है। मगर किताबें उस अहसास मे अपनी जगह बना लेती है।
हर किताब अपने साथ कई तरह की तलाश लिए चलती है। जिसमे जुड़ने वाला हर अनुभव उसमे अपने को महसूस करने के कोने तलाश्ता है। वो तलाश कभी तो उसमे उभरने वाले सवाल बनती है तो कभी अपने मनमुताबिक कल्पना करके जगह बना लेती है।
किताबों ने उसको खुद को समझने अथवा अपने जीने के तरीको से बहस करने का मौका प्रदान किया है। उसकी बातों मे किसी खास हलचल को महसूस किया जा सकता है। बदलाव, खाली बदलाव ही नहीं होता। यानि के कुछ हटा और कुछ आया, इसको सोचने के अलावा ये सोचा जा सकता है कि कुछ तब्दील हो गया।
ये "तब्दील" शब्द हमारे सोचने के चश्मों को एक नया मौड़ और ढाँचा देता है। बहुत सारी बुनियादी बातों के और परिवार के बीच मे कारणों के बाद उसकी शारीरिक भाषा मे एक ऐसी ही तब्दीली महसूस होती है।
वे कहती है, “हमारे सामने आज भी वही शख़्स चल-घूम रहे हैं जो पहले भी चलते थे। कोई हमारे से टकरा जाता था तो कभी कोई बिना बात के मुस्कुराकर भी चला जाता था। कोई दूर खड़ा देखता रहता था तो कोई पास आकर कुछ कहने की कोशिश करता था। कोई इशारों की ज़ुबाने मे कुछ कहने की कोशिश करता था तो कोई नज़र छुपाकर निकलता था। कोई हमारे लिए रास्ता बनाता था तो कोई ऐसे विहेव करता था कि वो दुनिया मे अकेला है। ये हमारे समाने निरंतण चलते रहते हैं। ये वे चित्र हैं जिनको हम याद भी रख सकते हैं और भूल भी सकते हैं। मगर, हमारे ऐसा करने या करने से इन्हे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो इन्ही रास्तों मे दोबारा से मिलेगें। चाहें आप देखो या ना देखो। क्या हमें आज भी कुछ पता है इस बैचेनी या कंपन के बारे में कि ये अपने इस स्वभाव मे क्या लिए चल रहे हैं?”
वे बेहद आसानी से अपने देखे, सुने या महसूस किये अहसास को दोहरा जाती है। एक पल के लिए नहीं सोचती की व इस दुनिया मे क्या और कैसा सवाल बना रही है। जो चित्र खाली इन रास्तों पर या तो नज़ायज़ माने जाते हैं या फिर देखकर अंदेखे किये जाते हैं वे हमारे लिए क्या सवाल बन सकते हैं? ये हमारे लिए क्या कोई शब्द बनाते हैं? मैंने उसकी बातों को सोचना पहले तो जरूरी नहीं समझा, सोचा ये तो लड़कियों के साथ मे रोजाना होता होगा, इसमे मेरे लिए क्या है? मैं क्या कोई कदम उठाऊ? लेकिन क्या होगा, क्या मैं कोई झंडा लिए शहर को सुधारने निकला हूँ क्या? मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो क्या करूँ? फिर जब अपने आसपास को दोहरा ने की कोशिश की तो कुछ चित्र ऐसे उभरे जो मैं रोजाना अपने किसी हिस्से मे ढ़ालने की कोशिश करता हूँ। वे मेरे सोचने और लिखने के माध्यम मे बसे हैं। इनको कैसे मैं हटा सकता हूँ? कुछ ऐसे सवाल बनकर सामने आते हैं जो कुछ शब्दों को सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। जैसे, किसी की कंपन को लिखना या सोचना या फिर दोहराना या बख़ान करना या खुद के लिए लेना ये कैसे पोसिबल होता है? इसकी इंद्रियाँ क्या है?
हम अपनी ज़िंदगी से क्या मेल करवाते हैं किसी जीवन को या जीने के तरीके को?
ये कहना बहुत ही आसान होता है कि ये दोहराया जा सकता है और ये दोहराने के तरीके है। पर हम किसी ज़िंदगी को दोहरा रहे हैं ये होता है या हमारे साथ उसका कोई रिश्ता बन गया होता है? हम उस रिश्ते को दोहराते हैं या फिर उस रिश्ते से दोहराते हैं? ये दोनों क्या है?
हम अपने दोहराये गए का अनालाइस ही नहीं कर सकतें। क्योंकि दोहराये मे किसी जीवन का पूरा अहसास शामिल है। जो सांस लेता है, जीता है, रोता है, ठहरता है, कभी-कभी गाता भी है तो कभी-कभी गुस्सा भी होता है। ये खाली एक ऐसा पहलू नहीं है कि उसे एक आत्मनिर्भर करके ही बताया जा सकें। वो अगर ज़ुबान पर आ गया है तो उसका नाता शायद बन गया है। उसी से वो रूप पाता है। नहीं तो उसी किसी ज़ुबान से रूप पाने की क्या चेष्टा।
हमारे लिए किसी का रूप क्या है और उसके साथ हमारा रिश्ता क्या है? मैं मानता हूँ ये तो मौके और जीवन अथवा सोचने के ऊपर निर्भर करता है लेकिन कुछ तो होता ऐसा जो रूपक हो हमारे लिए?
किसी कहानी को पढ़ना अथवा किसी जीवन को पढ़ना जो हमारे सामने सांस लेता है, डरता है, ताकतवर है उसके और मेरे बीच की ठहरी या फिसलती बातचीत मे बहुत सी चीजें बड़ी तेजी से निकल जाती हैं। जिनको शायद पकड़ना बेहद मुश्किल होता है, कुछ ऐसा भी होता है जो उसकी ज़िन्दगी का बहुत डरा देने वाला पल होता है जिसे पकड़ भी लिया तो छोड़ देना होता है।
हमारे सामने कोई कुछ पल के लिए अपनी यातनाओ और कामनाओ को रख कर चला गया। कुछ समय फिसला और कुछ पकड़ मे आ गया। लेकिन सब कुछ क्या मेरे लिए ही था, जो गया उसको हम कैसे पकड़े। उसको कैसे पढ़े? उसकी इंद्रियाँ क्या होगी?
ये तब्दीली का दौर चलता रहता है। मेरी दोस्त से मुलाकातों मे कुछ ऐसी ही तब्दीलियाँ उभरती हैं। क्या इस सोच को समझना हमारे लिए कुछ संभावनायें छोड़ता है। ये रुका सा महसूस होता है। इससे बाहर कैसे निकला जाये?
लख्मी
Tuesday, January 27, 2009
दरवाजे के बाहर नज़ारे
नीचे वाली सिढ़ियों से ही गीतों की तेज आवाजें आनी शुरू हो गई थी। लगता था की चार से पाँच जनों की पूरी टोली है। सबसे तेज आवाज़ हारमोनियम और ढोलक की थी। साथ ही साथ औरतों के तेज गीतों की। गला भर्राया हुआ सा मालुम हो रहा था। गीत कौन सा गाया जा रहा है वे समझ में नहीं आ रहा था। मगर तेज संगीत की धूनों के कारण उस आवाज़ में भी मधुरता के कण सुनाई पड़ रहे थे। कभी खाली संगीत ही सुनाई पड़ता तो कभी खाली गीत ही सिढ़ियों से ऊपर चले आते। ढोलक की हर थाप पर घूंघरूओ की आवाज़ भी उस भर्राई आवाज़ का साथ देती हुई चली आती।
वे सभी गीत-संगीत अभी के लिए नीचे वाले घर में ही रुक गए थे। वहीं पर आवाज़ घूम रही थी। ये एक बहुत ही टूटी सी बिल्डिंग है, सरकारी क्वॉटरों की। अस्पताल में काम करने वालो को दी गई थी। चार मन्जिल और सिढ़ियाँ कमबांइड बड़ी और चौड़ी। जिनपर कभी तो साड़ी बैचने वाले, तो कभी बच्चो का चूरन बैचने वाले घुसे चले आते हैं और आज ये मिरासियों कि महफ़िल, टोली समीत यहाँ की बेजान दीवारों में गीतों की वर्णमाला डालने चले आये थी। गीतों में बिखरते शब्द बस, गुहार ही थे। उसके साथ में मनोंरजन की बहार भी।
सिढ़ियों से ही वे लोग नज़र आ रहे थे। ऊपरी मन्जिला में रहने वाले लोग सिढ़ियों पर खड़े होकर देखने की कोशिश करते कि आखिर ये माज़रा क्या है कि चित्रहार सिढ़ियों में अपनी बहार लगाये है। लोगों का झुंड सिढ़ियों की मुंडेरियों पर जम गया था। लोग इस तरह से मुंडेरियों पर लटके थे की नज़ारा पूरा आँखों में उतर जाये। 'कहीं कोई नाच तो नहीं रहा, कोई ठुमक तो नहीं रहा, कोई थिरक तो नहीं रहा।' आखिर में इस मनोंरजन का भी मजा क्यों ना लिया जाये। ऐसा मौका बार-बार थोड़ी मिलता है। इसलिए आँखे बिना नीचे आये वहीं से देखना चाहती थी।
वैसे यहाँ के लोग बेहद इन्टेलिजेन्ट हैं, भीड़ करने पर विश्वास नहीं रखते। भीड़ में शामिल होने पर भी। ये लोग हाईसोइटी के जो हैं। बन्द कमरों मे रहना, हमेशा दरवाजा बन्द करके, जहाँ पर दरवाजे की घंटी का काम दिखाई देता है। अगर पड़ोस के घर में कुछ हो रहा हो तो ये बिना बुलाये देखने भी नहीं जाते। सामने वाले घर में कोई नाच भी रहा है तो अपने घर की किचन की खिड़की से सब कुछ देख लेगें लेकिन वहाँ उस माहौल में हिस्सेदारी नहीं दिखाते। ऐसा करने से सोइयटी थोड़ी फीकी पड़ जायेगी। यहाँ पर भी उस महफ़िल में बस, अपने दरवाजे से ही देखना चाहते थे। वहीं पर खड़े सब कुछ पाना चाहते थे। नहीं तो वापस अपने बन्द दरवाजो में खाली आवाज़ सुनकर ही जी लेगें और अगर इनको पता चल जाये की जो महफ़िल नीचे वाले घर के सामने लगी है वो थोड़ी देर में इनके दरवाजे पर भी होगी तो बस, चेहरे के भाव ही बदल जाते हैं। उसके बाद तो शरीर की भाषा में ऐसी हलचल आ जाती है की, ये सब इनके लिए बेकार का ड्रिरामा लगने लगता है और ज़ुबान पर होता है कि "ऐसा तो हम रोज़ ही देखते है।" अब चाहें उस महफ़िल में कोई भी गीत गुनगुनाया जा रहा हो वे सब पहले की ही प्रेमगाथा बनकर रह जाती है। चाहें उसमे नये शब्द हो या नये अन्दाज़, सब के सब पुराने किलों की तरह जम जाते हैं।
चलों, यहाँ तो दुआ से अभी ऐसा कुछ नहीं था। टोली का काम नीचे के दरवाजे से ख़त्म हो गया था। अब वो अपने मे गुनगुनाते हुए ऊपर की सिढ़ियाँ चड़ रहे थे। हारमोनियम और ढोलक की थाप दोनों एक साथ में चली आ रही थी और उनके साथ में गीतों में मचलती आवाज़े झूम रही थी। घूंघरू की हलचल अभी के लिए रुक गई थी। दूसरी मन्जिल कमरा नम्बर 135 का उन्होनें दरवाजा खटखटाया, वैसे तो गीतों की आवाज़ों से पूरी बिल्डिंग चौकन्नी हो गई थी। बस, खटखटाना इसलिए जरूरी था कि जो गीत इस वक़्त में गाया जा रहा है वो किसके नाम पर सपूत है? दरवाजे पर जैसे ही खट-खट हुई तो बाहर खड़े उन सभी के शरीर में जैसे बिजली सी उतर आई हो। गीतों की आवाज़ से लेकर संगीत की धून तक सभी में तेजी उतर आई थी। ढोलक की एक थाप लगी और गीत उस भर्राई आवाज़ में तैर गया।
दरवाजे पर एक लड़की थी, वो इन पाँचो जनो को देखकर वहीं पर खड़ी अपने घरवालो को आवाज़ लगाने लगी। उसकी आवाज़ भी बाहर में गाये जा रहे गीतों की आवाज़ों में खो गई थी। मगर, घर की दीवारों ने उसकी आवाज़ को ज़्यादा वज़नदार बना दिया था। अन्दर घर में से एक आदमी बाहर आकर खड़ा हो गया और उन्हे देखने लगा। उनके सामने पाँच जने थे। एक के गले मे हारमोनियम लटका था तो दूसरे के गले में ढोलक टंगी थी। दोनों के मुँह में लाल रंग की लाली छलक रही थी। माथे पर काले रंग का बड़ा सा टीका लगा था और हाथ अपना काम बड़ी बेफिक्री से कर रहे थे। खाकी कुर्ते में दोनों एक ही कंपनी के मुलाजिम लग रहे थे और सबसे आगे ख़डी थी तीन औरतें। तीनों ने घाघरा चौली पहना था अलग-अलग रंग का मगर तीनों मे ही छोटे-छोटे शीसे जड़े थे। एक औरत ने अपने शरीर पर सफेद रंग का दुसाला डाला हुआ था और दूसरी ने अपने गले मे एक थैला लटकाया था और हाथों मे घूघंरू लेकर बजा रही थी। दुसाला ओड़े औरत अपनी बड़ी मोटी और भर्राई आवाज़ में गीत गा रही थी। इन तीनों में से तीसरी की उम्र थोड़ी कम थी। उसने गुलाबी रंग का घाघरा चौली पहना था जो बेहद चमक रहा था। उसी ने अपने पाँव मे घूंघरू पहने थे। जो बस, बीच-बीच में थाप के साथ में उछल पड़ती थी। उसी को देखने के लिए सिढ़ियों की मुंडेरी पर भीड़ लटक रही थी।
गीत गा रही वो मोटी भर्राई आवाज़ वाली औरत के माथे पर काले रंग की मोटी सी बिन्दी लगी थी। उसका चेहरा बेहद भारी व बड़ा था। उसके चेहरे पर कई रंगो का मेकप था। आँखों की आईब्रों से लेकर कानो तक लाल और सफेद रंग की छोटी-छोटी बिन्दियाँ बनी हुई थी। गाल और ठोडी पर काले रंग की तीन एक साथ बिन्दियाँ बनी थी। आँखों मे काला और ये भारी काज़ल भरा हुआ था जिसके कारण उसकी आँखें लाल हो चली थी। नाक मे भारी व मोटी नथ थी और कान मे बड़े-बड़े पीतल के कुंडल थे। गले मे मेटल का भारी सा हार था। हाथों मे कलाइओ से लेकर कांधे तक उसने बाजूबन्द पहने हुए थे। वे उस लिबास मे बेहद भारी लग रही थी। उसके साथ-साथ उसकी आवाज़ उसके उस रूप को और भी मजबूत बना रही थी। किसी भी गीत को उसकी आवाज़ मे सुनने का मतलब था की कभी ना भूलाया जायेगा। अगर गीत याद न रहा तो ये बात तय रहेगी कि उसका चेहरा और रूप कभी दीमाग से ओझल नहीं होगा। उसी से ये वक़्त और महफ़िल यादों में किसी खूटी से टंगा रह जायेगा।
उन्होनें अपने गीत में मकान मालिक का नाम दोहराते हुए उन्हे खुश करने की कोशिश की। मकान मालिक अपना नाम उनके गीत मे सुनकर चौंक से गए। 'उनके गीत में मेरा नाम कैसे आया?' इस टोली ने इतना बेहतरीन माहौल बना दिया था कि उन्हे ये तक याद ना रहा था कि उनका नाम उनके ही दरवाजे पर लटकी तख़्ती पर लिखा है।
“राजा राम जी सवारी पँहुची रे इंद्रलोक"
जिनको लगा मीठे लठ्ठुओ भोग।
राजाराम मकान मालिक का ही नाम था। वे उनकी तरफ़ मे चौंकते हुए देखने लगे। राजाराम जी पंत अस्पताल मे ही काम करते हैं। वे वहाँ वॉडबॉय हैं। हालाँकि अब उनकी उम्र बॉय की नहीं रही। चवालिस साल के हो गए हैं। उन्हे वैसे इन गीतों मे बेहद मज़ा आता है। वे उनकी तरफ में देखकर मुस्कुराये और उन्हे घर मे बुलाने का फैसला लिया। वहीं दरवाजे पर बैठने का इशारा करते हुए वे अन्दर चले गए। मंडली ने उनका इशारा पाया और वहीं चौखट पर ही बैठ गई। बस, माहौल में इस वक़्त मद्धम हारमोनियम कि ही आवाज़ आ रही थी वो भी खाली एक ही हाथ चल रहा था। हारमोनियम की आवाज़ जैसे इस वक़्त माहौल को पम्प कर रही थी। कमरा उसी आवाज़ मे इतना सुहाना बन गया था कि जैसे सफ़र मे हो और विविधभारती चल रहा हो। कमरे मे केवड़े अथवा मुगरे के फूलों की महक भर गई थी। पाँचो टोली के लोग वहीं चौखट पर ही बैठने की अजेस्टमेन्ट कर रहे थे। राजाराम जी अन्दर कमरे में से पानी का जग भर कर बाहर आये और उनकी तरफ मे देखकर मुस्कुराने लगे। उनके चेहरे पर एक चमक थी। सबको पानी पिलाया और वहीं उनके साथ में लगे सोफे पर बैठ गए। उनकी बीवी और उनकी तीनों बेटियाँ उनके साथ मे ही आकर बैठ गई थी। टोली की आँखें इस समय मे पूरे कमरे में घूम रही थी। कभी कमरे में घूमती तो कभी सामने बैठे इस घर के मालिकों पर।
“अरे आप तो चुप हो गए, कोई गीत सुनाइये।" उनकी बीवी ने कहा।
“कौणसा गीत सुनना है थारे को, बीन्दड़ी।"
“अपने जी ने अनुसार कोई सा भी सुना दो।"
उन्होनें पीछे बैठे हारमोनियम वाले से कुछ आँखों में इशारा किया और हारमोनियम की धून शुरू हो गई। साथ में बैठी मे वो गुलाबी घाघरे वाली लड़की खड़ी हो गई और एक बार फिर से उस भर्राई आवाज़ मे कोई बेहद तड़कता लोकगीत बाहर आने लगा। इसमे उसके शब्दों को जानना या समझना कोई जरूरी नहीं था। पहली चार लाइन बेहद धीमे थी। जैसे ही उन लाइनों मे हल्की की रुकावट आई तो बस, ढोलक की दनादन थाप लगनी शुरू हो गई। यहाँ पर थाप लगी और वहाँ वो गुलाबी घाघरे वाली लड़की के पाँव जमीन में दबादब पड़ने लगे। वे वहीं पर हल्का-हल्का घूम रही थी। जब वो घूमती तो लगता जैसे उसके घाघरे का झोल भी उसके साथ में थिरक रहा है। गीत के साथ-साथ मे उसके होंठ हिल रहे थे। वो घूमती -घूमती राजाराम जी के किचन मे चली जाती और फिर बाहर आ जाती। वो तो बस, थाप पर दबादब कूद रही थी और बार-बार घूम जाती, अपनी चुनरी को अपने हाथों से कभी तो दायें तो कभी बायें करती, फिर घूम जाती, कभी घूमती-घूमती बैठती और फिर झटके से खड़ी हो जाती, फिर से अपनी चुनरी को पकड़ घूम जाती।
उनकी चौखट तो अब तक भर चुकी थी, देखने वालो की भीड़ दरवाजे पर जमा हो गई थी। सभी अवधारणाये तोड़कर लोग राजाराम जी की चौखट पर खड़े महफ़िल का आन्नद ले रहे थे। सभी मे उचक-उचक कर देखने की लालसा नज़र आ रही थी। आँखें जिसे खोज रही थी वो तो किचन में नाच रही थी। गीत में लय और संगीत में कसक इतनी जोरदार थी कि पाँव अपने आप जमीन से उठने लगते। ये नाच सभी में क्यों आ रहा था? ये सवाल बहुत बड़ा अथवा गहरा था। मगर इस हालात में किसी भी सवाल को सोचने का मतलब था की आप महफ़िल की मदहोशी से बेहयाई कर रहे हैं।
गीत काफी लंबा था, गाने और संगीत बजाने वालों के चेहरे पर पानी की बूंदे छलक आई थी। वो घूंघरू बजाने वाली के हाथ सुर्ख लाल हो गए थे। इतने मे एक बहुत ही मोटी आवाज़ में गीत शुरू हुआ। ये आवाज़ उन टोली मे से किसी की नहीं थी। वे आवाज़ राजाराम जी की थी, जो आज अपनी ही धुन में थी। पानी का ग्लास हाथ में पकड़े राजाराम जी बेहद मदहोश थे। दरवाजें पर खड़े सभी लोग मुस्कुरा रहे थे। उनकी बेटी बहुत खुश थी। राजाराम जी उस मोटी भर्राई आवाज़ वाली औरत के मुँह की तरफ देखते हुए गीत गा रहे थे। चेहरे पर गीत के साथ मे चलते भाव थे। कभी मुस्कुराहट के तो कभी कहीं खो जाने वाले, अपनी आँखें बन्द करके वो एक लम्बी लय को अपने मुँह मे छेड़ जाते।
ढोलक की थाप उसी तरह से बज रही थी जैसे अभी तक बुदबुदा रही थी। माहौल में इस जरा से बदलाव से रोमांच और बड़ गया था। अब टक्कर बराबर की थी। एक ऐसी टक्कर जो बेहद लज़ीज़ थी।
राजाराम जी कैसे इस अस्पताल की लाइन में आ गए थे ये सोचना नगवारा था। इससे पहले वे कई महफ़िल की शान से कम नहीं थे। अपने चार दोस्तों के साथ मे ये निकले थे लड़को और लड़कियों मे कला भरने। मगर खाली वे गीत जिनको कोई गाता नहीं हैं, कोई उनके पीछे दीवाना नहीं है। वे गीत कहाँ है? ये भी पूछना किसी के लिए जरूरी नहीं होता। अपनी इसी धून से निकलने के बाद मे ये इसी अस्पताल मे डेलीवेज़ का काम किया करते थे। जो कभी होता तो कभी नहीं होता था। जगंलो मे जाकर अपने गीतों को बहुत तेज़ आवाज़ में गाया करते थे। जहाँ पर लोग बड़ी जोर-जोर से हँसते थे वहाँ पर ये अपने गीतों मे खोते थे। इनका रिश्ता गीतों के साथ बिलकुल ऐसा ही था जैसे साल के एक महिने मे सपेरे अपने साँपो को आज़ाद छोड़ देते हैं कभी उनकी ख़बर नहीं लेते उसके बाद मे उन्हे दोबारा पकड़ते हैं, जहाँ पर छोड़ा था वहीं पर जाते है। लेकिन वो वहाँ नहीं मिलते।
यही इनका हाल था, अपने काम और उसकी टेंशन से जैसे ही बाहर आते तो बस, कहीं गायब हो जाते। किसी को नहीं मिलते। ये उन दिनों मे खोते, गायब होते और फिर से उस दौर मे पँहुच जाते जहाँ से इन्होनें खुद को निकाला था। ये होना खाली काम और समाजिक ज़िन्दगी मे ही कायम था, कला के साथ मे इसका रिश्ता डगमगाया था।
आज जैसे फिर से वो महिना था जिसमे इन्होनें खुद को आज़ाद छोड़ दिया था। उनकी लड़की उस गुलाबी घाघरे वाली लड़की के साथ मे नाच रही थी। कभी उसकी मुद्रा के साथ मे अपने शरीर को ढाल लेती तो कभी उससे कोसो दूर हो जाती। ये सिलसिला जारी था। राजाराम जी के लिए ये दौर किसी भी अवधारणा से कसा हुआ नहीं था।
जो कदम बाहर दरवाजे पर खड़े उनको निहार रहे थे वे कमरे मे आ गए थे। उनके गीतों मे कोई बीते सवाल का घेरा नहीं था। बस, माहौल मे कैसे उस लज़ीज़ स्वाद को बरकरार रखा जा सकता है वे था। उनकी बीवी तो बस, ये सोच रही थी कि अब पड़ोस मे होती बातों को कैसे समझेगी? कैसे लोगों को ये बतायेगी की उनके पति में ये कहाँ से और कैसे आया?
ये दौर ना जाने कितने तरह के भाव चेहरे पर बना रहा था और राजाराम जी का वो गीत ख़त्म ही नहीं हो रहा था। शायद यहाँ कोई चाहता भी नहीं था की वो कभी ख़त्म भी हो।
लख्मी
वे सभी गीत-संगीत अभी के लिए नीचे वाले घर में ही रुक गए थे। वहीं पर आवाज़ घूम रही थी। ये एक बहुत ही टूटी सी बिल्डिंग है, सरकारी क्वॉटरों की। अस्पताल में काम करने वालो को दी गई थी। चार मन्जिल और सिढ़ियाँ कमबांइड बड़ी और चौड़ी। जिनपर कभी तो साड़ी बैचने वाले, तो कभी बच्चो का चूरन बैचने वाले घुसे चले आते हैं और आज ये मिरासियों कि महफ़िल, टोली समीत यहाँ की बेजान दीवारों में गीतों की वर्णमाला डालने चले आये थी। गीतों में बिखरते शब्द बस, गुहार ही थे। उसके साथ में मनोंरजन की बहार भी।
सिढ़ियों से ही वे लोग नज़र आ रहे थे। ऊपरी मन्जिला में रहने वाले लोग सिढ़ियों पर खड़े होकर देखने की कोशिश करते कि आखिर ये माज़रा क्या है कि चित्रहार सिढ़ियों में अपनी बहार लगाये है। लोगों का झुंड सिढ़ियों की मुंडेरियों पर जम गया था। लोग इस तरह से मुंडेरियों पर लटके थे की नज़ारा पूरा आँखों में उतर जाये। 'कहीं कोई नाच तो नहीं रहा, कोई ठुमक तो नहीं रहा, कोई थिरक तो नहीं रहा।' आखिर में इस मनोंरजन का भी मजा क्यों ना लिया जाये। ऐसा मौका बार-बार थोड़ी मिलता है। इसलिए आँखे बिना नीचे आये वहीं से देखना चाहती थी।
वैसे यहाँ के लोग बेहद इन्टेलिजेन्ट हैं, भीड़ करने पर विश्वास नहीं रखते। भीड़ में शामिल होने पर भी। ये लोग हाईसोइटी के जो हैं। बन्द कमरों मे रहना, हमेशा दरवाजा बन्द करके, जहाँ पर दरवाजे की घंटी का काम दिखाई देता है। अगर पड़ोस के घर में कुछ हो रहा हो तो ये बिना बुलाये देखने भी नहीं जाते। सामने वाले घर में कोई नाच भी रहा है तो अपने घर की किचन की खिड़की से सब कुछ देख लेगें लेकिन वहाँ उस माहौल में हिस्सेदारी नहीं दिखाते। ऐसा करने से सोइयटी थोड़ी फीकी पड़ जायेगी। यहाँ पर भी उस महफ़िल में बस, अपने दरवाजे से ही देखना चाहते थे। वहीं पर खड़े सब कुछ पाना चाहते थे। नहीं तो वापस अपने बन्द दरवाजो में खाली आवाज़ सुनकर ही जी लेगें और अगर इनको पता चल जाये की जो महफ़िल नीचे वाले घर के सामने लगी है वो थोड़ी देर में इनके दरवाजे पर भी होगी तो बस, चेहरे के भाव ही बदल जाते हैं। उसके बाद तो शरीर की भाषा में ऐसी हलचल आ जाती है की, ये सब इनके लिए बेकार का ड्रिरामा लगने लगता है और ज़ुबान पर होता है कि "ऐसा तो हम रोज़ ही देखते है।" अब चाहें उस महफ़िल में कोई भी गीत गुनगुनाया जा रहा हो वे सब पहले की ही प्रेमगाथा बनकर रह जाती है। चाहें उसमे नये शब्द हो या नये अन्दाज़, सब के सब पुराने किलों की तरह जम जाते हैं।
चलों, यहाँ तो दुआ से अभी ऐसा कुछ नहीं था। टोली का काम नीचे के दरवाजे से ख़त्म हो गया था। अब वो अपने मे गुनगुनाते हुए ऊपर की सिढ़ियाँ चड़ रहे थे। हारमोनियम और ढोलक की थाप दोनों एक साथ में चली आ रही थी और उनके साथ में गीतों में मचलती आवाज़े झूम रही थी। घूंघरू की हलचल अभी के लिए रुक गई थी। दूसरी मन्जिल कमरा नम्बर 135 का उन्होनें दरवाजा खटखटाया, वैसे तो गीतों की आवाज़ों से पूरी बिल्डिंग चौकन्नी हो गई थी। बस, खटखटाना इसलिए जरूरी था कि जो गीत इस वक़्त में गाया जा रहा है वो किसके नाम पर सपूत है? दरवाजे पर जैसे ही खट-खट हुई तो बाहर खड़े उन सभी के शरीर में जैसे बिजली सी उतर आई हो। गीतों की आवाज़ से लेकर संगीत की धून तक सभी में तेजी उतर आई थी। ढोलक की एक थाप लगी और गीत उस भर्राई आवाज़ में तैर गया।
दरवाजे पर एक लड़की थी, वो इन पाँचो जनो को देखकर वहीं पर खड़ी अपने घरवालो को आवाज़ लगाने लगी। उसकी आवाज़ भी बाहर में गाये जा रहे गीतों की आवाज़ों में खो गई थी। मगर, घर की दीवारों ने उसकी आवाज़ को ज़्यादा वज़नदार बना दिया था। अन्दर घर में से एक आदमी बाहर आकर खड़ा हो गया और उन्हे देखने लगा। उनके सामने पाँच जने थे। एक के गले मे हारमोनियम लटका था तो दूसरे के गले में ढोलक टंगी थी। दोनों के मुँह में लाल रंग की लाली छलक रही थी। माथे पर काले रंग का बड़ा सा टीका लगा था और हाथ अपना काम बड़ी बेफिक्री से कर रहे थे। खाकी कुर्ते में दोनों एक ही कंपनी के मुलाजिम लग रहे थे और सबसे आगे ख़डी थी तीन औरतें। तीनों ने घाघरा चौली पहना था अलग-अलग रंग का मगर तीनों मे ही छोटे-छोटे शीसे जड़े थे। एक औरत ने अपने शरीर पर सफेद रंग का दुसाला डाला हुआ था और दूसरी ने अपने गले मे एक थैला लटकाया था और हाथों मे घूघंरू लेकर बजा रही थी। दुसाला ओड़े औरत अपनी बड़ी मोटी और भर्राई आवाज़ में गीत गा रही थी। इन तीनों में से तीसरी की उम्र थोड़ी कम थी। उसने गुलाबी रंग का घाघरा चौली पहना था जो बेहद चमक रहा था। उसी ने अपने पाँव मे घूंघरू पहने थे। जो बस, बीच-बीच में थाप के साथ में उछल पड़ती थी। उसी को देखने के लिए सिढ़ियों की मुंडेरी पर भीड़ लटक रही थी।
गीत गा रही वो मोटी भर्राई आवाज़ वाली औरत के माथे पर काले रंग की मोटी सी बिन्दी लगी थी। उसका चेहरा बेहद भारी व बड़ा था। उसके चेहरे पर कई रंगो का मेकप था। आँखों की आईब्रों से लेकर कानो तक लाल और सफेद रंग की छोटी-छोटी बिन्दियाँ बनी हुई थी। गाल और ठोडी पर काले रंग की तीन एक साथ बिन्दियाँ बनी थी। आँखों मे काला और ये भारी काज़ल भरा हुआ था जिसके कारण उसकी आँखें लाल हो चली थी। नाक मे भारी व मोटी नथ थी और कान मे बड़े-बड़े पीतल के कुंडल थे। गले मे मेटल का भारी सा हार था। हाथों मे कलाइओ से लेकर कांधे तक उसने बाजूबन्द पहने हुए थे। वे उस लिबास मे बेहद भारी लग रही थी। उसके साथ-साथ उसकी आवाज़ उसके उस रूप को और भी मजबूत बना रही थी। किसी भी गीत को उसकी आवाज़ मे सुनने का मतलब था की कभी ना भूलाया जायेगा। अगर गीत याद न रहा तो ये बात तय रहेगी कि उसका चेहरा और रूप कभी दीमाग से ओझल नहीं होगा। उसी से ये वक़्त और महफ़िल यादों में किसी खूटी से टंगा रह जायेगा।
उन्होनें अपने गीत में मकान मालिक का नाम दोहराते हुए उन्हे खुश करने की कोशिश की। मकान मालिक अपना नाम उनके गीत मे सुनकर चौंक से गए। 'उनके गीत में मेरा नाम कैसे आया?' इस टोली ने इतना बेहतरीन माहौल बना दिया था कि उन्हे ये तक याद ना रहा था कि उनका नाम उनके ही दरवाजे पर लटकी तख़्ती पर लिखा है।
“राजा राम जी सवारी पँहुची रे इंद्रलोक"
जिनको लगा मीठे लठ्ठुओ भोग।
राजाराम मकान मालिक का ही नाम था। वे उनकी तरफ़ मे चौंकते हुए देखने लगे। राजाराम जी पंत अस्पताल मे ही काम करते हैं। वे वहाँ वॉडबॉय हैं। हालाँकि अब उनकी उम्र बॉय की नहीं रही। चवालिस साल के हो गए हैं। उन्हे वैसे इन गीतों मे बेहद मज़ा आता है। वे उनकी तरफ में देखकर मुस्कुराये और उन्हे घर मे बुलाने का फैसला लिया। वहीं दरवाजे पर बैठने का इशारा करते हुए वे अन्दर चले गए। मंडली ने उनका इशारा पाया और वहीं चौखट पर ही बैठ गई। बस, माहौल में इस वक़्त मद्धम हारमोनियम कि ही आवाज़ आ रही थी वो भी खाली एक ही हाथ चल रहा था। हारमोनियम की आवाज़ जैसे इस वक़्त माहौल को पम्प कर रही थी। कमरा उसी आवाज़ मे इतना सुहाना बन गया था कि जैसे सफ़र मे हो और विविधभारती चल रहा हो। कमरे मे केवड़े अथवा मुगरे के फूलों की महक भर गई थी। पाँचो टोली के लोग वहीं चौखट पर ही बैठने की अजेस्टमेन्ट कर रहे थे। राजाराम जी अन्दर कमरे में से पानी का जग भर कर बाहर आये और उनकी तरफ मे देखकर मुस्कुराने लगे। उनके चेहरे पर एक चमक थी। सबको पानी पिलाया और वहीं उनके साथ में लगे सोफे पर बैठ गए। उनकी बीवी और उनकी तीनों बेटियाँ उनके साथ मे ही आकर बैठ गई थी। टोली की आँखें इस समय मे पूरे कमरे में घूम रही थी। कभी कमरे में घूमती तो कभी सामने बैठे इस घर के मालिकों पर।
“अरे आप तो चुप हो गए, कोई गीत सुनाइये।" उनकी बीवी ने कहा।
“कौणसा गीत सुनना है थारे को, बीन्दड़ी।"
“अपने जी ने अनुसार कोई सा भी सुना दो।"
उन्होनें पीछे बैठे हारमोनियम वाले से कुछ आँखों में इशारा किया और हारमोनियम की धून शुरू हो गई। साथ में बैठी मे वो गुलाबी घाघरे वाली लड़की खड़ी हो गई और एक बार फिर से उस भर्राई आवाज़ मे कोई बेहद तड़कता लोकगीत बाहर आने लगा। इसमे उसके शब्दों को जानना या समझना कोई जरूरी नहीं था। पहली चार लाइन बेहद धीमे थी। जैसे ही उन लाइनों मे हल्की की रुकावट आई तो बस, ढोलक की दनादन थाप लगनी शुरू हो गई। यहाँ पर थाप लगी और वहाँ वो गुलाबी घाघरे वाली लड़की के पाँव जमीन में दबादब पड़ने लगे। वे वहीं पर हल्का-हल्का घूम रही थी। जब वो घूमती तो लगता जैसे उसके घाघरे का झोल भी उसके साथ में थिरक रहा है। गीत के साथ-साथ मे उसके होंठ हिल रहे थे। वो घूमती -घूमती राजाराम जी के किचन मे चली जाती और फिर बाहर आ जाती। वो तो बस, थाप पर दबादब कूद रही थी और बार-बार घूम जाती, अपनी चुनरी को अपने हाथों से कभी तो दायें तो कभी बायें करती, फिर घूम जाती, कभी घूमती-घूमती बैठती और फिर झटके से खड़ी हो जाती, फिर से अपनी चुनरी को पकड़ घूम जाती।
उनकी चौखट तो अब तक भर चुकी थी, देखने वालो की भीड़ दरवाजे पर जमा हो गई थी। सभी अवधारणाये तोड़कर लोग राजाराम जी की चौखट पर खड़े महफ़िल का आन्नद ले रहे थे। सभी मे उचक-उचक कर देखने की लालसा नज़र आ रही थी। आँखें जिसे खोज रही थी वो तो किचन में नाच रही थी। गीत में लय और संगीत में कसक इतनी जोरदार थी कि पाँव अपने आप जमीन से उठने लगते। ये नाच सभी में क्यों आ रहा था? ये सवाल बहुत बड़ा अथवा गहरा था। मगर इस हालात में किसी भी सवाल को सोचने का मतलब था की आप महफ़िल की मदहोशी से बेहयाई कर रहे हैं।
गीत काफी लंबा था, गाने और संगीत बजाने वालों के चेहरे पर पानी की बूंदे छलक आई थी। वो घूंघरू बजाने वाली के हाथ सुर्ख लाल हो गए थे। इतने मे एक बहुत ही मोटी आवाज़ में गीत शुरू हुआ। ये आवाज़ उन टोली मे से किसी की नहीं थी। वे आवाज़ राजाराम जी की थी, जो आज अपनी ही धुन में थी। पानी का ग्लास हाथ में पकड़े राजाराम जी बेहद मदहोश थे। दरवाजें पर खड़े सभी लोग मुस्कुरा रहे थे। उनकी बेटी बहुत खुश थी। राजाराम जी उस मोटी भर्राई आवाज़ वाली औरत के मुँह की तरफ देखते हुए गीत गा रहे थे। चेहरे पर गीत के साथ मे चलते भाव थे। कभी मुस्कुराहट के तो कभी कहीं खो जाने वाले, अपनी आँखें बन्द करके वो एक लम्बी लय को अपने मुँह मे छेड़ जाते।
ढोलक की थाप उसी तरह से बज रही थी जैसे अभी तक बुदबुदा रही थी। माहौल में इस जरा से बदलाव से रोमांच और बड़ गया था। अब टक्कर बराबर की थी। एक ऐसी टक्कर जो बेहद लज़ीज़ थी।
राजाराम जी कैसे इस अस्पताल की लाइन में आ गए थे ये सोचना नगवारा था। इससे पहले वे कई महफ़िल की शान से कम नहीं थे। अपने चार दोस्तों के साथ मे ये निकले थे लड़को और लड़कियों मे कला भरने। मगर खाली वे गीत जिनको कोई गाता नहीं हैं, कोई उनके पीछे दीवाना नहीं है। वे गीत कहाँ है? ये भी पूछना किसी के लिए जरूरी नहीं होता। अपनी इसी धून से निकलने के बाद मे ये इसी अस्पताल मे डेलीवेज़ का काम किया करते थे। जो कभी होता तो कभी नहीं होता था। जगंलो मे जाकर अपने गीतों को बहुत तेज़ आवाज़ में गाया करते थे। जहाँ पर लोग बड़ी जोर-जोर से हँसते थे वहाँ पर ये अपने गीतों मे खोते थे। इनका रिश्ता गीतों के साथ बिलकुल ऐसा ही था जैसे साल के एक महिने मे सपेरे अपने साँपो को आज़ाद छोड़ देते हैं कभी उनकी ख़बर नहीं लेते उसके बाद मे उन्हे दोबारा पकड़ते हैं, जहाँ पर छोड़ा था वहीं पर जाते है। लेकिन वो वहाँ नहीं मिलते।
यही इनका हाल था, अपने काम और उसकी टेंशन से जैसे ही बाहर आते तो बस, कहीं गायब हो जाते। किसी को नहीं मिलते। ये उन दिनों मे खोते, गायब होते और फिर से उस दौर मे पँहुच जाते जहाँ से इन्होनें खुद को निकाला था। ये होना खाली काम और समाजिक ज़िन्दगी मे ही कायम था, कला के साथ मे इसका रिश्ता डगमगाया था।
आज जैसे फिर से वो महिना था जिसमे इन्होनें खुद को आज़ाद छोड़ दिया था। उनकी लड़की उस गुलाबी घाघरे वाली लड़की के साथ मे नाच रही थी। कभी उसकी मुद्रा के साथ मे अपने शरीर को ढाल लेती तो कभी उससे कोसो दूर हो जाती। ये सिलसिला जारी था। राजाराम जी के लिए ये दौर किसी भी अवधारणा से कसा हुआ नहीं था।
जो कदम बाहर दरवाजे पर खड़े उनको निहार रहे थे वे कमरे मे आ गए थे। उनके गीतों मे कोई बीते सवाल का घेरा नहीं था। बस, माहौल मे कैसे उस लज़ीज़ स्वाद को बरकरार रखा जा सकता है वे था। उनकी बीवी तो बस, ये सोच रही थी कि अब पड़ोस मे होती बातों को कैसे समझेगी? कैसे लोगों को ये बतायेगी की उनके पति में ये कहाँ से और कैसे आया?
ये दौर ना जाने कितने तरह के भाव चेहरे पर बना रहा था और राजाराम जी का वो गीत ख़त्म ही नहीं हो रहा था। शायद यहाँ कोई चाहता भी नहीं था की वो कभी ख़त्म भी हो।
लख्मी
Wednesday, January 21, 2009
जाने के हर रास्ते बन्द...
पंडित जी ने अपना कमन्डल उठाया और शमशानघाट से विदा लेने के लिए तैयार हो गए। बहुत ही नराज़ थे दिल्ली की सरकार से। अब शमशान घाट नये तरीके बनाया जा रहा है। जिसमे उसको बैठने के लायक बनाया जाएगा। जहाँ पर गन्दगी और कोई जानवर ना तो आएगा और ना ही दिखाई देगा। इसलिए पंडित जी की भी विदाई कर दी गई है। सबसे ज़्यादा जानवर पालने वाले ये ही शख़्स थे। जो अपना काम जानवरों से कराते आए है। चाहें वो अन्य जानवरों को भगाना हो या फालतू बच्चों को जो वहाँ से चीजों को बीन कर ले जाया करते थे। जिनके लिए यहाँ की कोई भी चीज भूत-प्रेत की नहीं थी। किसी की साड़ी या किसी का कोई भी कपड़ा हो फिर कोई खिलौना वो सब इनके लिए खेलने के ही आभूषण बन जाते। जिनसे अपने खेलो को सजाया और नाम दिया जाता। वो भी अब नज़र नहीं आएगे। धीरे-धीरे वहाँ कि सफ़ाई भी होने लगी है। वहाँ के पैशाब घर से लेकर लकड़ी की दूकान तक। शमशान घर की बाऊंडरी की दीवार में जितने आने-जाने के अनचाहें द्वार बने हुए थे। जो ज़्यादातर सुअर अपना आने-जाने के रास्ते बनाये हुए थे उसको भी बन्द कर दिया गया है।
ये काम पिछले 3 महिनो से चल रहा है। MCD के कुछ काम करने वाले लोग वहाँ पर हर रोज आते है और सफ़ाई शुरु कर देते है। पंडित जी जिस कोने में अपना आसरा बनाया हुआ था उस जगह की भी सफ़ाई कर दी गई है। पंडित जी ने अपने घर के सामने एक दीवार बनाई हुई थी। अर्थी में आई लकड़ियों से और वहाँ पर पड़ी रहती चीजों से। वो भी वहाँ से हटा देने से इतना खुला-खुला लगता है की शमशान घाट लगता ही नहीं की किसी कालोनी के किनारे का हिस्सा है। वो दीवार ना होने से कालोनी के पार्क का एक छोर शमशानघाट से मिल जाता है और शमशान घाट बहुत बड़ा नज़र आता है।
पंडित जी पूरी सरकार को गालियाँ देते हुए अब अपना बोरिया-बिस्तरा समेट चुके थे। बस, रजिस्टरों पर उनके हस्ताक्षर लेने बाकि थे। मगर वो तो मदिरा में इतने धुत थे कि उनके हस्ताक्षर कैसे कराये जाए ये सोचना पहले जरूरी था। उनको शिवराम जी ने और उनकी घरवाली ने पकड़ा हुआ था वो बहुत नशे में थे।
सफ़ाई हो जाने के बाद भी वहाँ पर एक ही आदमी ने अपना दब-दबा बनाया हुआ था। वो था लकड़ी वाला। लकड़ियों का काम इतना बड़ गया है कि अब शमशान घाट मे लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ नज़र आती है। अब वहाँ पर लकड़ी नहीं बल्की अर्थियाँ बिकती है। वो अब लकड़ियों को पहले से ही मोक्षस्थल पर अर्थियाँ बनाकर तैयार रखते है और वही बिकता है। शमशान घाट के गेट के ऊपर एक लाइन जो लिखी है की 'बाहर की कोई भी चीज को अन्दर नहीं लिया जाएगा। कृप्या लकड़ी व क्रियाक्रम का सारा समान अन्दर से ही ले।' हर मोक्षस्थल पर पहले ही अर्थी का सारा समान तैयार होता है तो मुर्दा आता है और उन लकड़ियों पर लेटा दिया जाता है बस, मुखागनी दे जाती है और कार्य समपन्न।
एक-एक अर्थी की कीमत लगा दी जाती है। कीमत होती है 1200, 1500, 2000, 3000 रुपये तक लगा दी जाती है बस, उसी का सौदा किया जाता है। 1200 रुपये में लकड़ियाँ कम और बचा-कुचा माल ज़्यादा होता है। जिसमे चलने के बाद में मुर्दे के खिसकने का डर ज़्यादा रहता है। कई बार तो गीली-गीली लकड़ियाँ रख दी जाती है। जिन्हे जलाने में कई किलो देशी घी लग जाता है तो लोग ऐसा काम ही नहीं करते। वो तो चाहते है की मरने के बाद तो उसे कोई दुख ना हो और मिट्टी का तेल डाला नहीं जा सकता। बस, 2000 रुपये तक में सौदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं लोग।
लकड़ी वाले ने कई टन लकड़ियाँ मंगाई हुई है और शमशान घाट मे चारों तरफ़ में अपनी लकड़ियों को फैला हुआ है। देखने मे तो शमशान घाट किसी पार्क से कम नहीं लगता। अब देखा जाए तो डर जैसी हवा दूर तक नहीं भटकती। शाम मे तो शायद वहाँ कई तरह की रोनक बन जाती होगीं। हर वक़्त वहाँ पर लाउडस्पीकर मे गायत्री मन्त्र की कैसेट चलती रहती है और वहाँ आए अर्थी के साथ में लोग उस मन्त्र का आन्नद लेते हैं।
शिवराम जी भी उन्ही पंडित जी के साथ मे शमशान घाट से जाने की कह रहे थे। शायद आगे बनने वाले शमशान घाट मे किसी शिवराम जी की जरूरत नहीं होगी। जो अपनी मर्जी से किसी भी अर्थी के साथ मे लग जाया करते। जो उसे पहले पुन्य का काम मानते और उसके बाद मे कुछ पाने की तमन्ना रखते। अब तो वहाँ पर कोई सरकारी नौकरी करने वाला आएगा जो सारे काम सरकारी नियमों के अनुसार करेगा। शायद अर्थी में होने वाले कामो को भी और रिवाज़ो को भी वो नौकरी मान कर ही करेगा। अब तो सारे काम नियम अनुसार ही होगें। कब क्या करना है वो सब अब कागज़ो में लिखा-पढ़ी के बाद ही आगे बढ़ाया जाएगा।
इन शब्दों में पंडित जी के बोल ज़्यादा थे। शिवराम जी तो बस उन्हे सम्भाले हुए थे और उलटे पाँव जाते-जाते शमशान घाट को ताक रहे थे। शायद ये उनका आखिरी दिन था।
लकड़ी वाले ने सारी लकड़ियों को उस अस्थियों वाले कमरे में लाद दिया था। जहाँ पर अब किसी आदमी का जाना न मुमकिन था। कई अस्थियों की थैलियाँ ज्यों की त्यों लटक रही थी। मगर अब वहाँ तक किसी का हाथ नहीं पँहुच सकता था। कोई अगर आ गया अपने किसी को लेने के लिए तो वो इन्हे कैसे लेकर जाएग? ये तो यहीं पर रह जाएगी।
शिवराम जी उसी कमरे के सामने खड़े बस, वहाँ पर टंगी उन थैलियों को देख रहे थे। सोच रहे थे की उन लकड़ियों को कैसे हटाया जाए जो वहाँ पर टंगी कई थैलियों को फाड़ रही थी। कई लकड़ियों के ताज (अर्थी के ऊपर झंडियों और गुब्बारों से सजाया हुआ) भी उन लकड़ियों मे फंस कर महज लकडी ही बन गए थे। आज से पहले वो अर्थियों के ताज हुआ करते थे। ये ताज़ उन पर चढ़ाया जाता था जो मरने से पहले अपनी तीन या चार पीढ़ी को देख जाया करते थे। यानि जो अपना पोता और पोते की भी औलाद देख लेता है। जिसको बैण्ड-बाजे के साथ में लाया जाता है और उसे इस कमरे की रौनक बना दिया जाता है। सारी रंगीन झंडियाँ तो अब उनमे नहीं नज़र आ रही थी बस, बाँस के डंडे ही दिखाई दे रहे थे।
लकड़ी वाला शिवराम जी जो अपने यहाँ पर नौकरी रखने के लिए कह रहा था। 2500 रुपये महिना दे देगा। बस, मोक्षस्थल पर 1500 रुपये वाली में जो लकड़ियाँ रखी जाती है उनमे से वो लकड़ियाँ कम लगे और पैसा भी पूरा मिले। लकड़ियाँ भी कम लगाई जाए और वो ऊंची भी नज़र आए। लगे की जैसे 1500 की अर्थी है मगर वो बनी हो 1200 मे लगी लकड़ियों से। ये काम खाली वहाँ पर शिवराम जी के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता था। वो इतनी ठोस अर्थी लगाते थे की लकड़ियाँ भी कम लगती थी और वो कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ती। मुर्दे का भी खिसकने का कोई डर नहीं होता था। बहुत मजबूत बनाते थे शिवराम जी अर्थी।
लकड़ी वाला ऐसे आदमी को क्यों हाथ से जाने देखा?
शिवराम जी का दिमाग अभी दो भागों में बट गया था। जिस काम को वो गालियाँ देते आए थे वो ही काम उन्हे अपनी तरफ़ में खींच रहा था जिससे वो अपना परिवार भी चला सकते थे और जिसे वो पुन्य का काम मानते थे वो भी उनके करीब ही रहता। जिस काम को करना चाहते है या करते आए है वो अब किसी सरकारी नौकरी मे तबदील हो गया है। अब तो जैसे कोई ऐसा काम ही नहीं बचा की जिसको अपनी मर्जी से किया जाए और वहाँ से कोई सौगात मिल जाए। एक ये ही काम था पर ये भी अब सरकारी नौकरी बन गया है। बस, यहीं पर उनका दिमाग उलझा हुआ था।
वो उस कमरे में से सारी चीजों को खींच रहे थे। आज से पहले कभी इतना गौर से नहीं देखा था उन चीजों को उन्होनें। कई तो बीढ़ी-माचिस, हुक्के की चिल्म, बक्से (गल्ले के जैसे) और कुछ बर्तन थे। बर्तनो पर तो तारीख़ें भी लिखी हुई थी जिन्हे गुदवा कर लिखा गया था। किसी पर 1981 कि तारीख़ थी तो किसी 1990 कि। ये तारीख़ें सन के हिसाब से 1980से शुरू होती और 1999 तक जाती थी। बर्तनो पर ज़ंग लग गई थी। कई पोटलियाँ निकली जिनमे कई पुराने कपड़े बन्धे हुए थे। जिनकी गिनती करना आसान नहीं था।
वो लकड़ियों पर खड़े हुए थे और अपना संतुलन बनाकर सारे सामानों को एक जगह पर लेकर खड़े थे। अभी तो कई समान और था जिस तक हाथ नहीं पँहुच रहा था।
यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था जिसे इन चीजों का आसरा भी हो। लकड़ी वाले के लिए ये जगह कोई शमशानघाट नहीं थी। ये जगह तो एक ऐसा कार्यस्थल थी की जहाँ पर आने वाला ग्राहक कहीं और से कुछ ले ही नहीं सकता। यहाँ पर आने वाला यहीं से ही चीजों को खरीद सकता है और कोई है भी नहीं यहाँ पर उसके आलावा। पंडित जी के लिए ये जगह एक बसेरा थी जिसको छोड़ने पर अपनी सारी पहचान की पत्रियों को बदलना होगा और लोगों से दोबारा से एक और नये रिश्ते की बुनियाद रखनी होगी।
आज कई और अन्य भागों में बट गया था ये शमशान घाट।
शिवराम जी अगर अब यहाँ से गए तो क्या करेगें और अब इस उम्र में कौन नौकरी देगा इस पर ही वो अपना सारा दिमाग ख़र्च करने मे लगे थे। अब तो सारे शमशान घाट में ये काम ख़त्म हो गया होगा।
लख्मी
ये काम पिछले 3 महिनो से चल रहा है। MCD के कुछ काम करने वाले लोग वहाँ पर हर रोज आते है और सफ़ाई शुरु कर देते है। पंडित जी जिस कोने में अपना आसरा बनाया हुआ था उस जगह की भी सफ़ाई कर दी गई है। पंडित जी ने अपने घर के सामने एक दीवार बनाई हुई थी। अर्थी में आई लकड़ियों से और वहाँ पर पड़ी रहती चीजों से। वो भी वहाँ से हटा देने से इतना खुला-खुला लगता है की शमशान घाट लगता ही नहीं की किसी कालोनी के किनारे का हिस्सा है। वो दीवार ना होने से कालोनी के पार्क का एक छोर शमशानघाट से मिल जाता है और शमशान घाट बहुत बड़ा नज़र आता है।
पंडित जी पूरी सरकार को गालियाँ देते हुए अब अपना बोरिया-बिस्तरा समेट चुके थे। बस, रजिस्टरों पर उनके हस्ताक्षर लेने बाकि थे। मगर वो तो मदिरा में इतने धुत थे कि उनके हस्ताक्षर कैसे कराये जाए ये सोचना पहले जरूरी था। उनको शिवराम जी ने और उनकी घरवाली ने पकड़ा हुआ था वो बहुत नशे में थे।
सफ़ाई हो जाने के बाद भी वहाँ पर एक ही आदमी ने अपना दब-दबा बनाया हुआ था। वो था लकड़ी वाला। लकड़ियों का काम इतना बड़ गया है कि अब शमशान घाट मे लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ नज़र आती है। अब वहाँ पर लकड़ी नहीं बल्की अर्थियाँ बिकती है। वो अब लकड़ियों को पहले से ही मोक्षस्थल पर अर्थियाँ बनाकर तैयार रखते है और वही बिकता है। शमशान घाट के गेट के ऊपर एक लाइन जो लिखी है की 'बाहर की कोई भी चीज को अन्दर नहीं लिया जाएगा। कृप्या लकड़ी व क्रियाक्रम का सारा समान अन्दर से ही ले।' हर मोक्षस्थल पर पहले ही अर्थी का सारा समान तैयार होता है तो मुर्दा आता है और उन लकड़ियों पर लेटा दिया जाता है बस, मुखागनी दे जाती है और कार्य समपन्न।
एक-एक अर्थी की कीमत लगा दी जाती है। कीमत होती है 1200, 1500, 2000, 3000 रुपये तक लगा दी जाती है बस, उसी का सौदा किया जाता है। 1200 रुपये में लकड़ियाँ कम और बचा-कुचा माल ज़्यादा होता है। जिसमे चलने के बाद में मुर्दे के खिसकने का डर ज़्यादा रहता है। कई बार तो गीली-गीली लकड़ियाँ रख दी जाती है। जिन्हे जलाने में कई किलो देशी घी लग जाता है तो लोग ऐसा काम ही नहीं करते। वो तो चाहते है की मरने के बाद तो उसे कोई दुख ना हो और मिट्टी का तेल डाला नहीं जा सकता। बस, 2000 रुपये तक में सौदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं लोग।
लकड़ी वाले ने कई टन लकड़ियाँ मंगाई हुई है और शमशान घाट मे चारों तरफ़ में अपनी लकड़ियों को फैला हुआ है। देखने मे तो शमशान घाट किसी पार्क से कम नहीं लगता। अब देखा जाए तो डर जैसी हवा दूर तक नहीं भटकती। शाम मे तो शायद वहाँ कई तरह की रोनक बन जाती होगीं। हर वक़्त वहाँ पर लाउडस्पीकर मे गायत्री मन्त्र की कैसेट चलती रहती है और वहाँ आए अर्थी के साथ में लोग उस मन्त्र का आन्नद लेते हैं।
शिवराम जी भी उन्ही पंडित जी के साथ मे शमशान घाट से जाने की कह रहे थे। शायद आगे बनने वाले शमशान घाट मे किसी शिवराम जी की जरूरत नहीं होगी। जो अपनी मर्जी से किसी भी अर्थी के साथ मे लग जाया करते। जो उसे पहले पुन्य का काम मानते और उसके बाद मे कुछ पाने की तमन्ना रखते। अब तो वहाँ पर कोई सरकारी नौकरी करने वाला आएगा जो सारे काम सरकारी नियमों के अनुसार करेगा। शायद अर्थी में होने वाले कामो को भी और रिवाज़ो को भी वो नौकरी मान कर ही करेगा। अब तो सारे काम नियम अनुसार ही होगें। कब क्या करना है वो सब अब कागज़ो में लिखा-पढ़ी के बाद ही आगे बढ़ाया जाएगा।
इन शब्दों में पंडित जी के बोल ज़्यादा थे। शिवराम जी तो बस उन्हे सम्भाले हुए थे और उलटे पाँव जाते-जाते शमशान घाट को ताक रहे थे। शायद ये उनका आखिरी दिन था।
लकड़ी वाले ने सारी लकड़ियों को उस अस्थियों वाले कमरे में लाद दिया था। जहाँ पर अब किसी आदमी का जाना न मुमकिन था। कई अस्थियों की थैलियाँ ज्यों की त्यों लटक रही थी। मगर अब वहाँ तक किसी का हाथ नहीं पँहुच सकता था। कोई अगर आ गया अपने किसी को लेने के लिए तो वो इन्हे कैसे लेकर जाएग? ये तो यहीं पर रह जाएगी।
शिवराम जी उसी कमरे के सामने खड़े बस, वहाँ पर टंगी उन थैलियों को देख रहे थे। सोच रहे थे की उन लकड़ियों को कैसे हटाया जाए जो वहाँ पर टंगी कई थैलियों को फाड़ रही थी। कई लकड़ियों के ताज (अर्थी के ऊपर झंडियों और गुब्बारों से सजाया हुआ) भी उन लकड़ियों मे फंस कर महज लकडी ही बन गए थे। आज से पहले वो अर्थियों के ताज हुआ करते थे। ये ताज़ उन पर चढ़ाया जाता था जो मरने से पहले अपनी तीन या चार पीढ़ी को देख जाया करते थे। यानि जो अपना पोता और पोते की भी औलाद देख लेता है। जिसको बैण्ड-बाजे के साथ में लाया जाता है और उसे इस कमरे की रौनक बना दिया जाता है। सारी रंगीन झंडियाँ तो अब उनमे नहीं नज़र आ रही थी बस, बाँस के डंडे ही दिखाई दे रहे थे।
लकड़ी वाला शिवराम जी जो अपने यहाँ पर नौकरी रखने के लिए कह रहा था। 2500 रुपये महिना दे देगा। बस, मोक्षस्थल पर 1500 रुपये वाली में जो लकड़ियाँ रखी जाती है उनमे से वो लकड़ियाँ कम लगे और पैसा भी पूरा मिले। लकड़ियाँ भी कम लगाई जाए और वो ऊंची भी नज़र आए। लगे की जैसे 1500 की अर्थी है मगर वो बनी हो 1200 मे लगी लकड़ियों से। ये काम खाली वहाँ पर शिवराम जी के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता था। वो इतनी ठोस अर्थी लगाते थे की लकड़ियाँ भी कम लगती थी और वो कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ती। मुर्दे का भी खिसकने का कोई डर नहीं होता था। बहुत मजबूत बनाते थे शिवराम जी अर्थी।
लकड़ी वाला ऐसे आदमी को क्यों हाथ से जाने देखा?
शिवराम जी का दिमाग अभी दो भागों में बट गया था। जिस काम को वो गालियाँ देते आए थे वो ही काम उन्हे अपनी तरफ़ में खींच रहा था जिससे वो अपना परिवार भी चला सकते थे और जिसे वो पुन्य का काम मानते थे वो भी उनके करीब ही रहता। जिस काम को करना चाहते है या करते आए है वो अब किसी सरकारी नौकरी मे तबदील हो गया है। अब तो जैसे कोई ऐसा काम ही नहीं बचा की जिसको अपनी मर्जी से किया जाए और वहाँ से कोई सौगात मिल जाए। एक ये ही काम था पर ये भी अब सरकारी नौकरी बन गया है। बस, यहीं पर उनका दिमाग उलझा हुआ था।
वो उस कमरे में से सारी चीजों को खींच रहे थे। आज से पहले कभी इतना गौर से नहीं देखा था उन चीजों को उन्होनें। कई तो बीढ़ी-माचिस, हुक्के की चिल्म, बक्से (गल्ले के जैसे) और कुछ बर्तन थे। बर्तनो पर तो तारीख़ें भी लिखी हुई थी जिन्हे गुदवा कर लिखा गया था। किसी पर 1981 कि तारीख़ थी तो किसी 1990 कि। ये तारीख़ें सन के हिसाब से 1980से शुरू होती और 1999 तक जाती थी। बर्तनो पर ज़ंग लग गई थी। कई पोटलियाँ निकली जिनमे कई पुराने कपड़े बन्धे हुए थे। जिनकी गिनती करना आसान नहीं था।
वो लकड़ियों पर खड़े हुए थे और अपना संतुलन बनाकर सारे सामानों को एक जगह पर लेकर खड़े थे। अभी तो कई समान और था जिस तक हाथ नहीं पँहुच रहा था।
यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था जिसे इन चीजों का आसरा भी हो। लकड़ी वाले के लिए ये जगह कोई शमशानघाट नहीं थी। ये जगह तो एक ऐसा कार्यस्थल थी की जहाँ पर आने वाला ग्राहक कहीं और से कुछ ले ही नहीं सकता। यहाँ पर आने वाला यहीं से ही चीजों को खरीद सकता है और कोई है भी नहीं यहाँ पर उसके आलावा। पंडित जी के लिए ये जगह एक बसेरा थी जिसको छोड़ने पर अपनी सारी पहचान की पत्रियों को बदलना होगा और लोगों से दोबारा से एक और नये रिश्ते की बुनियाद रखनी होगी।
आज कई और अन्य भागों में बट गया था ये शमशान घाट।
शिवराम जी अगर अब यहाँ से गए तो क्या करेगें और अब इस उम्र में कौन नौकरी देगा इस पर ही वो अपना सारा दिमाग ख़र्च करने मे लगे थे। अब तो सारे शमशान घाट में ये काम ख़त्म हो गया होगा।
लख्मी
दरवाजा खुला था
घर में हर एक चीज़ का अपना एक स्थान होता है पर आज को देखकर तो लग रहा जैसे कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो सज़ाई नहीं जा सकती हों।
दरवाजा खुला था। दरवाजे की साँकर हमेशा हिलती रहती है उनकी। कोई भी अन्दर आये दरवाजे की वही साँकर हिलकर बता देती है की कोई आया है। शिवराम जी जब भी गली मे कदम रखते तो गली वालों की नज़रें हमेशा उन्ही पर रहती थी। ये तो कम ही होता था की वो घर आ रहे है मगर ये ज़्यादा होता था की वो आज क्या ला रहे है। यही देखने के लिए निगाहें अक्सर उनपर चली जाती थी।
आज तो उनके काधों पर कुर्सी रखी थी मस्त गद्देदार और आराम दायक। वो उसे उठाये चले आ रहे थे और उनके हाथों मे एक भी पॉलिथीन थी। वो जैसे-जैसे अपने कदम अन्दर रखते जाते औरतें उनके आगे से अपने बच्चो को हटा लेती। पता नहीं किस सायें से बचना चाहती थी वो? शिवराम जी को ये सोचना ज़्यादा अनिवार्य नहीं होता था बस, आँखें यही देखती थी की जो आज तक मैं शमशाम घाट में रहकर नहीं देख पाया था वो इनको कैसे दिखता था? मुझे क्या? वो तनकर चले आते। उनका घर गली के बीच में था और गली भी इतनी चौड़ी नहीं थी की चार-पाँच आदमी उसमे से एक साथ निकल सकें। पतली गली में वो सभी के आँगनो में पाँव रखकर वो चले-चले जाते।
उनकी नज़र जब भी किसी पर पड़ती तो वो ये साफ़ देख लिया करते थे कि उनको कोई नहीं देख रहा होता सबकी नज़रें उस पर होती जो कभी काधों पर तो कभी हाथों में होता। वो ये देखकर हमेशा मुस्कुरा देते। इसलिए नहीं की ये गली वाले उन्हे ऐसे देख रहे है या आज के जमाने मे भी ये सब सोचा जाता है मगर इसलिए की अभी वो घर में घुसेगें और उनकी बीवी भी कुछ इसी नज़र से देखेगी और पता नहीं क्या-क्या पूछेगी? उन गली वालो की नज़र से ये उनको ये समझ में आने लगा था की वो जब भी घर वापस लौटते है तो वो अकेले नहीं होते उनके साथ मे कई ऐसे लोग होते थे जिनको शिवराम जी ने तो आज तक नहीं देखा था मगर उनके अलावा कई आँखों ने उन्हें देख लिया था। जिनको देखना आसान बात नहीं थी। सब के सब इस तरह से रास्ता छोड़ते जैसे शिवराम जी किसी को काँधों पर उठाकर ला रहे हो।
शिवराम जी ने अन्दर आकर कुर्सी को पहले तो अपने काँधों पर से उतारा और पॉलिथीन में रखी जूतियों को उन्होनें वहीं दरवाजे के पीछे रख दिया। ज़्यादा बड़ा कमरा नहीं है उनका। उनके सोने-बैठने की जगह बाहर वाले कमरे मे ही बनाई हुई है। वो कब आयेगें या कितने बख़्त में आयेगें? कुछ पता नहीं होता उनके घरवालों को। इसलिए वो एक खाट-बिस्तर वहीं एक कोने में दीवार से सटाकर हमेशा तय लगाकर रखते है।
अब शुरूआत हुई उस कुर्सी की जगह बनाने की। शिवराम जी उस कुर्सी की जगह अपने उसी छोटे से कमरे में बनाने लगे। कभी तो वो उस कुर्सी को अपनी खाट कर सिरहाने रखते तो कभी पातियाने पर। मन नहीं मानता था उनका। वो कुर्सी को उठाकर दूसरी दीवार की खिड़की के पास ले गए बिलकुल खिड़की के पास ही उन्होनें वो रखदी और बैठकर खिड़की के बाहर देखने लगें। उसकी ऊँचाई इतनी थी की रोज़ाना गली दिखाने वाली खिड़की आज तो कुछ और ही दिखा रही थी। खिड़की के बाहर देखने पर सामने वाले घर के अन्दर देखा जा सकता था मगर वो तो मोहम्मद भाई के घर का बाथरूम था। उन्होनें वहाँ से कुर्सी उठाई और वापस अपनी खाट के पास ले गए।
अभी के लिए उन्होने कुर्सी को ठीक खाट के बगल में ही रख दिया था। अब वो पॉलिथीन मे से जूतियाँ निकाल कर उसमे अपने पाँव घुसाने लगे। तीन जोड़ी जो पुरानी थी वो तो उनके बिलकुल ठीक ही आई थी। वो भी कैसे ना कैसे उन्होनें उसमे अपने पाँव डाल ही लिए थे मगर वो नई वाली जिसके बिनाह पर वो सारी उठा लाये थे वही नहीं आ रही थी। पूरा एक नम्बर बड़ी थी उनके वो। "शायद ये उसी दिन खरीदी होगी जिस दिन ये साहब स्वर्ग सिधारे थे। चड़ाने वाले को उनके पाँव का अन्दाजा नहीं होगा और क्यों हो भला ये अब चड़ाने के लिए ही तो थी कौन सा इनको अब पहननी थी।"
वो उन गोल्डन रंग की नई जूतियों को अपने हाथों में लेकर उसके ड़िज़ाइन को देखते रहे। कुछ खाट के जैसी बुनाई का ड़िज़ाइन था उसपर पर वो आई नहीं थी उनके। उन्होनें सारी जूतियों को खाट के नीचे सरकाया और वहीं एक-दम धड़ाम सें लेट गए। थोड़ी हो देर में वो वापस उठे और अपने तकीये में कुछ कतरन निकाली और उन्ही नई गोल्डन जूतियों को उठाया और उसके अन्दर वो कतरन फँसा कर उसे पहनने लगे। अभी भी नहीं आई थी तो उन्होनें दोबारा से और कतरन निकाली और अबकी ठीक तरह से उसमे फँसाई और पहनी। वाह!
चेहरा खिल गया था उनका वो आ गई थी। पर पाँव चैन से नहीं बैठ पा रहे थे शायद काट रही थी अभी वो नई जूतियाँ उन्हे? बड़े खुश से हुए थे कुछ पल के लिए वो और अपनी बनियान से उस जूती को साफ़ करते हुए वो वहीं लेट गए थोड़ा सुस्ताना जरूरी समझा था इतना सब कुछ हो जाने के बाद में उन्होनें।
अब उनके उस कमरे मे चार-पाँच चीजें तो ऐसी हो गई थी जिनका ठिकाना उनके घर के किसी और कमरे में तो नहीं था और कभी लड़-झगड़ के वो ठिकाना बनाना भी चाहें तो उनकी धर्मपत्नी ये काम तो कभी करने ही नहीं देगी उनकों और ना ही ये दौर कभी चलता फिर। उनकी बीवी के दिमाग पर तो बस एक ही भूत सवार रहता है कि ये एक मरे हुए आदमी का है वो भी चला आयेगा अन्दर। शिवराम जी को इस मरे हुए या समान का खौफ़, डर या ख़्याल हटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था।
वो एक ऐसी जगह में काम करते थे की जहाँ पर अपना कुछ टाइम बिता दो तो सारे डर और अवधारणाओ की जगह बदल जाती है। वो किसी कि अर्थी के पीछे-पीछे दो कदम चलना या वहाँ से वापस आकर स्नान करना सब का सब बे-माइने लगने लगता है। बस, ये सब इतना ज्ञात कराता है की हम अपने ऊपर से या तो किसी डर को निलम्बित कर रहे है या उस दुनिया में अपना सदेंशा भेज रहे हैं जो अभी तक किसी ने नहीं देखी। हम बस, इतना मानते हैं की जो मर कर जा रहा है वो देखेगा।
ये सब की सब बातें तो पूरी दुनिया सोचती तो खाली "मैं ही क्यों सोंचू" शिवराम जी ये सोच कर हमेशा अपने आपको हल्का करते। "ये सोच कर क्या फ़ायदा" कहकर अपनी छत की ओर देखकर वो घंटो ये ही सोचते रहते थे की मैं जो समान लेकर आ रहा हूँ वो क्या दूसित है? ऐसा क्या चिपक गया इसमे की ये किसी और के घर में नहीं जा सकती?
हर चीज के साथ में किसी का प्यार होता है तो किसी का रिवाज़ मगर इससे उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अब वहाँ पर पड़ी सुखती रहेगी या वो किस के लिए बन जाती है फिर? कई सारी चीजें वहाँ पर ऐसी पड़ी हुई है कि जिन्हें छूना और उन्हें वहीं पर पड़े रहने देने से एक एकांत का ज्ञात होता है कि जिनके नाम की वो चड़ाई गई है वो उसके साथ में अपनी आत्मा से जुड़ गई है। चलो कोई दे गया कुछ वो उसके लिए था जो उसे अब इस्तमाल नहीं कर पायेगा और जो इस्तमाल कर सकते हैं वो भी इस्तमाल नहीं करेगें। तो उन चीजों का होना या ना होना किस दुनिया से जुड़ जाता है। ये भयभीत है और अदृश्य दूनिया है।
शिवराम जी उन चीजों को देखकर बस, इसी धून में घूमने लगते की जैसे अभी उन चीजों मे बसे उस शख़्स से बातें कर रहे हो। बस, क्या था दूसरी तरफ से आवाज़ नहीं आ रही थी। वो उन चीजों को देखकर ये सोचने लगे की। वो कहाँ सोता होगा तो कोई चादर दे गया और खाट भी। वो कहाँ बैठता होगा तो कुर्सी दे गया। कपड़े से लेकर कोई नंगे पाँव मे जूतियाँ भी दे गया होगा ये सब क्या है? ये प्यार ही तो है ना! ये सब की सब जैसे बस, सतकार के लिए ही रह गई है। "अगर मैं मरूगाँ तो मेरी मईयत पर क्या चड़ाया जायेगा?” ये सोच कर वो हँसने लगे।
अब तो सपने भी शिवराम जी को कुछ ऐसे ही दिखाई देने लगे थे। वो रात भी इन्ही बातों के साथ में अपनी नींद पूरी कर लिया करते थे। अब तो वो गहरी नींद में सो गए थे। जब भी वो सोने के लिए लेटते तो वो अपने सारे कपड़ों को उतार कर वहीं खाट के नीचे में सरका दिया करते थे। उनके कपड़ों में एक ऐसी महक भर गई थी जिससे उनको हमेशा एक उलझन रहती थी। वो महक जो जलती हुई लकड़ियों कि थी कुछ सामाग्री जैसी। वो तो पज़ामा भी उतार दिया करते थे और गहरी नींद में इस तरह से खो जाते की कोई भी आवाज उनके कानों में कोई करकस नहीं पैदा नहीं कर सकती थी। महिने में चार ही बार उनके कपड़े धुलते और बदलते थे और उनके कपड़े धोने वाली एक ही औरत थी उनके घर में वो भी उनकी धर्मपत्नी।
ऐसा कोई भी दिन नहीं होता था जब उनकी झपड़ नहीं होती अपनी बीवी से। उनके थोड़ी देर सो जाने के बाद में उनके घर का अन्दर का दरवाजा खूलता और उनकी बीवी अपने में बड़बड़ाती हुई बाहर आती। उनके कपड़ों को उठाकर अपने कपड़ों से बचाती हुई उन्हें दूर से पकड़ती हुई घुसलखाने में डाल देती। हर बार उनके साथ मे रखी कोई ना कोई नई चीज़ नज़र आती।
हमेशा उनके एक ही तरह के बोल सुनने को मिलते थे वो हमेशा ही बड़बड़ाती हुई जब भी बाहर में आती तो उनको ही कोसती। "पता नहीं क्या अला-बला उठा लाते हैं। ये तो पूरे घर को शमशाम बना कर ही दम लेगें। खुद को तो देखो ज़रा एक दम मुर्दे की तरह हालत हो गई है। आज देखो क्या उठा लाये? अपने कपड़ों को भी घुसलखाने में भी नहीं डालते। कैसी बदबू आती है कपड़ों में से जैसे किसी की चिता जल रही हो।"
अब तो कोई असर नहीं पड़ता था शिवराम जी को। वो यूहीं बोलती-बोलती कपड़े धोने के लिए बैठ जाती। वो कपड़े धोने के बाद मे उठी और उनकी खाट के नीचे रखी उस पीली पॉलिथीन को खखोरने लगी। उसमे वही जूतियाँ थी। उन्होनें चारों जूतियों को देखा उन तीनों पुरानी जूतियों को उन्होनें बाहर दहलीज़ पर रख दिया और उन नई जूतियों को उठाकर घुसलखाने में ले गई। जिस पानी से वो कपड़े धो रही थी उसी पानी मे से हल्का सा छिड़काव उन्होनें उन जूतियों पर किया और साफ़ कपड़े से पौंछकर उन्होनें वहीं पर खाट के नीचे ऐसे रख दिया जैसे वो अभी जागेगें और उसमे पाँव डालकर बाहर चले जायेगें और कपड़ों को उठाकर वो छत पर चली गई।
लख्मी
दरवाजा खुला था। दरवाजे की साँकर हमेशा हिलती रहती है उनकी। कोई भी अन्दर आये दरवाजे की वही साँकर हिलकर बता देती है की कोई आया है। शिवराम जी जब भी गली मे कदम रखते तो गली वालों की नज़रें हमेशा उन्ही पर रहती थी। ये तो कम ही होता था की वो घर आ रहे है मगर ये ज़्यादा होता था की वो आज क्या ला रहे है। यही देखने के लिए निगाहें अक्सर उनपर चली जाती थी।
आज तो उनके काधों पर कुर्सी रखी थी मस्त गद्देदार और आराम दायक। वो उसे उठाये चले आ रहे थे और उनके हाथों मे एक भी पॉलिथीन थी। वो जैसे-जैसे अपने कदम अन्दर रखते जाते औरतें उनके आगे से अपने बच्चो को हटा लेती। पता नहीं किस सायें से बचना चाहती थी वो? शिवराम जी को ये सोचना ज़्यादा अनिवार्य नहीं होता था बस, आँखें यही देखती थी की जो आज तक मैं शमशाम घाट में रहकर नहीं देख पाया था वो इनको कैसे दिखता था? मुझे क्या? वो तनकर चले आते। उनका घर गली के बीच में था और गली भी इतनी चौड़ी नहीं थी की चार-पाँच आदमी उसमे से एक साथ निकल सकें। पतली गली में वो सभी के आँगनो में पाँव रखकर वो चले-चले जाते।
उनकी नज़र जब भी किसी पर पड़ती तो वो ये साफ़ देख लिया करते थे कि उनको कोई नहीं देख रहा होता सबकी नज़रें उस पर होती जो कभी काधों पर तो कभी हाथों में होता। वो ये देखकर हमेशा मुस्कुरा देते। इसलिए नहीं की ये गली वाले उन्हे ऐसे देख रहे है या आज के जमाने मे भी ये सब सोचा जाता है मगर इसलिए की अभी वो घर में घुसेगें और उनकी बीवी भी कुछ इसी नज़र से देखेगी और पता नहीं क्या-क्या पूछेगी? उन गली वालो की नज़र से ये उनको ये समझ में आने लगा था की वो जब भी घर वापस लौटते है तो वो अकेले नहीं होते उनके साथ मे कई ऐसे लोग होते थे जिनको शिवराम जी ने तो आज तक नहीं देखा था मगर उनके अलावा कई आँखों ने उन्हें देख लिया था। जिनको देखना आसान बात नहीं थी। सब के सब इस तरह से रास्ता छोड़ते जैसे शिवराम जी किसी को काँधों पर उठाकर ला रहे हो।
शिवराम जी ने अन्दर आकर कुर्सी को पहले तो अपने काँधों पर से उतारा और पॉलिथीन में रखी जूतियों को उन्होनें वहीं दरवाजे के पीछे रख दिया। ज़्यादा बड़ा कमरा नहीं है उनका। उनके सोने-बैठने की जगह बाहर वाले कमरे मे ही बनाई हुई है। वो कब आयेगें या कितने बख़्त में आयेगें? कुछ पता नहीं होता उनके घरवालों को। इसलिए वो एक खाट-बिस्तर वहीं एक कोने में दीवार से सटाकर हमेशा तय लगाकर रखते है।
अब शुरूआत हुई उस कुर्सी की जगह बनाने की। शिवराम जी उस कुर्सी की जगह अपने उसी छोटे से कमरे में बनाने लगे। कभी तो वो उस कुर्सी को अपनी खाट कर सिरहाने रखते तो कभी पातियाने पर। मन नहीं मानता था उनका। वो कुर्सी को उठाकर दूसरी दीवार की खिड़की के पास ले गए बिलकुल खिड़की के पास ही उन्होनें वो रखदी और बैठकर खिड़की के बाहर देखने लगें। उसकी ऊँचाई इतनी थी की रोज़ाना गली दिखाने वाली खिड़की आज तो कुछ और ही दिखा रही थी। खिड़की के बाहर देखने पर सामने वाले घर के अन्दर देखा जा सकता था मगर वो तो मोहम्मद भाई के घर का बाथरूम था। उन्होनें वहाँ से कुर्सी उठाई और वापस अपनी खाट के पास ले गए।
अभी के लिए उन्होने कुर्सी को ठीक खाट के बगल में ही रख दिया था। अब वो पॉलिथीन मे से जूतियाँ निकाल कर उसमे अपने पाँव घुसाने लगे। तीन जोड़ी जो पुरानी थी वो तो उनके बिलकुल ठीक ही आई थी। वो भी कैसे ना कैसे उन्होनें उसमे अपने पाँव डाल ही लिए थे मगर वो नई वाली जिसके बिनाह पर वो सारी उठा लाये थे वही नहीं आ रही थी। पूरा एक नम्बर बड़ी थी उनके वो। "शायद ये उसी दिन खरीदी होगी जिस दिन ये साहब स्वर्ग सिधारे थे। चड़ाने वाले को उनके पाँव का अन्दाजा नहीं होगा और क्यों हो भला ये अब चड़ाने के लिए ही तो थी कौन सा इनको अब पहननी थी।"
वो उन गोल्डन रंग की नई जूतियों को अपने हाथों में लेकर उसके ड़िज़ाइन को देखते रहे। कुछ खाट के जैसी बुनाई का ड़िज़ाइन था उसपर पर वो आई नहीं थी उनके। उन्होनें सारी जूतियों को खाट के नीचे सरकाया और वहीं एक-दम धड़ाम सें लेट गए। थोड़ी हो देर में वो वापस उठे और अपने तकीये में कुछ कतरन निकाली और उन्ही नई गोल्डन जूतियों को उठाया और उसके अन्दर वो कतरन फँसा कर उसे पहनने लगे। अभी भी नहीं आई थी तो उन्होनें दोबारा से और कतरन निकाली और अबकी ठीक तरह से उसमे फँसाई और पहनी। वाह!
चेहरा खिल गया था उनका वो आ गई थी। पर पाँव चैन से नहीं बैठ पा रहे थे शायद काट रही थी अभी वो नई जूतियाँ उन्हे? बड़े खुश से हुए थे कुछ पल के लिए वो और अपनी बनियान से उस जूती को साफ़ करते हुए वो वहीं लेट गए थोड़ा सुस्ताना जरूरी समझा था इतना सब कुछ हो जाने के बाद में उन्होनें।
अब उनके उस कमरे मे चार-पाँच चीजें तो ऐसी हो गई थी जिनका ठिकाना उनके घर के किसी और कमरे में तो नहीं था और कभी लड़-झगड़ के वो ठिकाना बनाना भी चाहें तो उनकी धर्मपत्नी ये काम तो कभी करने ही नहीं देगी उनकों और ना ही ये दौर कभी चलता फिर। उनकी बीवी के दिमाग पर तो बस एक ही भूत सवार रहता है कि ये एक मरे हुए आदमी का है वो भी चला आयेगा अन्दर। शिवराम जी को इस मरे हुए या समान का खौफ़, डर या ख़्याल हटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था।
वो एक ऐसी जगह में काम करते थे की जहाँ पर अपना कुछ टाइम बिता दो तो सारे डर और अवधारणाओ की जगह बदल जाती है। वो किसी कि अर्थी के पीछे-पीछे दो कदम चलना या वहाँ से वापस आकर स्नान करना सब का सब बे-माइने लगने लगता है। बस, ये सब इतना ज्ञात कराता है की हम अपने ऊपर से या तो किसी डर को निलम्बित कर रहे है या उस दुनिया में अपना सदेंशा भेज रहे हैं जो अभी तक किसी ने नहीं देखी। हम बस, इतना मानते हैं की जो मर कर जा रहा है वो देखेगा।
ये सब की सब बातें तो पूरी दुनिया सोचती तो खाली "मैं ही क्यों सोंचू" शिवराम जी ये सोच कर हमेशा अपने आपको हल्का करते। "ये सोच कर क्या फ़ायदा" कहकर अपनी छत की ओर देखकर वो घंटो ये ही सोचते रहते थे की मैं जो समान लेकर आ रहा हूँ वो क्या दूसित है? ऐसा क्या चिपक गया इसमे की ये किसी और के घर में नहीं जा सकती?
हर चीज के साथ में किसी का प्यार होता है तो किसी का रिवाज़ मगर इससे उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अब वहाँ पर पड़ी सुखती रहेगी या वो किस के लिए बन जाती है फिर? कई सारी चीजें वहाँ पर ऐसी पड़ी हुई है कि जिन्हें छूना और उन्हें वहीं पर पड़े रहने देने से एक एकांत का ज्ञात होता है कि जिनके नाम की वो चड़ाई गई है वो उसके साथ में अपनी आत्मा से जुड़ गई है। चलो कोई दे गया कुछ वो उसके लिए था जो उसे अब इस्तमाल नहीं कर पायेगा और जो इस्तमाल कर सकते हैं वो भी इस्तमाल नहीं करेगें। तो उन चीजों का होना या ना होना किस दुनिया से जुड़ जाता है। ये भयभीत है और अदृश्य दूनिया है।
शिवराम जी उन चीजों को देखकर बस, इसी धून में घूमने लगते की जैसे अभी उन चीजों मे बसे उस शख़्स से बातें कर रहे हो। बस, क्या था दूसरी तरफ से आवाज़ नहीं आ रही थी। वो उन चीजों को देखकर ये सोचने लगे की। वो कहाँ सोता होगा तो कोई चादर दे गया और खाट भी। वो कहाँ बैठता होगा तो कुर्सी दे गया। कपड़े से लेकर कोई नंगे पाँव मे जूतियाँ भी दे गया होगा ये सब क्या है? ये प्यार ही तो है ना! ये सब की सब जैसे बस, सतकार के लिए ही रह गई है। "अगर मैं मरूगाँ तो मेरी मईयत पर क्या चड़ाया जायेगा?” ये सोच कर वो हँसने लगे।
अब तो सपने भी शिवराम जी को कुछ ऐसे ही दिखाई देने लगे थे। वो रात भी इन्ही बातों के साथ में अपनी नींद पूरी कर लिया करते थे। अब तो वो गहरी नींद में सो गए थे। जब भी वो सोने के लिए लेटते तो वो अपने सारे कपड़ों को उतार कर वहीं खाट के नीचे में सरका दिया करते थे। उनके कपड़ों में एक ऐसी महक भर गई थी जिससे उनको हमेशा एक उलझन रहती थी। वो महक जो जलती हुई लकड़ियों कि थी कुछ सामाग्री जैसी। वो तो पज़ामा भी उतार दिया करते थे और गहरी नींद में इस तरह से खो जाते की कोई भी आवाज उनके कानों में कोई करकस नहीं पैदा नहीं कर सकती थी। महिने में चार ही बार उनके कपड़े धुलते और बदलते थे और उनके कपड़े धोने वाली एक ही औरत थी उनके घर में वो भी उनकी धर्मपत्नी।
ऐसा कोई भी दिन नहीं होता था जब उनकी झपड़ नहीं होती अपनी बीवी से। उनके थोड़ी देर सो जाने के बाद में उनके घर का अन्दर का दरवाजा खूलता और उनकी बीवी अपने में बड़बड़ाती हुई बाहर आती। उनके कपड़ों को उठाकर अपने कपड़ों से बचाती हुई उन्हें दूर से पकड़ती हुई घुसलखाने में डाल देती। हर बार उनके साथ मे रखी कोई ना कोई नई चीज़ नज़र आती।
हमेशा उनके एक ही तरह के बोल सुनने को मिलते थे वो हमेशा ही बड़बड़ाती हुई जब भी बाहर में आती तो उनको ही कोसती। "पता नहीं क्या अला-बला उठा लाते हैं। ये तो पूरे घर को शमशाम बना कर ही दम लेगें। खुद को तो देखो ज़रा एक दम मुर्दे की तरह हालत हो गई है। आज देखो क्या उठा लाये? अपने कपड़ों को भी घुसलखाने में भी नहीं डालते। कैसी बदबू आती है कपड़ों में से जैसे किसी की चिता जल रही हो।"
अब तो कोई असर नहीं पड़ता था शिवराम जी को। वो यूहीं बोलती-बोलती कपड़े धोने के लिए बैठ जाती। वो कपड़े धोने के बाद मे उठी और उनकी खाट के नीचे रखी उस पीली पॉलिथीन को खखोरने लगी। उसमे वही जूतियाँ थी। उन्होनें चारों जूतियों को देखा उन तीनों पुरानी जूतियों को उन्होनें बाहर दहलीज़ पर रख दिया और उन नई जूतियों को उठाकर घुसलखाने में ले गई। जिस पानी से वो कपड़े धो रही थी उसी पानी मे से हल्का सा छिड़काव उन्होनें उन जूतियों पर किया और साफ़ कपड़े से पौंछकर उन्होनें वहीं पर खाट के नीचे ऐसे रख दिया जैसे वो अभी जागेगें और उसमे पाँव डालकर बाहर चले जायेगें और कपड़ों को उठाकर वो छत पर चली गई।
लख्मी
Saturday, January 17, 2009
मेरे होने या ना होने से कुछ फ़र्क है?
आज का दिन कुछ बदला-बदला सा ही गुज़रा, दिन कि शुरूआत बहुत भीड़ से हुई। आज के दिन मेरा जाना एलएनजेपी कॉलोनी हुआ। एलएनजेपी कॉलोनी का पूरा नाम लोकनायक जयप्रकाश कॉलोनी है। ये दिल्ली की ऐसी जगह पर है जिसके एक हाथ पर नई दिल्ली है तो दूसरे हाथ पर पूरानी दिल्ली। शहर के हर बड़े काम यहीं से शुरूआत करते हैं। यानी के यहाँ से कई रैलियाँ आती तो कभी जाती है। रामलीला मैदान से राजघाट सभी को देखने आये लोग यहाँ की रैली बनते हैं। मुझे भी ये जगह बहुत भाती है और सबसे ज़्यादा यहाँ के रिक्शे की सवारी। जिसमे बैठने का मतलब है कि आप कितने अपने को लेकर सावधान रहते हैं उसका इम्तिहान हो जाता है। जो दिल्ली इस सवारी से दिखती है वैसी तो शायद कभी देखी ही नहीं होगी। ये तो मेरी गांरटी है।
जहाँ पर तंग गलियों मे भी रिक्शे ऐसे भागते हैं कि सड़क पर चलती मर्सिडीज़ कार। वैसे यहाँ की तो ये ही मर्सिडिज़ कार हैं और यही हवाई जहाज। बस, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर कभी आप मेरी इस बात से इम्प्रैस होकर रिक्शे की सवारी निकल पड़ो तो उसपर बैठते समय अपने पाँव रिक्शा चलाने वाले की सीट के नीचे कसकर बैठना। क्योंकि इस सफ़र मे कब ब्रैक लग जाये वो कहा नहीं जा सकता। वहाँ अगर किसी को रिक्से पर बैठा देखोगे तो कहोगे की ये बात तो आपने गलत कही है लेकिन वो लोग यहाँ के माहौल मे ऐसे रम गए है कि उन्हे तेज ब्रैक लगने पर भी अहसास नहीं होता कि हम हिले हैं तो चाहें धरती हिले या कोई भुचाल आये उन्हे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बिलकुल बस, के कंडेक्टर की तरह बन गए हैं। जो आपको बनने मे वक़्त लगेगा।
मेरे लिए आज बस्ती भी कुछ अलग ही थी। लग रहा था की पिछली रात मे कुछ गुज़रा है। उसी की गर्मी बातों मे फैली थी। दिल्ली शहर मे कोई भी बदलाव हो यहाँ पर उसकी परछाई को बखूबी महसूस किया जा सकता है। एक बात अगर मुँह से निकल गई तो वो जब तक यहाँ की हर गली मे भम्रण नहीं कर लेती तब तक वो वापस उसी ज़ुबान में नहीं आती।
एक अंधेरे कमरे में चार औरतें बैठी बातें कर रही थी। वहीं पर मेरी साथी भी थी जिससे मैं मिलने के लिए गया था। वो इसी बस्ती में रहती भी है और साथ-साथ एक ऐसे संदर्भ से भी जुड़ी हुई है जो लोगों के बीच में रहकर उनके जीवन के तरीको और हर अहसास को बाँटने का काम करते हैं। ये वे नज़र लिए रहते हैं जो शहर की नज़र के अन्दर से कुछ अपना खोजती है। वे जगहें बनाती है जहाँ पर किसी को भी न्यौता है वो वहाँ आकर अपने जीवन से संबधित और फैसलों को बाँट सकता है। ये एक बहुत बेहतरीन काम है। मगर मैं इसे काम नहीं मानता, मेरे लिए तो ये एक ऐसा रिश्ता है जो हर आदमी तलाशता है। जैसे हम इस रिश्ते की तमन्ना या उम्मीद लगाकर रखते हैं जो हमारे जीवन में कुछ घटना हो जाने के बाद में आता है। जो खाली साहस ही ना बाँधे बल्की उन सभी बातों को समझने में मदद करे जो आने वाले जीवन मे अपनी भूमिका बनायेगी।
मेरी साथी अपने मे उस रूप को बनाने की कोशिश करती है। आज यहाँ पर बातें कुछ अलग ही थी। आज अपने से कुछ सवाल किए जा रहे थे। उन्होंने मेरे वहाँ पहुँते ही एक बात पूछी, "पिछले दिनों यहाँ पर एक सर्वे हुआ, जो बस्ती को विस्थापन करने से पहले किया जाता है। लेकिन यहाँ के लोगों ने उन्हे मार-फटकार कर भगा दिया। उनका मानना है की पहले हमारे कुछ सवालों के जवाब दिये जाये उसके बाद मे हम सर्वे होने देगें। जो बात उनकी भी ठीक ही है। लेकिन, हमें ये तक नहीं पता कि ये सर्वे किस चीज के थे? कुछ जाने-माने लोगों ने ये रुकवा दिये। अब जब हम बस्ती मे निकलते है लोगों के साथ बातचीत करने के लिए या उनकी कलाओ के लिए माहौल बनाना के लिए तो वो हमसे कहते हैं, हम यहाँ कब तक रहेगें जो आप हमारी कलाओ की बात कर रही है? और सब कुछ जैसे रुक जाता है। हम क्या कहें? "
इसके बारे में तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता था। खाली यही के शहर में बदलाव मे जो फैसले सरकार ले लेती है तो उसको खाली मानना ही पड़ता है। बस, हमारी ताकत यही है की यहाँ पर बिताये हमारे जीवन के साल और उसके सबूत। जो ये नहीं होगे की हमने यहाँ कितने बेटे-बेटियों की शादी की है या कितने मौसम झेले हैं बस, हमारे पास होने चाहिये कुछ कागज़। जिसपर सरकारी मोहर लगी है। वही है हमारी ताकत। इसके अलावा तो मेरे पास बोले के लिए कुछ नहीं था।
उन्होंने फिर से कुछ पूछा वे बोले, "यहाँ पर कई ऐसी औरते हैं तो 20-20 सालों से अपने घर से बाहर नहीं निकली। बस, घर ही मे रहकर उन्होंने अपने घर को संभाला है। वे जब हमसे ये कहती हैं कि हम यहाँ से कहाँ जायेगें? और यहाँ से पास कौन सी जगह पड़ेगी या वहाँ पर मेरे बच्चो का गुजारा होगा तो हम कुछ कह नहीं पाते। एक बात है, यहाँ पर लोगों ने जो अपनी कला या हुनर से कुछ काम तैयार किए हैं शहर मे अपनी पहचान बनाने के लिए उसकी भविष्य क्या है फिर? यही सवाल अब कलाओ के बीच मे बाधा बन रहे हैं।"
ये लड़ाई बहुत पुरानी है, शहर से घर और जीने के लिए जगह माँगने की। लेकिन ये रसम रखी की रखी रही है। ये एक ऐसी बहस है जिसका कोई अंत नहीं है। बस, अपना आधार ही साहस है। यही सजाना है और बनाना है। लेकिन फिर भी मैं उनकी उस बैचेनी को नहीं जान पाया था जो उनमे उफान मार रही थी। वो थी, कलाओ के बारे मे। इसको उभाराना जितना मुश्किल है उतना ही उसको दबते देखना। ये सीधा आने वाले टाइम पर अटेक करता है।
बस्ती मे इसी की बैचेनी थी जो आज महसूस हो रही थी। चाय की दुकान के सामने से लेकर कुछ माहौल तक। पर इसके बावज़ूद एक आरामदायक अहसास भी था। जैसे इस बात से परहेज नहीं है। बस, जुझने के तरीके में खटास है। जो जीने के तरीके के समान हो गई है।
मेरी साथी मुझे लेकर बाहर वाले कमरे मे आ गई। जहाँ से बस्ती बिलकुल साफ दिखती है और उसकी चहलकदमी की आवाजें भी साफ सुनाई देती हैं। वो मुझे बाहर का नज़ारा बताने लगी। वो बता रही थी, "यहाँ पर घरों में एक बहुत ही प्यारी बात चलती है जो अब जैसे रिवाज़ ही बन गई है। यहाँ हर घर का, एक ना एक पाठक जरूर है।"
मैं समझा नहीं, वे फिर से बोली, "यहाँ हर घर अपने पड़ोस में एक ना एक आदमी या कहलो एक ना एक शख़्स, जो कोई औरत भी हो सकती है और लड़की भी, उसको अपने घर मे कुछ भी बनता है उसे चख़ाने लिए जरूर भेजता है। जो उसके स्वाद को बताता है और हिस्सेदार बनता है। फिर वो जिस कटोरी मे वो खाना भेजा गया था उसी कटोरी मे अपने घर से कुछ भेजती है। फिर वो कटोरी घूमती है घर-घर और स्वाद का एक घेहरा सा बना लेती है। जो बिना किसी बात के घूमता है। ये रीत सी बन गई है। हर घर का कोई ना कोई तो है। हर दिन, रात हो या कोई त्यौहार, ये हर दिन मे तब्दील हो जाते है। कुछ ही देर मे इतनी कटोरियाँ जमा हो जाती है कि हर स्वाद का चटखारा लेने मे मज़ा आता है। कभी-कभी सोचती हूँ की ये खाली पकवान या खाने के साथ ही जुड़ा है या किसी और भी चीजों की संभावनायें लिए ये चलता है? जो घर से घर जा रहा है और मोहल्ले से मोहल्ले वो क्या है? खाली रिश्ता ही तो नहीं है। ये तो कुछ और है? वो ही मैं समझ नहीं पाती।
इस जगह मे जो रेखायें हैं वो यही है, जो नज़र तो नहीं आती मगर बहुत कड़ी हैं। जिसकी आड़ मे कई और रेखायें खींची हैं। जिसके बलबूते पर ये बुनियादें खड़ी हैं। कहानियों की, कलाओ की, तीज़-त्यौहारों की और जिनमे बातों के कुन्दे लटके हैं। एक-दूसरे से जुड़े हुए।
वो कहती-कहती रुक गई, लेकिन उसके होंठ कुलबुला रहे थे। शायद बहुत सारे शब्द रूक गए थे मुँह के अन्दर ही। पर ऐसा नहीं है की वे बाहर नहीं निकलेगें। वो बस, वक़्त की नज़ाकत पर निर्भर हो गए हैं। वो बाहर आने का रास्ता खोज़ नहीं रहे बल्की खुद ही बना रहे हैं।
वो जाते-जाते एक बात और बोली, "एक बात मैं काफी दिन से सोच रही हूँ, मैं यहाँ पर रहती हूँ पिछले 20 सालों से और मेरा घर यहाँ पर है पिछले 30 सालों से। लेकिन मैं वो क्यों नहीं पकड़ पाती जो यहाँ पर एक महिना, दो महिना गुजारने वाले पकड़ लेते हैं? अपनी जगह को, जहाँ पर रहते हैं उसको समझने के लिए क्या हमें किसी प्रकार की दूरी की जरूरत होती है या नजदीकी की। मैं पिछले 12 सालों की बात कहूँ तो मैंने बहुत से बदलाव देखे हैं लेकिन उन बदलावों को मेरी जरूरत नहीं थी, वे तो होने ही थे लेकिन वो बदलाव मेरे जीवन पर भी गहरी छाप छोड़ते हैं तो मैं क्या छोड़ रही हूँ?
ये सवाल मेरे लिए भी सुने-सुनाये नहीं थे या मैं अपने बने-बनाये समीकरण से इसका जवाब नहीं दे सकता था। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं वो कह पाता जो मैं अपने घर के पास होते बदलाव या शहर मे होते बदलाव को अपने घर मे नहीं महसूस करता। क्या ये बदलाव होने और मेरे साथ होने मे फ़र्क होता है? मेरा होना जरूरी नहीं है लेकिन मेरे साथ होना तय है। ये क्या रेखायें खींचते हैं? जैसे मेरे एक और साथी ने एक सवाल किया था मुझसे जो बिलकुल ऐसा ही था। उसने कहा था, जिस स्कूल मे हम बस्ता लेकर जाते है, पढ़ने के लिए, वर्दी पहनकर। रोज जाते हैं। लेकिन स्कूल छोड़ने के बाद मे हम उसी स्कूल मे आज जाये हाथ मे कैमरा लेकर तस्वीरें खींचने के लिए तो क्या नज़र होगी हमारी?
ये सवाल बहुत छोटा था पर इसका आधार गहरा था जो आज समझ मे आ रहा था। हम अपनी जगह से, जहाँ पर हम रहते हैं उससे क्या नाता बनाकर रखते हैं जिससे कुछ जगहें नज़रअंदाज हो जाती है? ये नजदीकी और दूरी का रिश्ता क्या है? बदलाव से और होने या न होने से।
दिन का अंत यही सोचते-सोचते हुआ लेकिन नज़र फिर से उस सड़क पर चली गई जहाँ से ये बस्ती पूरी नज़र आती है। अपने मे खोई हुई और अपनी ही आवाजों मे गुम सी हुई।
लख्मी
जहाँ पर तंग गलियों मे भी रिक्शे ऐसे भागते हैं कि सड़क पर चलती मर्सिडीज़ कार। वैसे यहाँ की तो ये ही मर्सिडिज़ कार हैं और यही हवाई जहाज। बस, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर कभी आप मेरी इस बात से इम्प्रैस होकर रिक्शे की सवारी निकल पड़ो तो उसपर बैठते समय अपने पाँव रिक्शा चलाने वाले की सीट के नीचे कसकर बैठना। क्योंकि इस सफ़र मे कब ब्रैक लग जाये वो कहा नहीं जा सकता। वहाँ अगर किसी को रिक्से पर बैठा देखोगे तो कहोगे की ये बात तो आपने गलत कही है लेकिन वो लोग यहाँ के माहौल मे ऐसे रम गए है कि उन्हे तेज ब्रैक लगने पर भी अहसास नहीं होता कि हम हिले हैं तो चाहें धरती हिले या कोई भुचाल आये उन्हे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बिलकुल बस, के कंडेक्टर की तरह बन गए हैं। जो आपको बनने मे वक़्त लगेगा।
मेरे लिए आज बस्ती भी कुछ अलग ही थी। लग रहा था की पिछली रात मे कुछ गुज़रा है। उसी की गर्मी बातों मे फैली थी। दिल्ली शहर मे कोई भी बदलाव हो यहाँ पर उसकी परछाई को बखूबी महसूस किया जा सकता है। एक बात अगर मुँह से निकल गई तो वो जब तक यहाँ की हर गली मे भम्रण नहीं कर लेती तब तक वो वापस उसी ज़ुबान में नहीं आती।
एक अंधेरे कमरे में चार औरतें बैठी बातें कर रही थी। वहीं पर मेरी साथी भी थी जिससे मैं मिलने के लिए गया था। वो इसी बस्ती में रहती भी है और साथ-साथ एक ऐसे संदर्भ से भी जुड़ी हुई है जो लोगों के बीच में रहकर उनके जीवन के तरीको और हर अहसास को बाँटने का काम करते हैं। ये वे नज़र लिए रहते हैं जो शहर की नज़र के अन्दर से कुछ अपना खोजती है। वे जगहें बनाती है जहाँ पर किसी को भी न्यौता है वो वहाँ आकर अपने जीवन से संबधित और फैसलों को बाँट सकता है। ये एक बहुत बेहतरीन काम है। मगर मैं इसे काम नहीं मानता, मेरे लिए तो ये एक ऐसा रिश्ता है जो हर आदमी तलाशता है। जैसे हम इस रिश्ते की तमन्ना या उम्मीद लगाकर रखते हैं जो हमारे जीवन में कुछ घटना हो जाने के बाद में आता है। जो खाली साहस ही ना बाँधे बल्की उन सभी बातों को समझने में मदद करे जो आने वाले जीवन मे अपनी भूमिका बनायेगी।
मेरी साथी अपने मे उस रूप को बनाने की कोशिश करती है। आज यहाँ पर बातें कुछ अलग ही थी। आज अपने से कुछ सवाल किए जा रहे थे। उन्होंने मेरे वहाँ पहुँते ही एक बात पूछी, "पिछले दिनों यहाँ पर एक सर्वे हुआ, जो बस्ती को विस्थापन करने से पहले किया जाता है। लेकिन यहाँ के लोगों ने उन्हे मार-फटकार कर भगा दिया। उनका मानना है की पहले हमारे कुछ सवालों के जवाब दिये जाये उसके बाद मे हम सर्वे होने देगें। जो बात उनकी भी ठीक ही है। लेकिन, हमें ये तक नहीं पता कि ये सर्वे किस चीज के थे? कुछ जाने-माने लोगों ने ये रुकवा दिये। अब जब हम बस्ती मे निकलते है लोगों के साथ बातचीत करने के लिए या उनकी कलाओ के लिए माहौल बनाना के लिए तो वो हमसे कहते हैं, हम यहाँ कब तक रहेगें जो आप हमारी कलाओ की बात कर रही है? और सब कुछ जैसे रुक जाता है। हम क्या कहें? "
इसके बारे में तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता था। खाली यही के शहर में बदलाव मे जो फैसले सरकार ले लेती है तो उसको खाली मानना ही पड़ता है। बस, हमारी ताकत यही है की यहाँ पर बिताये हमारे जीवन के साल और उसके सबूत। जो ये नहीं होगे की हमने यहाँ कितने बेटे-बेटियों की शादी की है या कितने मौसम झेले हैं बस, हमारे पास होने चाहिये कुछ कागज़। जिसपर सरकारी मोहर लगी है। वही है हमारी ताकत। इसके अलावा तो मेरे पास बोले के लिए कुछ नहीं था।
उन्होंने फिर से कुछ पूछा वे बोले, "यहाँ पर कई ऐसी औरते हैं तो 20-20 सालों से अपने घर से बाहर नहीं निकली। बस, घर ही मे रहकर उन्होंने अपने घर को संभाला है। वे जब हमसे ये कहती हैं कि हम यहाँ से कहाँ जायेगें? और यहाँ से पास कौन सी जगह पड़ेगी या वहाँ पर मेरे बच्चो का गुजारा होगा तो हम कुछ कह नहीं पाते। एक बात है, यहाँ पर लोगों ने जो अपनी कला या हुनर से कुछ काम तैयार किए हैं शहर मे अपनी पहचान बनाने के लिए उसकी भविष्य क्या है फिर? यही सवाल अब कलाओ के बीच मे बाधा बन रहे हैं।"
ये लड़ाई बहुत पुरानी है, शहर से घर और जीने के लिए जगह माँगने की। लेकिन ये रसम रखी की रखी रही है। ये एक ऐसी बहस है जिसका कोई अंत नहीं है। बस, अपना आधार ही साहस है। यही सजाना है और बनाना है। लेकिन फिर भी मैं उनकी उस बैचेनी को नहीं जान पाया था जो उनमे उफान मार रही थी। वो थी, कलाओ के बारे मे। इसको उभाराना जितना मुश्किल है उतना ही उसको दबते देखना। ये सीधा आने वाले टाइम पर अटेक करता है।
बस्ती मे इसी की बैचेनी थी जो आज महसूस हो रही थी। चाय की दुकान के सामने से लेकर कुछ माहौल तक। पर इसके बावज़ूद एक आरामदायक अहसास भी था। जैसे इस बात से परहेज नहीं है। बस, जुझने के तरीके में खटास है। जो जीने के तरीके के समान हो गई है।
मेरी साथी मुझे लेकर बाहर वाले कमरे मे आ गई। जहाँ से बस्ती बिलकुल साफ दिखती है और उसकी चहलकदमी की आवाजें भी साफ सुनाई देती हैं। वो मुझे बाहर का नज़ारा बताने लगी। वो बता रही थी, "यहाँ पर घरों में एक बहुत ही प्यारी बात चलती है जो अब जैसे रिवाज़ ही बन गई है। यहाँ हर घर का, एक ना एक पाठक जरूर है।"
मैं समझा नहीं, वे फिर से बोली, "यहाँ हर घर अपने पड़ोस में एक ना एक आदमी या कहलो एक ना एक शख़्स, जो कोई औरत भी हो सकती है और लड़की भी, उसको अपने घर मे कुछ भी बनता है उसे चख़ाने लिए जरूर भेजता है। जो उसके स्वाद को बताता है और हिस्सेदार बनता है। फिर वो जिस कटोरी मे वो खाना भेजा गया था उसी कटोरी मे अपने घर से कुछ भेजती है। फिर वो कटोरी घूमती है घर-घर और स्वाद का एक घेहरा सा बना लेती है। जो बिना किसी बात के घूमता है। ये रीत सी बन गई है। हर घर का कोई ना कोई तो है। हर दिन, रात हो या कोई त्यौहार, ये हर दिन मे तब्दील हो जाते है। कुछ ही देर मे इतनी कटोरियाँ जमा हो जाती है कि हर स्वाद का चटखारा लेने मे मज़ा आता है। कभी-कभी सोचती हूँ की ये खाली पकवान या खाने के साथ ही जुड़ा है या किसी और भी चीजों की संभावनायें लिए ये चलता है? जो घर से घर जा रहा है और मोहल्ले से मोहल्ले वो क्या है? खाली रिश्ता ही तो नहीं है। ये तो कुछ और है? वो ही मैं समझ नहीं पाती।
इस जगह मे जो रेखायें हैं वो यही है, जो नज़र तो नहीं आती मगर बहुत कड़ी हैं। जिसकी आड़ मे कई और रेखायें खींची हैं। जिसके बलबूते पर ये बुनियादें खड़ी हैं। कहानियों की, कलाओ की, तीज़-त्यौहारों की और जिनमे बातों के कुन्दे लटके हैं। एक-दूसरे से जुड़े हुए।
वो कहती-कहती रुक गई, लेकिन उसके होंठ कुलबुला रहे थे। शायद बहुत सारे शब्द रूक गए थे मुँह के अन्दर ही। पर ऐसा नहीं है की वे बाहर नहीं निकलेगें। वो बस, वक़्त की नज़ाकत पर निर्भर हो गए हैं। वो बाहर आने का रास्ता खोज़ नहीं रहे बल्की खुद ही बना रहे हैं।
वो जाते-जाते एक बात और बोली, "एक बात मैं काफी दिन से सोच रही हूँ, मैं यहाँ पर रहती हूँ पिछले 20 सालों से और मेरा घर यहाँ पर है पिछले 30 सालों से। लेकिन मैं वो क्यों नहीं पकड़ पाती जो यहाँ पर एक महिना, दो महिना गुजारने वाले पकड़ लेते हैं? अपनी जगह को, जहाँ पर रहते हैं उसको समझने के लिए क्या हमें किसी प्रकार की दूरी की जरूरत होती है या नजदीकी की। मैं पिछले 12 सालों की बात कहूँ तो मैंने बहुत से बदलाव देखे हैं लेकिन उन बदलावों को मेरी जरूरत नहीं थी, वे तो होने ही थे लेकिन वो बदलाव मेरे जीवन पर भी गहरी छाप छोड़ते हैं तो मैं क्या छोड़ रही हूँ?
ये सवाल मेरे लिए भी सुने-सुनाये नहीं थे या मैं अपने बने-बनाये समीकरण से इसका जवाब नहीं दे सकता था। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं वो कह पाता जो मैं अपने घर के पास होते बदलाव या शहर मे होते बदलाव को अपने घर मे नहीं महसूस करता। क्या ये बदलाव होने और मेरे साथ होने मे फ़र्क होता है? मेरा होना जरूरी नहीं है लेकिन मेरे साथ होना तय है। ये क्या रेखायें खींचते हैं? जैसे मेरे एक और साथी ने एक सवाल किया था मुझसे जो बिलकुल ऐसा ही था। उसने कहा था, जिस स्कूल मे हम बस्ता लेकर जाते है, पढ़ने के लिए, वर्दी पहनकर। रोज जाते हैं। लेकिन स्कूल छोड़ने के बाद मे हम उसी स्कूल मे आज जाये हाथ मे कैमरा लेकर तस्वीरें खींचने के लिए तो क्या नज़र होगी हमारी?
ये सवाल बहुत छोटा था पर इसका आधार गहरा था जो आज समझ मे आ रहा था। हम अपनी जगह से, जहाँ पर हम रहते हैं उससे क्या नाता बनाकर रखते हैं जिससे कुछ जगहें नज़रअंदाज हो जाती है? ये नजदीकी और दूरी का रिश्ता क्या है? बदलाव से और होने या न होने से।
दिन का अंत यही सोचते-सोचते हुआ लेकिन नज़र फिर से उस सड़क पर चली गई जहाँ से ये बस्ती पूरी नज़र आती है। अपने मे खोई हुई और अपनी ही आवाजों मे गुम सी हुई।
लख्मी
Thursday, January 15, 2009
किसने किया, मुँह बन्द
मँहगाई गरीबी ज़ुर्म और घोटाला
इन पर नहीं प्रतिबंध होने वाला
क्या अर्थ है समाज का समझ नहीं आता
अपने हाथों से ही अपनी पहचान को मिटा डाला
फिर वर्तमान समस्या का हल निकाल डाला
लोग कहते हैं,सरकार ने विकास की ओर जाते-जाते मंदी की खाई में धकेल डाला
वो तो भला हो मैटो वालो का की जम़ीन खोदकर हमें निकाल डाला
खुदाई चलती रही कार्यशैलियों की रफ़्तार भी थम गई
किसने कारीगरों के हाथों पर तेजाब डाला
मशीनों की रणनिती ने किया इंसानो पर राज
क्या करे विदेश मुद्रा ने हम को खरीद डाला
आज देश है पर्यटक स्थल,
क्योंकि यहाँ है विदेशी पंछियों का बोल-बाला
सोने की चिडिया था जो भारत
आज वो बना रोबॉट मतवाला
जिसकी संवेदनाए मर गई है
चूके अपने हाथों ने ही उसका दिल निकाल डाला
आज भी होते है आदोंलन,
क्योंकि अधिकारों का नहीं कोई रखवाला
दुष्कर्म रोज होते हैं, ज़ुर्म के मुँह पर कौन मारे ताला
राकेश
इन पर नहीं प्रतिबंध होने वाला
क्या अर्थ है समाज का समझ नहीं आता
अपने हाथों से ही अपनी पहचान को मिटा डाला
फिर वर्तमान समस्या का हल निकाल डाला
लोग कहते हैं,सरकार ने विकास की ओर जाते-जाते मंदी की खाई में धकेल डाला
वो तो भला हो मैटो वालो का की जम़ीन खोदकर हमें निकाल डाला
खुदाई चलती रही कार्यशैलियों की रफ़्तार भी थम गई
किसने कारीगरों के हाथों पर तेजाब डाला
मशीनों की रणनिती ने किया इंसानो पर राज
क्या करे विदेश मुद्रा ने हम को खरीद डाला
आज देश है पर्यटक स्थल,
क्योंकि यहाँ है विदेशी पंछियों का बोल-बाला
सोने की चिडिया था जो भारत
आज वो बना रोबॉट मतवाला
जिसकी संवेदनाए मर गई है
चूके अपने हाथों ने ही उसका दिल निकाल डाला
आज भी होते है आदोंलन,
क्योंकि अधिकारों का नहीं कोई रखवाला
दुष्कर्म रोज होते हैं, ज़ुर्म के मुँह पर कौन मारे ताला
राकेश
हड़ताल में पूरा शहर है अटका
ज़िन्दगी के आठ दिन
कटे तारे गिन-गिन
राशन ख़त्म, भाषण ख़त्म
हुआ बाजारों में आने वाला माल ख़त्म
माँगे बनी हड़ताल का कारण
प्लेटफ़ोर्म ख़ाली रेल बिन
गाड़ी रुकी तेल बिन
जिसको देखो सिर पकड़े बैठा, टूटे हड़ताल इस ताक में रहता
पर हड़ताल एक सच्चाई है, जिसने अत्याचार पर आवाज उठाई है
एक ही मुद्दा नहीं अपने बीच यारों, न जाने कितने मुद्दों की तो अभी बारी नहीं आई है
मंदी की चपेट में आया जीवन, सरकार ने ऐसी कूटनिती कुछ ऐसी बनाई है
इन आठ दिनों ने दिया है झटका
हड़ताल में पूरा शहर है अटका
जब टूटी हड़ताल तो सब का दिल मटका
रुक न जाये अर्थव्यवस्था का पहिया
जरा जमकर जोर लगाना भईया
खुली हड़ताल तो राहत पाई है
माँगे पूरी हुई तो सूकून से रोटी खाई है।
राकेश
कटे तारे गिन-गिन
राशन ख़त्म, भाषण ख़त्म
हुआ बाजारों में आने वाला माल ख़त्म
माँगे बनी हड़ताल का कारण
प्लेटफ़ोर्म ख़ाली रेल बिन
गाड़ी रुकी तेल बिन
जिसको देखो सिर पकड़े बैठा, टूटे हड़ताल इस ताक में रहता
पर हड़ताल एक सच्चाई है, जिसने अत्याचार पर आवाज उठाई है
एक ही मुद्दा नहीं अपने बीच यारों, न जाने कितने मुद्दों की तो अभी बारी नहीं आई है
मंदी की चपेट में आया जीवन, सरकार ने ऐसी कूटनिती कुछ ऐसी बनाई है
इन आठ दिनों ने दिया है झटका
हड़ताल में पूरा शहर है अटका
जब टूटी हड़ताल तो सब का दिल मटका
रुक न जाये अर्थव्यवस्था का पहिया
जरा जमकर जोर लगाना भईया
खुली हड़ताल तो राहत पाई है
माँगे पूरी हुई तो सूकून से रोटी खाई है।
राकेश
Tuesday, January 13, 2009
ये नोर्मल तस्वीर क्या है?
कल एक अजीब सी बात हुई, ये बहुत ही सोचने के लायक थी। ऐसा नहीं है कि ये कभी सुना या सोचा नहीं है लेकिन ये तो एकदम गज़ब ही था। कल मेरा जाना एक सरकारी दफ़्तर में हुआ। जिसमे मुझसे कुछ डॉकोमेन्टस माँगे गए। जैसे- राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फोटो, स्कूल का सार्टीविकेट, वोटर आई कार्ड वगैरह। उसके साथ-साथ एक फोर्म भी भरना था जो उन्ही ने ही दिया था। मैं वो फोर्म भरकर और ये सारे काग़जात लेकर उसी ऑफिस मे पँहुच गया। उन्होंने मेरे सारे काग़जात देखे और फोटो को देखते हुए कहा, "ये क्या तस्वीर है? आपको पता नहीं है कि पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर कैसे खिंचवाई जाती है, इसमे चेहरे को नोर्मल रखना होता है। ये क्या तस्वीर। है? ये नहीं चलेगी, जाइये दोबारा लेकर आईये।"
उनकी ये बात सुनकर मैं वापस अपने घर चला आया। मैंने कोई बेकार तस्वीर थोड़ी खिंचवाई थी। मेरा एक दोस्त गोविंदा का बहुत बड़ा फैन है तो वो जब भी तस्वीर खिंचवाता था तो अपने चेहरे को हमेशा गोविंदा अंदाज़ में बना लेता था फिर चाहें वो पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर हो या पोस्टकार्ड साइज़ की। मैंने भी तो कुछ ऐसा ही तो किया था। इसमे हर्ज़ ही क्या था?
मगर उस ऑफिसर ने कहा था की नोर्मल तस्वीर होनी चाहिये। ये रटता हुआ मैं फोटोग्राफर के पास में गया। उससे मैंने कहा, "भाई साहब एक पासपोर्ट साइज़ में तस्वीर खिंचवानी है लेकिन फोटो नोर्मल होनी चाहिये।"
वे ये सुनकर हँसने लगा और कहने लगा, "सर चिंता मत किजिये आप, फोटो एकदम नोर्मल होगी।"
उसने मुझे अपने अन्दर वाले कमरे में बैठा दिया। सामने का पर्दा लगाया और लाइट को बन्द कर दिया। ये एक छोटा सा कमरा था। यहाँ का नया फोटोस्टुडियो था ये। पीछे सफेद रंग का पर्दा खींचा और सामने लगी टेबल पर उसने मुझे बैठा दिया। उसके बाद वो मेरे चेहरे की तरफ़ में आया और देखने लगा। मैंने उससे कहा, "भाईसाहब ये नोर्मल होना क्या होता है? ये चेहरा नोर्मल है ये कैसे पता चलता है? हम हर तस्वीर में अपनी अदा दिखा सकते हैं अलग-अलग भाव भी ला सकते हैं तो ये पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर में क्यों नहीं?"
उसको पता चल गया था कि आज उसको क्या कहा जा रहा हैं। वो कुछ ना बोलते हुए बस, मेरी तरफ़ देखकर हँसने लगा। फिर बोला, "ये बताया नहीं जा सकता सर, पर हाँ मैं जो तस्वीर खींचूगा वो नोर्मल होगी, एकदम आम आदमी की।"
वो ये कहते हुए मेरी तरफ में आया और मेरी कमीज़ ठीक करते हुए बोला, "सर आप बस, मेरी तरफ देखिये। चेहरे को एकदम ढीला छोड़ दिजिये। आँखें एकदम सामने। जब तक मैं ना कहूँ पलक मत झपकना। अपनी बॉडी को थोड़ा हल्का किजिये, हाँ एकदम सही। सीना टाइट कर लिजिये। हाथों को अपने घुटनों पर रख लिजिये। चेहरा थोड़ा नीचे की तरफ, गर्दन का कंठ नहीं नज़र आना चाहिये। आँखें बड़ी मत किजिये, एकदम रिलेक्स होकर बैठिये। एक मिनट में बस, आपका फोटो खिंच जायेगा।"
वो मेरी कमीज को दोबारा से ठीक करते हुए वापस अपनी जगह पर गया। उसकी दूरी लगभग चार फीट की थी। एक बड़ा सा कैमरा मेरे ऊपर ताना हुआ था और बगल में जलती लाइट मेरे मुँह पर पड़ रही थी। मेरा चेहरा लगभग चमक रहा था। ऐसा लग रहा था की जैसे जीरो वॉट का बल्ब मेरे चेहरे पर ही जल रहा हो। इसके बाद मे दो बार कैमरे का फ्लैस मेरे चेहरे पर पड़ा और तस्वीर खिंच गई।
वो मेरी तरफ मे देखते हुए बोला, "लिजिये सर खिंच गई आपकी नोर्मल तस्वीर।"
इस बार मैं हँसा और उससे कहा, "भाई साहब एक बात बताइये ये कौन सा वाला नोर्मल है? डॉक्टर जो कहता है वो वाला नोर्मल? या उस सरकारी आदमी ने जो माँगा वो वाला? फ़िल्मों में जो नज़र आता है वो वाला या आपने जो खींचा वो वाला?"
फोटोग्राफ़र बोला, "सर, ये सारा है। ये वो भी है जो डॉक्टर कहता है और वो वाला भी है जो उस सरकारी आदमी ने माँगा था और ये वो वाला भी है जो मैंने खींचा है। बेसिक्ली ये नोर्मल इंसान वो है जिसकी डिंमाड सबसे ज़्यादा है। मगर ये ही नहीं मिलता।"
"तो क्या मिलता है भाई साहब यहाँ?" मैंने कहा।
फोटोग्राफ़र बोला, "यहाँ पर सब कुछ मिलावट का समान मिलता है। ये मिलावट आपको पता है क्या है। यही तो मस्ती है। यहाँ पर हर कामों मे अलग-अलग चीज चाहिये। तो लोग उसी हिसाब से बँट जाते हैं। जैंसे जो शादी के लिए चाहिये वे अलग है, सरकारी कामों मे अलग, पोज़िंग के लिए अलग, पोर्टपोलियों के अलग और अब तो हैंटीकेप के सार्टीविकेट के लिए भी अलग तो लोग भी उसी के हिसाब से अपने आपको बदल लेते हैं।"
"एक बात बताइये भाईसाहब, आपने ये अलग-अलग महकमों और कामों मे चेहरे बनाने की डिंमाड को कैसे जाना?" मैंने कहा।
फोटोग्राफ़र बोला, "सबसे पहली बात तो ये की मैं भी तो इसी दुनिया में रहता हूँ। इसलिए जो भी यहाँ होता है तो मेरे साथ भी होता है। दूसरा ये की, हमें चेहरों के भाव से, एक्ट से खेलना आना चाहिये तभी तो ये काम है, नहीं तो हमें आता क्या है और सही बात बताऊँ, वो ये की यहाँ पर ये खेल सबको आता है।"
मैंने कहा, "तो ये खेल हर साइज़ के फोटो के साथ खेला जाता है? किस साइज के साथ में कौन सा खेल है ये कैसे बन गया?"
फोटोग्राफ़र बोला, "मेरे हिसाब से तो खाली दो ही तरह के भाव हैं इस दुनिया में। जिसमे से एक हमने बनाया है दूसरा जो हमने नहीं बनाया। बस, उसे मान लिया है। पहला तो ये ही जो आपने खिंचवाया। पासपोर्ट साइज़ का खेल। नोर्मल फोटो, और दूसरा जो खुलकर आता है वो है कि किसी भी साइज़ में आप किसी भी तरह का भाव अपने चेहरे में ला सकते हो।"
"तो ये नोर्मल होना और बाकी का होना क्या है? क्या वो नोर्मल नहीं है?" मैंने कहा।
फोटोग्राफ़र ने कहा, "ये नोर्मल होना कुछ नहीं होता। ये सब बस, माँग है। सरकार को लगता की हम एक ऐसा चेहरा बनाके उसको दे जिसमे कुछ भी अलग से मिलाया ना गया हो। सरकार समझती है की आदमी मे रोना, हँसना, तेडूपंती या स्टाइल सब अलग से आई हैं। ये ऊपर वाले ने नहीं दी। तो सरकार वो चेहरा माँगती है।"
ये माँग के साथ में चेहरे का होना ये तो बहुत कस देता होगा। ये कसा हुआ भी ना लगे और खूबसूरत भी लगे ये कैसे करते फिर?" मैंने कहा।
फोटोग्राफ़र ने कहा, "सर, यही तो हमारा काम है। एक बात कहे आपसे, जब कोई अपनी फोटो खिंचवाता है तो वो हमेशा ये सोचता है कि जब वे अपनी खींची हुई तस्वीर को देखे तो उसे लगता चाहिये की उसका चेहरा ऐसा दिखता है। जो उसे शीसे में नहीं दिखता वो तस्वीर में दिखना चाहिये बस, कोई-कोई अपनी पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर को ही बड़ा करवा लेता है। कभी-कभी तो फ्रैम भी।"
"आपको क्या है लगता है अभी तक जितनी भी तस्वीरें आपने खींची हैं उन तस्वीरों मे से कितनी नोर्मल है और कितनी नहीं?" मैंने कहा।
फोटोग्राफ़र ने कहा, "आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे ये देखिये।"
उसने मेरे सामने काफी सारी तस्वीरें बिछा दी। जिसमे बहुत सारे लोगों की तस्वीरें थी। पहली फैमली फोटो थी। जिसमे एक आदमी ने अपने बच्चे को गोद मे ले रखा था और बीवी उसका हाथ पकड़कर उसके साथ मे खड़ी थी। इसे उसने नोर्मल कहा था, दूसरी भी इन्ही की तस्वीर दिखाई उसमे वो औरत कुर्सी पर बैठी थी और वो उसके पीछे खड़ा था उसके काँधों पर हाथ रखे। ये उसने स्टाइलिस्ट कहा था।
एक तस्वीर में तीन लड़के थे, एक बैठा हुआ था और दो उसके पीछे खड़े थे। एक के हाथ में हंटर था तो दूसरा उसकी तरफ में देख रहा था। तीसरी तस्वीर किसी स्कूल की थी। जिसमे चालिस बच्चो के बीच में एक टीचर बैठी है और सारे बच्चे सामने देख रहे हैं। एकदम सीधे। उन्ही में से एक लड़का अपने बालों में हाथ मार रहा था। वो उस तस्वीर में सबसे अलग ही नज़र आ रहा था।
ऐसी ही ना जाने कितनी ही तस्वीरें थी उसके पास में। जिसको वो अब बटवारे में टटोल रहा था। लेकिन ये बटवारा किसी काम का नहीं था। बस, अपने आँकड़े ठीक करने के जैसा ही था। लेकिन था मज़ेदार। मैं उसे उसी सोच मे छोड़कर चला आया पर वो बिलकुल सटीक था अपनी सोच पर। जैसे चेहरों के खेल मे वो बहुत आगे निकल गया हो। शायद यही उसका काम था। जिसमे वो अपने को भी देखता था। क्योंकि इस खेल का सबसे मंझा हुआ खिलाड़ी तो वही था।
मैं वहाँ से निकलते हुए बस, यही सोच रहा था की अब उस सरकारी अफ़्सर को मेरी तस्वीर नोर्मल लगे। फिर कहता कि लगेगी क्यों नहीं आखिर ये खींची किसने है?
लख्मी
उनकी ये बात सुनकर मैं वापस अपने घर चला आया। मैंने कोई बेकार तस्वीर थोड़ी खिंचवाई थी। मेरा एक दोस्त गोविंदा का बहुत बड़ा फैन है तो वो जब भी तस्वीर खिंचवाता था तो अपने चेहरे को हमेशा गोविंदा अंदाज़ में बना लेता था फिर चाहें वो पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर हो या पोस्टकार्ड साइज़ की। मैंने भी तो कुछ ऐसा ही तो किया था। इसमे हर्ज़ ही क्या था?
मगर उस ऑफिसर ने कहा था की नोर्मल तस्वीर होनी चाहिये। ये रटता हुआ मैं फोटोग्राफर के पास में गया। उससे मैंने कहा, "भाई साहब एक पासपोर्ट साइज़ में तस्वीर खिंचवानी है लेकिन फोटो नोर्मल होनी चाहिये।"
वे ये सुनकर हँसने लगा और कहने लगा, "सर चिंता मत किजिये आप, फोटो एकदम नोर्मल होगी।"
उसने मुझे अपने अन्दर वाले कमरे में बैठा दिया। सामने का पर्दा लगाया और लाइट को बन्द कर दिया। ये एक छोटा सा कमरा था। यहाँ का नया फोटोस्टुडियो था ये। पीछे सफेद रंग का पर्दा खींचा और सामने लगी टेबल पर उसने मुझे बैठा दिया। उसके बाद वो मेरे चेहरे की तरफ़ में आया और देखने लगा। मैंने उससे कहा, "भाईसाहब ये नोर्मल होना क्या होता है? ये चेहरा नोर्मल है ये कैसे पता चलता है? हम हर तस्वीर में अपनी अदा दिखा सकते हैं अलग-अलग भाव भी ला सकते हैं तो ये पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर में क्यों नहीं?"
उसको पता चल गया था कि आज उसको क्या कहा जा रहा हैं। वो कुछ ना बोलते हुए बस, मेरी तरफ़ देखकर हँसने लगा। फिर बोला, "ये बताया नहीं जा सकता सर, पर हाँ मैं जो तस्वीर खींचूगा वो नोर्मल होगी, एकदम आम आदमी की।"
वो ये कहते हुए मेरी तरफ में आया और मेरी कमीज़ ठीक करते हुए बोला, "सर आप बस, मेरी तरफ देखिये। चेहरे को एकदम ढीला छोड़ दिजिये। आँखें एकदम सामने। जब तक मैं ना कहूँ पलक मत झपकना। अपनी बॉडी को थोड़ा हल्का किजिये, हाँ एकदम सही। सीना टाइट कर लिजिये। हाथों को अपने घुटनों पर रख लिजिये। चेहरा थोड़ा नीचे की तरफ, गर्दन का कंठ नहीं नज़र आना चाहिये। आँखें बड़ी मत किजिये, एकदम रिलेक्स होकर बैठिये। एक मिनट में बस, आपका फोटो खिंच जायेगा।"
वो मेरी कमीज को दोबारा से ठीक करते हुए वापस अपनी जगह पर गया। उसकी दूरी लगभग चार फीट की थी। एक बड़ा सा कैमरा मेरे ऊपर ताना हुआ था और बगल में जलती लाइट मेरे मुँह पर पड़ रही थी। मेरा चेहरा लगभग चमक रहा था। ऐसा लग रहा था की जैसे जीरो वॉट का बल्ब मेरे चेहरे पर ही जल रहा हो। इसके बाद मे दो बार कैमरे का फ्लैस मेरे चेहरे पर पड़ा और तस्वीर खिंच गई।
वो मेरी तरफ मे देखते हुए बोला, "लिजिये सर खिंच गई आपकी नोर्मल तस्वीर।"
इस बार मैं हँसा और उससे कहा, "भाई साहब एक बात बताइये ये कौन सा वाला नोर्मल है? डॉक्टर जो कहता है वो वाला नोर्मल? या उस सरकारी आदमी ने जो माँगा वो वाला? फ़िल्मों में जो नज़र आता है वो वाला या आपने जो खींचा वो वाला?"
फोटोग्राफ़र बोला, "सर, ये सारा है। ये वो भी है जो डॉक्टर कहता है और वो वाला भी है जो उस सरकारी आदमी ने माँगा था और ये वो वाला भी है जो मैंने खींचा है। बेसिक्ली ये नोर्मल इंसान वो है जिसकी डिंमाड सबसे ज़्यादा है। मगर ये ही नहीं मिलता।"
"तो क्या मिलता है भाई साहब यहाँ?" मैंने कहा।
फोटोग्राफ़र बोला, "यहाँ पर सब कुछ मिलावट का समान मिलता है। ये मिलावट आपको पता है क्या है। यही तो मस्ती है। यहाँ पर हर कामों मे अलग-अलग चीज चाहिये। तो लोग उसी हिसाब से बँट जाते हैं। जैंसे जो शादी के लिए चाहिये वे अलग है, सरकारी कामों मे अलग, पोज़िंग के लिए अलग, पोर्टपोलियों के अलग और अब तो हैंटीकेप के सार्टीविकेट के लिए भी अलग तो लोग भी उसी के हिसाब से अपने आपको बदल लेते हैं।"
"एक बात बताइये भाईसाहब, आपने ये अलग-अलग महकमों और कामों मे चेहरे बनाने की डिंमाड को कैसे जाना?" मैंने कहा।
फोटोग्राफ़र बोला, "सबसे पहली बात तो ये की मैं भी तो इसी दुनिया में रहता हूँ। इसलिए जो भी यहाँ होता है तो मेरे साथ भी होता है। दूसरा ये की, हमें चेहरों के भाव से, एक्ट से खेलना आना चाहिये तभी तो ये काम है, नहीं तो हमें आता क्या है और सही बात बताऊँ, वो ये की यहाँ पर ये खेल सबको आता है।"
मैंने कहा, "तो ये खेल हर साइज़ के फोटो के साथ खेला जाता है? किस साइज के साथ में कौन सा खेल है ये कैसे बन गया?"
फोटोग्राफ़र बोला, "मेरे हिसाब से तो खाली दो ही तरह के भाव हैं इस दुनिया में। जिसमे से एक हमने बनाया है दूसरा जो हमने नहीं बनाया। बस, उसे मान लिया है। पहला तो ये ही जो आपने खिंचवाया। पासपोर्ट साइज़ का खेल। नोर्मल फोटो, और दूसरा जो खुलकर आता है वो है कि किसी भी साइज़ में आप किसी भी तरह का भाव अपने चेहरे में ला सकते हो।"
"तो ये नोर्मल होना और बाकी का होना क्या है? क्या वो नोर्मल नहीं है?" मैंने कहा।
फोटोग्राफ़र ने कहा, "ये नोर्मल होना कुछ नहीं होता। ये सब बस, माँग है। सरकार को लगता की हम एक ऐसा चेहरा बनाके उसको दे जिसमे कुछ भी अलग से मिलाया ना गया हो। सरकार समझती है की आदमी मे रोना, हँसना, तेडूपंती या स्टाइल सब अलग से आई हैं। ये ऊपर वाले ने नहीं दी। तो सरकार वो चेहरा माँगती है।"
ये माँग के साथ में चेहरे का होना ये तो बहुत कस देता होगा। ये कसा हुआ भी ना लगे और खूबसूरत भी लगे ये कैसे करते फिर?" मैंने कहा।
फोटोग्राफ़र ने कहा, "सर, यही तो हमारा काम है। एक बात कहे आपसे, जब कोई अपनी फोटो खिंचवाता है तो वो हमेशा ये सोचता है कि जब वे अपनी खींची हुई तस्वीर को देखे तो उसे लगता चाहिये की उसका चेहरा ऐसा दिखता है। जो उसे शीसे में नहीं दिखता वो तस्वीर में दिखना चाहिये बस, कोई-कोई अपनी पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर को ही बड़ा करवा लेता है। कभी-कभी तो फ्रैम भी।"
"आपको क्या है लगता है अभी तक जितनी भी तस्वीरें आपने खींची हैं उन तस्वीरों मे से कितनी नोर्मल है और कितनी नहीं?" मैंने कहा।
फोटोग्राफ़र ने कहा, "आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे ये देखिये।"
उसने मेरे सामने काफी सारी तस्वीरें बिछा दी। जिसमे बहुत सारे लोगों की तस्वीरें थी। पहली फैमली फोटो थी। जिसमे एक आदमी ने अपने बच्चे को गोद मे ले रखा था और बीवी उसका हाथ पकड़कर उसके साथ मे खड़ी थी। इसे उसने नोर्मल कहा था, दूसरी भी इन्ही की तस्वीर दिखाई उसमे वो औरत कुर्सी पर बैठी थी और वो उसके पीछे खड़ा था उसके काँधों पर हाथ रखे। ये उसने स्टाइलिस्ट कहा था।
एक तस्वीर में तीन लड़के थे, एक बैठा हुआ था और दो उसके पीछे खड़े थे। एक के हाथ में हंटर था तो दूसरा उसकी तरफ में देख रहा था। तीसरी तस्वीर किसी स्कूल की थी। जिसमे चालिस बच्चो के बीच में एक टीचर बैठी है और सारे बच्चे सामने देख रहे हैं। एकदम सीधे। उन्ही में से एक लड़का अपने बालों में हाथ मार रहा था। वो उस तस्वीर में सबसे अलग ही नज़र आ रहा था।
ऐसी ही ना जाने कितनी ही तस्वीरें थी उसके पास में। जिसको वो अब बटवारे में टटोल रहा था। लेकिन ये बटवारा किसी काम का नहीं था। बस, अपने आँकड़े ठीक करने के जैसा ही था। लेकिन था मज़ेदार। मैं उसे उसी सोच मे छोड़कर चला आया पर वो बिलकुल सटीक था अपनी सोच पर। जैसे चेहरों के खेल मे वो बहुत आगे निकल गया हो। शायद यही उसका काम था। जिसमे वो अपने को भी देखता था। क्योंकि इस खेल का सबसे मंझा हुआ खिलाड़ी तो वही था।
मैं वहाँ से निकलते हुए बस, यही सोच रहा था की अब उस सरकारी अफ़्सर को मेरी तस्वीर नोर्मल लगे। फिर कहता कि लगेगी क्यों नहीं आखिर ये खींची किसने है?
लख्मी
अपने से बहस
हमारा "आसपास" क्या है?, क्या "आसपास" है और क्या दूर, इस समझ के पात्र क्या हैं? कुछ "आसपास" होना और दूर होने का मतलब क्या है? इसके बीच मे जुड़ाव क्या है? "आसपास" और दूर होने का फैसला हम कैसे करते हैं?
इन सवाल को लेकर मैं जहाँ पर रहता हूँ और वहाँ के बारे मे सोचता हूँ तो कई तरह की पैकिंग नज़र आती हैं। जैसे, समाज़ मे "आसपास" को बहुत तरह की पैकिंग मे रखा गया है। जिसमे हमारे रहने को, हमारे चलने को, हमारे काम करने को, हमारे काम करने के बाद मे आने वाले कल की कल्पना करने को, हमें कहाँ जाना है?, कहाँ तक पँहूचना है?... इन सूरतों में हमारे दिमाग के साथ मे हमारे शरीर की पैकिंग पहले से ही तय हो जाती है।
इसका एक उदाहरण देने की कोशिश करता हूँ, जैसे, घर का एक ढाँचा, क्या कभी उसे ध्यान से देखा है? साढ़े बाइस गज़ के मकान को रहने लायक बनाया जाता है। परिवार के सदस्य के मुताबिक उसकी कल्पना को बनावट का रूप दिया जाता है। दो लोगों का परिवार, दो बच्चो की कल्पना और मकान तैयार, उसके साथ मे बस, मिलने के लिए आने वाले लोगों कि भी कल्पना आकार पा लेती है। मगर इसको हम अगर कुछ देर के लिए भूला दे तो?, बच्चा बड़ा हुआ उसकी शादी हुई तो एक कमरा ऊपर चड़ा दिया, दूसरे की हुई तो एक और चड़ा दिया। ये भी वहाँ तक होता है जहाँ तक पैकिंग की संभावनाये होती है। वे भी जायज़ संभावनाये। अगर ये नहीं हो पाता तो उस घर के ढाँचे मे एक और जगह जुड़ जाती है। और पैकिंग के लिए वे भी तैयारी के लिए मौज़ूद है।
ये सोच हमारे संदर्भ मे क्या करती है? हमारे बीच मे ये उपजाऊ है या नहीं?
अभी तक हमारे लिए "आसपास" कई तरह की विशेषताओ से भरा है। मैं कहता हूँ हमारे बीच मे "आसपास" को खुलते, सींचते, उठाते, कहानी कहते, भूल जाते और याद करते हुए देखा है। उसके साथ-साथ उसमे खुद के रॉल को भी बखूबी महसूस किया है। इस दायरे मे ज़्यादातर "आसपास" हमारे अपने रहन-सहन, माहौल से सीधा बातचीत मे रहा है। जो कभी कुछ बोलता है तो कभी गूंगा है। हम जहाँ पर खड़े हुए बस, आसपास वहीं से बयाँ होता है। जो कभी-कभी किसी सूरत मे महज़ एक शब्द की ही भांति दोहराया गया है।
मैं कोशिश कर रहा था "आसपास" को "दूरी" से लिखने व सोचने की। यानि के हमसे दूर क्या है? वे क्या है जिसे हम दूर कहतें हैं? किससे दूरी मे रहते हैं? दूरी को बताने के लिए हमारे पास क्या सवाल हैं और क्या तस्वीरें हैं?
एक आदमी से मैंने पूछा तो वे बोला, "कुछ चीज़ें दूर होती हैं। जहाँ तक हम पँहूच नहीं सकते, कुछ चीज़ों तक पँहूचने की हमारी औकात नहीं होती। बाकि सब तो हमारे आसपास ही है।"
इस ज़ुबान से हम क्या सोच सकते हैं? समाज़ नज़दीकी बोलने के लिए उसका विलोम शब्द अपने हाथ मे रखता है। ये क्रिया क्या है?
"आसपास" से "दूरी" तक को सोचना व सींच पाना।
मुझे लगा ये सोचते हुए की हमें हमारे रियाज़ मे कुछ परिवर्तन लाने होगें। हमारी नज़र, हमारी ज़ुबान और चीज़ें पकड़ने का काँटा सभी को एक ही तरह की आदत पड़ जाती है। जब हम एक ही लय मे लम्बा चलते हैं। हमारे दायरे भले ही फैलाव मे हो लेकिन वे रास्ते हमारे अन्दाजेभर ही होते हैं। अपने आपको किरॉस चैक करना शायद अपनी जगह नहीं बना पाता हमारे अन्दर।
"विलोम शब्द" या "विलोम रूप" की तरह से देखना उसी कार्य को समपन्न करता है।
विलोम शब्द को हम क्या मानते हैं? जब बचपन मे ये सिखाया जाता था तो दिमाग खाली उस शब्द तक ही सीमित रहता था जिसे विलोम रूप मे देखा जा रहा है। उससे क्या आकार दिमाग मे खुल रहा है वे समझने की दुनिया शायद स्कूल के महकमे नहीं समा पाई।
हमारे जीने के तरीके को समाज अपनी नियमों अनुसार से एक रूप मे कस देता है। जिससे वे हर कदम को तय करता है। कहाँ से निकलेगा और आगे क्या मिलेगा ये तक हमारे कदमो के साथ मे तय होता है।
सही मायने मे तो हमारे शरीर के साथ मे हमारे दिमाग का रिश्ता बेहद टाइट बन जाता है या बना दिया जाता है। बाकि रह गया नज़रिया उसे हम खुद से बनाने की कशिश मे लगे रहते हैं। इसको हम किस रूपक मे देखें? या समाज मे इस बदलते नज़रिये की जरूरत क्या है?
हमारी उस जगह से शुरूआत करते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, जिनसे हमारे रिश्ता है ओर जिनसे हम टकराते हैं।
यहाँ से इस बुनियादी दुनिया को समझने की कोशिश की जा सकती है क्या?
लख्मी
इन सवाल को लेकर मैं जहाँ पर रहता हूँ और वहाँ के बारे मे सोचता हूँ तो कई तरह की पैकिंग नज़र आती हैं। जैसे, समाज़ मे "आसपास" को बहुत तरह की पैकिंग मे रखा गया है। जिसमे हमारे रहने को, हमारे चलने को, हमारे काम करने को, हमारे काम करने के बाद मे आने वाले कल की कल्पना करने को, हमें कहाँ जाना है?, कहाँ तक पँहूचना है?... इन सूरतों में हमारे दिमाग के साथ मे हमारे शरीर की पैकिंग पहले से ही तय हो जाती है।
इसका एक उदाहरण देने की कोशिश करता हूँ, जैसे, घर का एक ढाँचा, क्या कभी उसे ध्यान से देखा है? साढ़े बाइस गज़ के मकान को रहने लायक बनाया जाता है। परिवार के सदस्य के मुताबिक उसकी कल्पना को बनावट का रूप दिया जाता है। दो लोगों का परिवार, दो बच्चो की कल्पना और मकान तैयार, उसके साथ मे बस, मिलने के लिए आने वाले लोगों कि भी कल्पना आकार पा लेती है। मगर इसको हम अगर कुछ देर के लिए भूला दे तो?, बच्चा बड़ा हुआ उसकी शादी हुई तो एक कमरा ऊपर चड़ा दिया, दूसरे की हुई तो एक और चड़ा दिया। ये भी वहाँ तक होता है जहाँ तक पैकिंग की संभावनाये होती है। वे भी जायज़ संभावनाये। अगर ये नहीं हो पाता तो उस घर के ढाँचे मे एक और जगह जुड़ जाती है। और पैकिंग के लिए वे भी तैयारी के लिए मौज़ूद है।
ये सोच हमारे संदर्भ मे क्या करती है? हमारे बीच मे ये उपजाऊ है या नहीं?
अभी तक हमारे लिए "आसपास" कई तरह की विशेषताओ से भरा है। मैं कहता हूँ हमारे बीच मे "आसपास" को खुलते, सींचते, उठाते, कहानी कहते, भूल जाते और याद करते हुए देखा है। उसके साथ-साथ उसमे खुद के रॉल को भी बखूबी महसूस किया है। इस दायरे मे ज़्यादातर "आसपास" हमारे अपने रहन-सहन, माहौल से सीधा बातचीत मे रहा है। जो कभी कुछ बोलता है तो कभी गूंगा है। हम जहाँ पर खड़े हुए बस, आसपास वहीं से बयाँ होता है। जो कभी-कभी किसी सूरत मे महज़ एक शब्द की ही भांति दोहराया गया है।
मैं कोशिश कर रहा था "आसपास" को "दूरी" से लिखने व सोचने की। यानि के हमसे दूर क्या है? वे क्या है जिसे हम दूर कहतें हैं? किससे दूरी मे रहते हैं? दूरी को बताने के लिए हमारे पास क्या सवाल हैं और क्या तस्वीरें हैं?
एक आदमी से मैंने पूछा तो वे बोला, "कुछ चीज़ें दूर होती हैं। जहाँ तक हम पँहूच नहीं सकते, कुछ चीज़ों तक पँहूचने की हमारी औकात नहीं होती। बाकि सब तो हमारे आसपास ही है।"
इस ज़ुबान से हम क्या सोच सकते हैं? समाज़ नज़दीकी बोलने के लिए उसका विलोम शब्द अपने हाथ मे रखता है। ये क्रिया क्या है?
"आसपास" से "दूरी" तक को सोचना व सींच पाना।
मुझे लगा ये सोचते हुए की हमें हमारे रियाज़ मे कुछ परिवर्तन लाने होगें। हमारी नज़र, हमारी ज़ुबान और चीज़ें पकड़ने का काँटा सभी को एक ही तरह की आदत पड़ जाती है। जब हम एक ही लय मे लम्बा चलते हैं। हमारे दायरे भले ही फैलाव मे हो लेकिन वे रास्ते हमारे अन्दाजेभर ही होते हैं। अपने आपको किरॉस चैक करना शायद अपनी जगह नहीं बना पाता हमारे अन्दर।
"विलोम शब्द" या "विलोम रूप" की तरह से देखना उसी कार्य को समपन्न करता है।
विलोम शब्द को हम क्या मानते हैं? जब बचपन मे ये सिखाया जाता था तो दिमाग खाली उस शब्द तक ही सीमित रहता था जिसे विलोम रूप मे देखा जा रहा है। उससे क्या आकार दिमाग मे खुल रहा है वे समझने की दुनिया शायद स्कूल के महकमे नहीं समा पाई।
हमारे जीने के तरीके को समाज अपनी नियमों अनुसार से एक रूप मे कस देता है। जिससे वे हर कदम को तय करता है। कहाँ से निकलेगा और आगे क्या मिलेगा ये तक हमारे कदमो के साथ मे तय होता है।
सही मायने मे तो हमारे शरीर के साथ मे हमारे दिमाग का रिश्ता बेहद टाइट बन जाता है या बना दिया जाता है। बाकि रह गया नज़रिया उसे हम खुद से बनाने की कशिश मे लगे रहते हैं। इसको हम किस रूपक मे देखें? या समाज मे इस बदलते नज़रिये की जरूरत क्या है?
हमारी उस जगह से शुरूआत करते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, जिनसे हमारे रिश्ता है ओर जिनसे हम टकराते हैं।
यहाँ से इस बुनियादी दुनिया को समझने की कोशिश की जा सकती है क्या?
लख्मी
Friday, January 9, 2009
एक अकेला शहर में
दिनॉक: 12-12-2008, समय: 11:40 बजे
इसमे उभरते जीवन की कल्पना मे बहते कुछ पल, समझने की कोशिश करे तो, अंजानपन को जीना क्या है? जो ज़िन्दगी में कोहरे की तरह आकर बस जाता है और हम उसे अपने आसपास का एक अनुमान समझकर जीने की कोशिश करते हैं। वो शायद आँखों की पकड़ में नहीं आ पाता। उसे छूने का अहसास बनाया जा सकता है जिसे अपनी याद्दाश्त का हिस्सा बना लिया जाये, वो एक क्षण ही है। जो आज को अपना सम्मान समझ लेता है।
राकेश
Thursday, January 8, 2009
एक ज़िन्दगी की बदलती कहानी
हम तस्वीरों में अपने आप को कहाँ देखते हैं?
बहते हुए पानी में हम कभी भी अपनी परछाई को समझने की कोशिश कर सकते हैं।

हम तस्वीरों में अपने आप को कहाँ देखते हैं?
बहते हुए पानी में हम कभी भी अपनी परछाई को समझने की कोशिश कर सकते हैं।

हम तस्वीरों में अपने आप को कहाँ देखते हैं?
बहते हुए पानी में हम कभी भी अपनी परछाई को समझने की कोशिश कर सकते हैं।

हम तस्वीरों में अपने आप को कहाँ देखते हैं?
बहते हुए पानी में हम कभी भी अपनी परछाई को समझने की कोशिश कर सकते हैं।
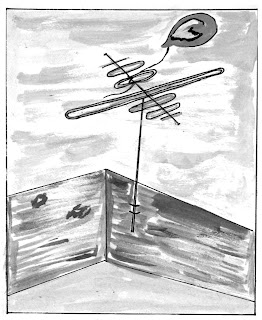
हम तस्वीरों में अपने आप को कहाँ देखते हैं?
बहते हुए पानी में हम कभी भी अपनी परछाई को समझने की कोशिश कर सकते हैं।

हम तस्वीरों में अपने आप को कहाँ देखते हैं?
बहते हुए पानी में हम कभी भी अपनी परछाई को समझने की कोशिश कर सकते हैं।
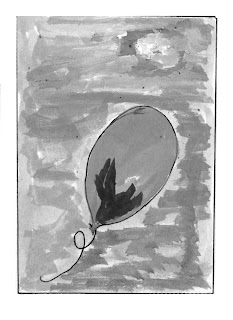
हम तस्वीरों में अपने आप को कहाँ देखते हैं?
बहते हुए पानी में हम कभी भी अपनी परछाई को समझने की कोशिश कर सकते हैं।

हम तस्वीरों में अपने आप को कहाँ देखते हैं?
बहते हुए पानी में हम कभी भी अपनी परछाई को समझने की कोशिश कर सकते हैं।

हम तस्वीरों में अपने आप को कहाँ देखते हैं?
बहते हुए पानी में हम कभी भी अपनी परछाई को समझने की कोशिश कर सकते हैं।

राकेश
बहते हुए पानी में हम कभी भी अपनी परछाई को समझने की कोशिश कर सकते हैं।

हम तस्वीरों में अपने आप को कहाँ देखते हैं?
बहते हुए पानी में हम कभी भी अपनी परछाई को समझने की कोशिश कर सकते हैं।

हम तस्वीरों में अपने आप को कहाँ देखते हैं?
बहते हुए पानी में हम कभी भी अपनी परछाई को समझने की कोशिश कर सकते हैं।

हम तस्वीरों में अपने आप को कहाँ देखते हैं?
बहते हुए पानी में हम कभी भी अपनी परछाई को समझने की कोशिश कर सकते हैं।
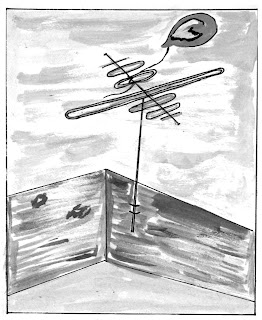
हम तस्वीरों में अपने आप को कहाँ देखते हैं?
बहते हुए पानी में हम कभी भी अपनी परछाई को समझने की कोशिश कर सकते हैं।

हम तस्वीरों में अपने आप को कहाँ देखते हैं?
बहते हुए पानी में हम कभी भी अपनी परछाई को समझने की कोशिश कर सकते हैं।
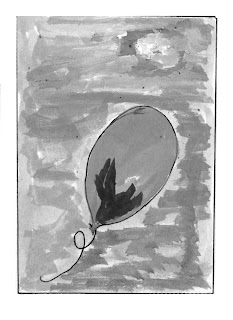
हम तस्वीरों में अपने आप को कहाँ देखते हैं?
बहते हुए पानी में हम कभी भी अपनी परछाई को समझने की कोशिश कर सकते हैं।

हम तस्वीरों में अपने आप को कहाँ देखते हैं?
बहते हुए पानी में हम कभी भी अपनी परछाई को समझने की कोशिश कर सकते हैं।

हम तस्वीरों में अपने आप को कहाँ देखते हैं?
बहते हुए पानी में हम कभी भी अपनी परछाई को समझने की कोशिश कर सकते हैं।

राकेश
Wednesday, January 7, 2009
उसकी चुप्पी से डर था
हमारे जीवन के सवाल क्या हैं? या वे सवाल क्या हैं जो हमें जीने लायक बनाते हैं? या वे जिससे हम जीना सीखते हैं? या वे जिनको लेकर हमें रोज चलना और बदलना होता है?
क्या कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं जो हमें टकराने को कहते हैं? किससे टकराने को और कैसे टकराने को जोर देते हैं। क्या कुछ सवाल ऐसे हैं जिन्हे हम खुद बनाते हैं अपने लिए या वे हमारे लिए कोई बनाकर देता है। हमारे खुद के सवालों मे हमारी इच्छाएँ क्या रूप लेती हैं अथवा उन सवालों में क्या जो हमारे लिए किसी ने बनाकर छोड़े हैं।
क्या हमें ये पता है कि हर दिन के अनुसार हमारे सवाल बदल जाते हैं या फिर छूटे हुए सवाल ही नये आकार और रूप ने बदलकर ताज़ा हो जाते हैं। इनका रिश्ता खाली निर्धारित समय से होता है या फिर ये हमारे जीवन जीने के तरीको में या बदलाव के रूपों मे भी अपना जोर दिखाते हैं?
सवालों को सोचते हुए लगता है कि हमें किसी ने घेरा हुआ है, हम आजाद नहीं है। हम जो भी अपने लिए बनाते अथवा चुनते हैं वे किसी न किसी तरह से एक ऐसी पकड़ मे दबती जाती है कि उसका बेजोड़ तलाशना भी मुश्किल लगता है लेकिन कभी-कभी ये हमें नई राहें खोजने की चेष्टा देती है। कहीं और निकल जाने की उम्मीद भरती है। जिसमे "कहीं और" बहुत फैला हुआ लगता है। आपार कल्पनाए लिए हमारे बगल में चलता है। कभी भरे व लदे चित्रों के साथ तो कभी खाली शुमसान माहौल की तरह।
एक चित्र को सामने लाये तो, जैसे- कोई भरी या लदी गाड़ी पटरी से उतर जाये तो क्या होता है?
ये समय हमारे जीवन मे पलभर के लिए सब कुछ थामकर कोई एक ऐसा हिस्सा खुला छोड़ देता है जिससे कहीं खिचने की भरपूर चाहत होती है। लेकिन वो क्या है?
एक और चित्र को बयाँ करते हैं, जैसे- अचानक से जीवन जीने का तरीका, उसका आधार, रूप-सज्जा और बोल बदल जाये तो क्या होता है?
ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कोई गाड़ी पटरी से उतर गई है। यहाँ जीवन गाड़ी नहीं बल्कि वे तेजी है जो धीमी रफ़्तार मे तब आती है जब कोई उसकी कम रफ़्तार की उम्मीद लगाता है या फिर उसके मुकाबले अपनी रफ़्तार नहीं बना पाता।
मेरे दिमाग मे पहले ये सब किसी अवधारणा के तहत ही था। हाँ भले ही अपने अनुमान से शहर, जीवन और तेजी को समझने मे मैंने कई कोशिशें की हैं। पर वे क्या रही हैं मेरे लिए? खाली वे अंदाजेभर ही तो थे जो किसी को समझाने भर के रूपक थी। शायद मैं खुद घूम रहा हूँ।
पिछले दिनों मेरी काफी पुरानी साथी से मुलाकात हुई, उसको देखकर और उसकी बातों को सुनकर पहली बार लगा कि जैसे उसकी आवाज़ किसी भरे व लदे भाव से भारी हो गई है। ये एक अहसास था उसके लिए जो उसके अन्दर था। जिसने उसके अपने कुछ सवाल बदल दिये थे। जिसके साथ उसका मेल-जोल भी शुरू हो गया था। पहले जैसी किसी बात पर ना जाऊँ तो वे कुछ पूछ रही थी। जो उसके लिए था जिसमे अगर मैं अपनी राय या शब्द जैसे कुछ रखता तो वो मेरे लिए उसके जीने के अनुसार बेहद दूर था। वे मेरा ही नहीं था। मेरे शरीर के साथ समाज का रिश्ता कई अन्य असवधारणाओं से रचा गया था। जिसमे मुझे ताकतवर बनाया दिया था। इन सब बातों का उसके अहसास और आवाज़ से कोई नाता नहीं था और ना ही कोई रिश्ता बनाया जा सकता था।
वे कह रही थी, "मैंने पिछले दिनों अपने घर मे एक बदलाव देखा है। एक ऐसा बदलाव जिसे महसूस करके ऐसा लगा जैसे वे अभी हाल-फिलाल मे नहीं आया है। वे पहले से ही जमा हुआ था या कह सकती हूँ कि वे कहीं छुपा था मेरे ही घर के अन्दर। हाँ जिसके नीचे वे छुपा था वे मेरे घर, परिवार के वे रिश्ते थे जिनके मान-सम्मान को बरकरार रखा जाता है और ये भी की उस बदलाव को बाहर आने की कोई जगह नहीं दी गई थी मेरे घर मे। कई ऐसे बड़े रिश्ते हैं हमारे घर मे कि उनकी आड़ मे कई ऐसे बदलाव सांस लेते हैं। जो अभी बाहर आने बाकी हैं।
ये सारा बदलाव खाली मेरे लिए ही था। जिसमे मुझे भी बदलने पर मजबूर किया। जो चाहते न चाहते मुझपर हावी हुआ। जिसको अभी तुम देख सकते हो। मेरे हर रोज को जीने के सवाल ही बदल दिए गए और उसके साथ-साथ मेरे लिए वे गहरे भी हो गए। मैं समझ नहीं पाती की ये घर के माहौल में अचानक कैसे उतर आते हैं। बस, एक बात कहती हूँ जिसने ये सारी बातें मुझमे तैयार की हैं।
मैं हर रोज सवेरे जल्दी उठती हूँ। दस लोगों के लिए खाना बनाती हूँ, चाय-नाश्ता सब कुछ तैयार करती हूँ। लेकिन जब कोई घर मे आता है तो मेरे बारे कहा जाता है कि इसका कोई नहीं है, ये अकेली रह गई है। तब मैं समझ नहीं पाती कि वे दस लोग कौन हैं जिसके लिए मैं रोज सुबह उठ रही हूँ या खाना बना रही हूँ। ये कौन है? या मैं कौन हूँ?
वे रिश्ता जिसके तले वे सब कुछ छुपा था वे नहीं रहा या वे अपनी कोई परछाई भी नहीं छोड़कर गया? जो भी कोई आता है मुझे इस तरह से भाव भरी नज़रों से देखता है कि एक पल भी मैं उनकी आँखों मे नहीं देख पाती झटक जाती हूँ। यही सोचकर की कहीं मेरी आँखों मे पानी ना उतर आये। और जब वे उस झलक को मेरी आँखों में नहीं देख पाते तो उनकी नर्मी मेरे लिए और भी मजबूत हो जाती है। जिसको खुद मे उतर जाने को मैं रोक नहीं पाती। वे हमेशा कहते हैं कि तुझे उनकी याद नहीं आती?
मैं क्यों याद करूँ उन्हे?, जो छुटा है उसी को क्यों दोहराऊँ, जो वे सब अपने साथ ले गए उसे क्यों वापस खींचूँ? और जो उनकी परछाई है उसके साथ मे मैं क्या रिश्ता बनाऊँ?
ये सब कुछ बदलाव की आग मे शामिल है जिसको महसूस करना भी एक पल के बेहद कठोर लगता है। अब तो टाइम का भी पता नहीं रहता। घर के साथ मे टाइम का रिश्ता किसी और ही दिशा मे दौड़ रहा है या समझों दौड़ चुका है। जितनी भी देर बाहर रहूँ कोई सवाल-जवाब नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, मानती हूँ की अच्छा लगता है पर पहले जिन माहौलों की आदत या अहसास मुझमे भर गया है उसमे ये बदलाव डरा देता है।"
वो मुझे इसके बाद मे देखती रही। उसकी उस वक़्त की आँखों मे कुछ चाहने की राह थी। वे आँखे अभी भी नहीं भूली जाती मुझसे। ये सब कुछ दुनियाना उसका कोई समाजिक रिश्तो के बदलाव को ही जाहिर करना नहीं था। जिसको "ऐसा ही होता है" कहकर टाला जा सकता हो। या फिर दुनिया का आइना दिखाकर सहमति जताई जा सकती हो या फिर उसको ताकत देकर छोड़ा जा सकता हो। ना जाने ये विवरण कहाँ ले जाता है? पहली बार लगा जैसे मैं या हम समाजिक रिश्तों मे अभी काफी पीछे खड़े हैं अगर कुछ मानते हैं तो ये सब कुछ भम्र हो सकता है। बस, दूर खड़े ये सोच रहे हैं कि उनसे कैसे जुझा जाये या फिर कैसे समझा जाये। हमारा टकराना या फिर उनमे रहकर कई अन्य तरह के बदलावों को देखना। ये कई तरह की संभावनाओं को सामने लाकर खड़ा कर देता है। बस, फ़र्क सिर्फ़ इतना है की ये संभावनायें हमारे हाथ मे नहीं होती। ये वे संभावनाये नहीं है जिनकी उम्मीद हम अक्सर बाँध कर रखते हैं।
हाँलाकि वे मुस्कुराकर ये सब कहे जा रही थी। मुझे उसके कहने या बोलने से नहीं बस, उसकी चुप्पी से डर था।
लख्मी
क्या कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं जो हमें टकराने को कहते हैं? किससे टकराने को और कैसे टकराने को जोर देते हैं। क्या कुछ सवाल ऐसे हैं जिन्हे हम खुद बनाते हैं अपने लिए या वे हमारे लिए कोई बनाकर देता है। हमारे खुद के सवालों मे हमारी इच्छाएँ क्या रूप लेती हैं अथवा उन सवालों में क्या जो हमारे लिए किसी ने बनाकर छोड़े हैं।
क्या हमें ये पता है कि हर दिन के अनुसार हमारे सवाल बदल जाते हैं या फिर छूटे हुए सवाल ही नये आकार और रूप ने बदलकर ताज़ा हो जाते हैं। इनका रिश्ता खाली निर्धारित समय से होता है या फिर ये हमारे जीवन जीने के तरीको में या बदलाव के रूपों मे भी अपना जोर दिखाते हैं?
सवालों को सोचते हुए लगता है कि हमें किसी ने घेरा हुआ है, हम आजाद नहीं है। हम जो भी अपने लिए बनाते अथवा चुनते हैं वे किसी न किसी तरह से एक ऐसी पकड़ मे दबती जाती है कि उसका बेजोड़ तलाशना भी मुश्किल लगता है लेकिन कभी-कभी ये हमें नई राहें खोजने की चेष्टा देती है। कहीं और निकल जाने की उम्मीद भरती है। जिसमे "कहीं और" बहुत फैला हुआ लगता है। आपार कल्पनाए लिए हमारे बगल में चलता है। कभी भरे व लदे चित्रों के साथ तो कभी खाली शुमसान माहौल की तरह।
एक चित्र को सामने लाये तो, जैसे- कोई भरी या लदी गाड़ी पटरी से उतर जाये तो क्या होता है?
ये समय हमारे जीवन मे पलभर के लिए सब कुछ थामकर कोई एक ऐसा हिस्सा खुला छोड़ देता है जिससे कहीं खिचने की भरपूर चाहत होती है। लेकिन वो क्या है?
एक और चित्र को बयाँ करते हैं, जैसे- अचानक से जीवन जीने का तरीका, उसका आधार, रूप-सज्जा और बोल बदल जाये तो क्या होता है?
ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कोई गाड़ी पटरी से उतर गई है। यहाँ जीवन गाड़ी नहीं बल्कि वे तेजी है जो धीमी रफ़्तार मे तब आती है जब कोई उसकी कम रफ़्तार की उम्मीद लगाता है या फिर उसके मुकाबले अपनी रफ़्तार नहीं बना पाता।
मेरे दिमाग मे पहले ये सब किसी अवधारणा के तहत ही था। हाँ भले ही अपने अनुमान से शहर, जीवन और तेजी को समझने मे मैंने कई कोशिशें की हैं। पर वे क्या रही हैं मेरे लिए? खाली वे अंदाजेभर ही तो थे जो किसी को समझाने भर के रूपक थी। शायद मैं खुद घूम रहा हूँ।
पिछले दिनों मेरी काफी पुरानी साथी से मुलाकात हुई, उसको देखकर और उसकी बातों को सुनकर पहली बार लगा कि जैसे उसकी आवाज़ किसी भरे व लदे भाव से भारी हो गई है। ये एक अहसास था उसके लिए जो उसके अन्दर था। जिसने उसके अपने कुछ सवाल बदल दिये थे। जिसके साथ उसका मेल-जोल भी शुरू हो गया था। पहले जैसी किसी बात पर ना जाऊँ तो वे कुछ पूछ रही थी। जो उसके लिए था जिसमे अगर मैं अपनी राय या शब्द जैसे कुछ रखता तो वो मेरे लिए उसके जीने के अनुसार बेहद दूर था। वे मेरा ही नहीं था। मेरे शरीर के साथ समाज का रिश्ता कई अन्य असवधारणाओं से रचा गया था। जिसमे मुझे ताकतवर बनाया दिया था। इन सब बातों का उसके अहसास और आवाज़ से कोई नाता नहीं था और ना ही कोई रिश्ता बनाया जा सकता था।
वे कह रही थी, "मैंने पिछले दिनों अपने घर मे एक बदलाव देखा है। एक ऐसा बदलाव जिसे महसूस करके ऐसा लगा जैसे वे अभी हाल-फिलाल मे नहीं आया है। वे पहले से ही जमा हुआ था या कह सकती हूँ कि वे कहीं छुपा था मेरे ही घर के अन्दर। हाँ जिसके नीचे वे छुपा था वे मेरे घर, परिवार के वे रिश्ते थे जिनके मान-सम्मान को बरकरार रखा जाता है और ये भी की उस बदलाव को बाहर आने की कोई जगह नहीं दी गई थी मेरे घर मे। कई ऐसे बड़े रिश्ते हैं हमारे घर मे कि उनकी आड़ मे कई ऐसे बदलाव सांस लेते हैं। जो अभी बाहर आने बाकी हैं।
ये सारा बदलाव खाली मेरे लिए ही था। जिसमे मुझे भी बदलने पर मजबूर किया। जो चाहते न चाहते मुझपर हावी हुआ। जिसको अभी तुम देख सकते हो। मेरे हर रोज को जीने के सवाल ही बदल दिए गए और उसके साथ-साथ मेरे लिए वे गहरे भी हो गए। मैं समझ नहीं पाती की ये घर के माहौल में अचानक कैसे उतर आते हैं। बस, एक बात कहती हूँ जिसने ये सारी बातें मुझमे तैयार की हैं।
मैं हर रोज सवेरे जल्दी उठती हूँ। दस लोगों के लिए खाना बनाती हूँ, चाय-नाश्ता सब कुछ तैयार करती हूँ। लेकिन जब कोई घर मे आता है तो मेरे बारे कहा जाता है कि इसका कोई नहीं है, ये अकेली रह गई है। तब मैं समझ नहीं पाती कि वे दस लोग कौन हैं जिसके लिए मैं रोज सुबह उठ रही हूँ या खाना बना रही हूँ। ये कौन है? या मैं कौन हूँ?
वे रिश्ता जिसके तले वे सब कुछ छुपा था वे नहीं रहा या वे अपनी कोई परछाई भी नहीं छोड़कर गया? जो भी कोई आता है मुझे इस तरह से भाव भरी नज़रों से देखता है कि एक पल भी मैं उनकी आँखों मे नहीं देख पाती झटक जाती हूँ। यही सोचकर की कहीं मेरी आँखों मे पानी ना उतर आये। और जब वे उस झलक को मेरी आँखों में नहीं देख पाते तो उनकी नर्मी मेरे लिए और भी मजबूत हो जाती है। जिसको खुद मे उतर जाने को मैं रोक नहीं पाती। वे हमेशा कहते हैं कि तुझे उनकी याद नहीं आती?
मैं क्यों याद करूँ उन्हे?, जो छुटा है उसी को क्यों दोहराऊँ, जो वे सब अपने साथ ले गए उसे क्यों वापस खींचूँ? और जो उनकी परछाई है उसके साथ मे मैं क्या रिश्ता बनाऊँ?
ये सब कुछ बदलाव की आग मे शामिल है जिसको महसूस करना भी एक पल के बेहद कठोर लगता है। अब तो टाइम का भी पता नहीं रहता। घर के साथ मे टाइम का रिश्ता किसी और ही दिशा मे दौड़ रहा है या समझों दौड़ चुका है। जितनी भी देर बाहर रहूँ कोई सवाल-जवाब नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, मानती हूँ की अच्छा लगता है पर पहले जिन माहौलों की आदत या अहसास मुझमे भर गया है उसमे ये बदलाव डरा देता है।"
वो मुझे इसके बाद मे देखती रही। उसकी उस वक़्त की आँखों मे कुछ चाहने की राह थी। वे आँखे अभी भी नहीं भूली जाती मुझसे। ये सब कुछ दुनियाना उसका कोई समाजिक रिश्तो के बदलाव को ही जाहिर करना नहीं था। जिसको "ऐसा ही होता है" कहकर टाला जा सकता हो। या फिर दुनिया का आइना दिखाकर सहमति जताई जा सकती हो या फिर उसको ताकत देकर छोड़ा जा सकता हो। ना जाने ये विवरण कहाँ ले जाता है? पहली बार लगा जैसे मैं या हम समाजिक रिश्तों मे अभी काफी पीछे खड़े हैं अगर कुछ मानते हैं तो ये सब कुछ भम्र हो सकता है। बस, दूर खड़े ये सोच रहे हैं कि उनसे कैसे जुझा जाये या फिर कैसे समझा जाये। हमारा टकराना या फिर उनमे रहकर कई अन्य तरह के बदलावों को देखना। ये कई तरह की संभावनाओं को सामने लाकर खड़ा कर देता है। बस, फ़र्क सिर्फ़ इतना है की ये संभावनायें हमारे हाथ मे नहीं होती। ये वे संभावनाये नहीं है जिनकी उम्मीद हम अक्सर बाँध कर रखते हैं।
हाँलाकि वे मुस्कुराकर ये सब कहे जा रही थी। मुझे उसके कहने या बोलने से नहीं बस, उसकी चुप्पी से डर था।
लख्मी
डीडीए का गलत रिज़ल्ट
डीडीए फ़्लैट का रिज़ल्ट दोबारा से निकाला जायेगा, ये ख़बर टीवी पर सुनने के बाद कई उंमगों को जैसे दोबारा से सांस मिल गई हो। सबके चेहरों मे जैसे आशा की कई नई लहरें फिर से लहरा गई हो। ऊपर वाले की तरफ नज़र करके खड़े लोग टीवी के सामने हाथ जोड़े ना जाने कितनी दुआएँ और कलमे पढ़ने लगे। "इस बार तो पक्का अपना भी नाम लिस्ट मे होगा।" यही ज़हन मे गुलाटियाँ मार रहा था। हाँलाकि पिछली लिस्ट मे अपना नाम था भी या नहीं इसको याद ना करते हुए इस बार इरादे काफी पुख़्ता कर दिये थे।
ये ख़बर दिन-रात टीवी पर दिखाई जा रही थी और इस दौरान हर जगह न्यूज़ ख़त्म हो जाने के बाद मे बस, अपनी ही बहस शुरू हो जाती। लोग ये सुनने के लिए टीवी के सामने बैठे रहते की वो तारीख कौन सी होगी जब ये रिज़ल्ट दोबारा से निकाला जायेगा। किसी के लिए दुख के आँसू तो किसी के लिए उमगों भरे आँखू बनकर ये न्यूज़ चल रही थी। ये बिलकुल ऐसा ही था जैसे किसी खिलाड़ी को एक और एक्सट्रा बॉल मिल गई हो। अब उम्मीद होगी उस आखिरी बॉल पर छक्का लगाने की।
कई सौ-सौ रूपये के फ़ार्म भरे इन्तजार करते लोग बस, इसी राह मे थे कि कुछ तो होगा ऐसा दिल्ली जैसे बड़े शहर मे जहाँ हमारे नाम की भी कोई जगह होगी। कोई तो दरवाजा ऐसा बनेगा कभी जिसके आगे हमारे नाम की भी तख़्ती लगेगी। कोई तो ऐसा राशन कार्ड होगा जिसमे मेरा नाम सबसे ऊपर और मुखिया का ऑदा लेगा। पर क्या ये संभव है? वो भी दिल्ली जैसे बड़े शहर मे?
ये सपने हर छोटी कॉलोनियों मे रहने वाले के दिमाग मे हमेशा ताज़ा रहते हैं। जो बस, अवसर तलाशते हैं किसी ऐसे मौके का जिसमे ये कूद सकें और अपनी किश्मत आज़मा सकें। यही इन्तजार इनको हमेशा चौंकन्ना रखता है। ये हमेशा इसी ताड़ मे रहते हैं कि कोई तो फार्म निकले, किसी भी अख़बार मे जिसमे हमारे जैब की मुताबिक घर के प्लान हो। इसलिए हर अख़बार पर इनकी नज़र रहती है। चाहें ये कोई भी अख़बार खरीदे या नहीं मगर नज़र शहर मे किसी भी चाय की दुकान पर रखे अख़बारों मे या फिर राह चलते किसी भी अजनबी से रिश्ता बनाकर उसका अख़बार शेयर करने से नज़र आ ही जाती है। ये खाली अख़बार तक ही सीमित नहीं रहती। ये चाहत टीवी के हर न्यूज़ चैनल पर पँहुच ही जाती है।
अभी कुछ समय पहले ये न्यूज़ काफी जोरो से यहाँ दक्षिण पुरी मे फैली के, प्रगति मैदान मे मीडिल क्लास के लिए घर निकाले गए हैं। तो बस, पँहुच गए सभी अपने-अपने नाम से किश्मत को आज़माने, लेकिन दूसरे ही दिन जब घरों की किमतों पर सरकार ने नज़र डाली तो सब उंमगें जैसे धरी-की धरी रह गई।
नेमसिंह जी एक मात्र आदमी हैं जिनकी हर स्कीम पर निगाह रहती है। वे तो कभी भी कोई भी स्कीम नहीं छोड़ते। बस, जहाँ के बारे मे भी पूछना हो, पूछ सकते हैं। मकान लेने की ऐसी हुड़क किसी मे भी शायद देखी नहीं जा सकती। वे वहाँ प्रगति मैदान से आये और कहने लगे, "बताओ भला, घर निकाले हैं मीडिल क्लास के लिए और किमत 13 लाख से 16 लाख। अब जरा ये भी बता दो की किसी मीडिल क्लास का आदमी इस किमत मे फिट बैठता है? अच्छा ये नहीं तो ये ही बता दो की अगर मेरे जैसा आदमी बैंक से लोन भी लेगा तो उसकी मासिक किश्त कितने की होगी? लगभग देखा जाये तो 7000 रुपये से 8000 रुपये तक। अब जो आदमी महिने मे 6000 रुपये कमाता हो वो किश्त देगा तो खायेगा क्या? वाह! री सरकार, तुझे सलाम।"
ये कहते हुए वो अपने घर के अन्दर चले गए पर बात यहीं पर नहीं ख़त्म हुई थी। वे तो अब उनके बोल से निकल कर कई अलग-अलग दिमाग और ज़ुबानो मे चली गई थी। बातों ही बातों मे घरों की बातें फैल गई। लोग मकान-मकान का नारा लगाने लगे। कोई भरने की कहता तो कोई बात को टालने की। इसलिए तो यहाँ पैसा इनवेस्ट करवाने वालो की भी कमी नहीं है। बस, इच्छाएँ पकड़कर और चेहरा पढ़कर ये घुसे चले आते हैं और सब कुछ जैसे निकालकर रख देते हैं। इनके लिए सोलह या सत्तराह लाख को बॉय हाथ का खेल होता है। बैठे-बैठे कागज़ के एक छोटे से टुकड़े पर ये आपकी ज़िन्दगी का मैप बना डालते हैं और मैप मे बस, पैसा ही पैसा होता है। ये पैसा कहाँ से आयेगा और कैसे आयेगा ये सब पता होता है इन्हे। बस, ये नहीं बताते की ये पैसा मेरे पास रहेगा कब तक?
नेमसिंह जी इन सब के घेरे मे नहीं पड़ते, साफ निकल आते हैं। उन्हे पता है कि उनका पैसा कहाँ से आता है, कैसे आता है और कहाँ चला जायेगा। अपने घर मे कई समानों के साथ-साथ एक कौना ऐसा भी बनाया है जिसमे ना जाने कितने मकानों के फार्म फोटोस्टेट किये हुए रखे हैं और ना जाने कितनी अख़बार की कटींग भी। जिसमे घर के बारे मे कई प्रकार की डीटेल शामिल है। साथ-साथ सरकारी फ़्लैट के बारे मे सारी बातें भी। किसी मे गाज़ियाबाद के फार्म हैं तो किसी मे दिल्ली के। ये हर जगह अपनी किश्मत आज़माने से नहीं चूकते।
"पूरे चार सालों के बाद में निकाले हैं सरकार ये जनता फ़्लैट, और अब देखो वो भी अटक गए। ना जाने क्या होगा हमारा तो?”
दक्षिणपुरी में इन दिनों पहली बार घर लेने और पाने की मारामारी छाई रही। इतनी बातें, इतनी इच्छाएँ और इतना जोश आज से पहले नहीं था। इसके कई कारण हो सकते हैं। पर तमन्ना एक ही होगी। ये क्रैज़ खाली बदलाव के तहत ही नहीं था बल्कि अब दक्षिणपुरी ने अपने आने वाले टाइम को देखना शुरू किया था और ये सब राजीव गांधी विकास के घरों को लेकर तो कुछ ज़्यादा ही था। सबसे पहले तो घर के फार्म खरीदने की मारामारी उसके बाद मे उसको छुपाकर भरने की होंश भी। ये बड़ी मज़ेदार वारदातों से बनती है। कई खेल हैं इनमे। अगर गली में किसी एक को पता चल जाता कि सरकार ने घर निकाले हैं गरीबों के लिए तो वो किसी और को अपने मुँह से नहीं बताता। इनका मानना ये रहता है कि जितना लोगों को पता चलेगा उतने ही उम्मीदवार बड़ जायेगें और हमारे चांस कम हो जायेगें। वैसे देखा जाये तो ये खाली अपने ही मन की बनाई बात रहती। पता यहाँ पर सबको रहता बस, सभी उसको छुपाने के तरीके तलाशते रहते।
यहाँ पर ये खेल हर गली, हर नुक्कड़, हर बसस्टेंड अथवा हर बस मे भी देखा जाता। हर कोई अपनी तरह से उसको नाटने की बात करता और ये समझाने की कोशिश करता की "ये हमारे लिए नहीं है" या ये कहता के "इसमे इतने रूपये भरे जायेगें, हमारे बस का नहीं है" और ज़्यादा से ज़्यादा बताते तो कोई ये कहता कि "ये निकलेगा ही नहीं।" ताकी लोग उस तरफ ना खिंचे।
मगर वो कहते है ना, बहकावे मे ना आओ, बस अपनी अकल लगाओ। यहाँ पर भी लोग कुछ ऐसा ही करते हैं। "हाँ-हूँ" के बाद तो कहानी कुछ अलग ही मोड़ ले लेती और सरकार की झाँसों भरी स्कीम भी पूरी हो जाती। सौ-सौ रुपये लिए दिल्ली की करोंड़ों पगली जनता घर-घर चिल्लाती हुई फार्म की खिड़कियों पर टूट पड़ती। और सरकारी खातों मे वे ही सौ-सौ के नोट जैसे अरबों रुपये की बारिश कर देते। ये सौ के नोट किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन सरकार के लिए बेहद बड़ी बात थी। ये एक भूख की तरह से होती जिसका नशा आदमी को कहीं भी, कभी भी नंगा खड़ा कर देता और क्यों ना हो भला आखिर सरकार भी तो हमारी है।
घर की तरफ मे भागमभाग दक्षिणपुरी मे आखिर क्यों हुआ? ये क्या दौर रहा है जो लोग खिंचे चले जा रहे हैं? ये पहले तो था ही नहीं। इनमे कई कारणों मे एक वज़ह ये भी है कि, नेमसिंह जी कि तरह यहाँ हजारों लोग और हैं जो टीवी, अख़बार और रेडियो पर अपने कान लगाये रखते हैं। खाली इसलिए ही नहीं की आठ फूट के दरवाजे पर हमारे नाम की तख़्ती हो या राशन कार्ड मे अपना भी नाम मुखिया की जगह हो। खाली यही नहीं है। यहाँ पर लोगों के पास मे साढ़े बाइस गज़ के मकान है। जो इंदिरा गांधी विकास से सन् 1975 मे मिले थे और आज की तारीख मे कितनों ने यहाँ खरीदे भी हैं। जिनको ऊँचा तो किया जा सकता है लेकिन फैलाया नहीं जा सकता। इसे दो या तीन, तीन या चार मंजिल बनाया जा सकता है। लेकिन जैसे-जैसे मकान ऊपर चड़ता जाता है उसकी चौड़ाई उतनी ही कम होती जाती है। कमरा एक और रहने वाले चार तो कैसे हो गुजारा? इस बड़ते परिवार की वज़ह से यहाँ पिछले साल कई मकान तो बिक भी गए हैं। मगर कुछ लोगों का कहना है कि जो यहाँ दक्षिणपुरी से बैक कर गया वो दिल्ली जैसे बड़े शहर मे बीस गज़ का भी मकान नहीं खरीद सकता। पर इसके बावज़ूद भी ये मैप अब बड़ा हो चला है। दक्षिणपुरी से दिल्ली की कई जगहें अब नजदीक हो गई हैं। संगम विहार, मीठापुर, जैतपुर, मेरठ, कंझावला तथा बदरपूर जैसी जगहें दक्षिणपुरी के मैप के साथ मे जुड़ गई हैं। बस, यहीं पर जगह मिल सकती है जिसमे चार लोगों के परिवार का गुजारा चल सकता है अथवा नहीं।
ये एक रेस है जो शुरू हो गई है जिसमे सभी भाग रहे हैं। ना जाने कौन जितेगा? पर यहाँ इस दौड़ मे सभी शामिल हैं। हाँ बस, फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि यहाँ इस दौड़ मे सभी एक-दूसरे से अंजान बनकर दौड़ रहे हैं।
"उषा देखले भगवान भी कुछ चाहता है तभी तो रिज़ल्ट दोबारा निकलवा रहा है। इस बार हमारा पक्का निकलेगा। हे माता रानी निकलवा दे तो नंगे पाँव तेरे दरवार मे आऊँगा। निकलवा दे।"
उनकी बीवी भी उनके पीछे-पीछे अपने हाथ जोड़ती हुई ऊपर वाले को देखने लगी, “आपको पता है जी विवेक के साथ क्या हुआ था? उसने सरकारी नौकरी का फार्म भरा था। उस सरकारी नौकरी का ड्रा निकाला गया तो उसमे उसका नाम नहीं आया। मगर बड़े अधिकारियों ने कहा की इसमे कुछ घपला किया गया है हम ये रिज़ल्ट दोबारा निकालेगें। बस, उसी मे उसका नाम निकल आया, सरकारी नौकरी लग गई उसकी। किसी को भी रिश्वत मे एक रुपये तक की चाय नहीं पिलाई उसने। आज देखो कितने चाव से नौकरी कर रहा है। हमारे साथ भी ऐसा ही हो तो मज़ा आ जाये। भगवान निकलवा दे।"
कुछ ऐसी ही कहानियाँ यहाँ दक्षिणपुरी की कई जगहों मे चल रही हैं। सभी का इन्तजार दोबारा से शुरू हो गया है। इतना तो शायद पास और फैल करवाने वाले स्कूल के रिज़ल्ट का भी नहीं होता। कोई बेसब्री नहीं है सब धैर्य बाँधे बैठे हैं। लगभग तीन दिन और टीवी के सामने मुँह गढ़ाये बैठे रहना होगा। सभी मनोंरजन की चीजें न्यूज़ चैनल मे तब्दील हो गई हैं। "काश के हमारा निकल आये"
ये नारा दुआओं और मांगो मे बदल गया है। उंमगें जैसे दोबारा से जीवित हो गई हैं।
लख्मी
ये ख़बर दिन-रात टीवी पर दिखाई जा रही थी और इस दौरान हर जगह न्यूज़ ख़त्म हो जाने के बाद मे बस, अपनी ही बहस शुरू हो जाती। लोग ये सुनने के लिए टीवी के सामने बैठे रहते की वो तारीख कौन सी होगी जब ये रिज़ल्ट दोबारा से निकाला जायेगा। किसी के लिए दुख के आँसू तो किसी के लिए उमगों भरे आँखू बनकर ये न्यूज़ चल रही थी। ये बिलकुल ऐसा ही था जैसे किसी खिलाड़ी को एक और एक्सट्रा बॉल मिल गई हो। अब उम्मीद होगी उस आखिरी बॉल पर छक्का लगाने की।
कई सौ-सौ रूपये के फ़ार्म भरे इन्तजार करते लोग बस, इसी राह मे थे कि कुछ तो होगा ऐसा दिल्ली जैसे बड़े शहर मे जहाँ हमारे नाम की भी कोई जगह होगी। कोई तो दरवाजा ऐसा बनेगा कभी जिसके आगे हमारे नाम की भी तख़्ती लगेगी। कोई तो ऐसा राशन कार्ड होगा जिसमे मेरा नाम सबसे ऊपर और मुखिया का ऑदा लेगा। पर क्या ये संभव है? वो भी दिल्ली जैसे बड़े शहर मे?
ये सपने हर छोटी कॉलोनियों मे रहने वाले के दिमाग मे हमेशा ताज़ा रहते हैं। जो बस, अवसर तलाशते हैं किसी ऐसे मौके का जिसमे ये कूद सकें और अपनी किश्मत आज़मा सकें। यही इन्तजार इनको हमेशा चौंकन्ना रखता है। ये हमेशा इसी ताड़ मे रहते हैं कि कोई तो फार्म निकले, किसी भी अख़बार मे जिसमे हमारे जैब की मुताबिक घर के प्लान हो। इसलिए हर अख़बार पर इनकी नज़र रहती है। चाहें ये कोई भी अख़बार खरीदे या नहीं मगर नज़र शहर मे किसी भी चाय की दुकान पर रखे अख़बारों मे या फिर राह चलते किसी भी अजनबी से रिश्ता बनाकर उसका अख़बार शेयर करने से नज़र आ ही जाती है। ये खाली अख़बार तक ही सीमित नहीं रहती। ये चाहत टीवी के हर न्यूज़ चैनल पर पँहुच ही जाती है।
अभी कुछ समय पहले ये न्यूज़ काफी जोरो से यहाँ दक्षिण पुरी मे फैली के, प्रगति मैदान मे मीडिल क्लास के लिए घर निकाले गए हैं। तो बस, पँहुच गए सभी अपने-अपने नाम से किश्मत को आज़माने, लेकिन दूसरे ही दिन जब घरों की किमतों पर सरकार ने नज़र डाली तो सब उंमगें जैसे धरी-की धरी रह गई।
नेमसिंह जी एक मात्र आदमी हैं जिनकी हर स्कीम पर निगाह रहती है। वे तो कभी भी कोई भी स्कीम नहीं छोड़ते। बस, जहाँ के बारे मे भी पूछना हो, पूछ सकते हैं। मकान लेने की ऐसी हुड़क किसी मे भी शायद देखी नहीं जा सकती। वे वहाँ प्रगति मैदान से आये और कहने लगे, "बताओ भला, घर निकाले हैं मीडिल क्लास के लिए और किमत 13 लाख से 16 लाख। अब जरा ये भी बता दो की किसी मीडिल क्लास का आदमी इस किमत मे फिट बैठता है? अच्छा ये नहीं तो ये ही बता दो की अगर मेरे जैसा आदमी बैंक से लोन भी लेगा तो उसकी मासिक किश्त कितने की होगी? लगभग देखा जाये तो 7000 रुपये से 8000 रुपये तक। अब जो आदमी महिने मे 6000 रुपये कमाता हो वो किश्त देगा तो खायेगा क्या? वाह! री सरकार, तुझे सलाम।"
ये कहते हुए वो अपने घर के अन्दर चले गए पर बात यहीं पर नहीं ख़त्म हुई थी। वे तो अब उनके बोल से निकल कर कई अलग-अलग दिमाग और ज़ुबानो मे चली गई थी। बातों ही बातों मे घरों की बातें फैल गई। लोग मकान-मकान का नारा लगाने लगे। कोई भरने की कहता तो कोई बात को टालने की। इसलिए तो यहाँ पैसा इनवेस्ट करवाने वालो की भी कमी नहीं है। बस, इच्छाएँ पकड़कर और चेहरा पढ़कर ये घुसे चले आते हैं और सब कुछ जैसे निकालकर रख देते हैं। इनके लिए सोलह या सत्तराह लाख को बॉय हाथ का खेल होता है। बैठे-बैठे कागज़ के एक छोटे से टुकड़े पर ये आपकी ज़िन्दगी का मैप बना डालते हैं और मैप मे बस, पैसा ही पैसा होता है। ये पैसा कहाँ से आयेगा और कैसे आयेगा ये सब पता होता है इन्हे। बस, ये नहीं बताते की ये पैसा मेरे पास रहेगा कब तक?
नेमसिंह जी इन सब के घेरे मे नहीं पड़ते, साफ निकल आते हैं। उन्हे पता है कि उनका पैसा कहाँ से आता है, कैसे आता है और कहाँ चला जायेगा। अपने घर मे कई समानों के साथ-साथ एक कौना ऐसा भी बनाया है जिसमे ना जाने कितने मकानों के फार्म फोटोस्टेट किये हुए रखे हैं और ना जाने कितनी अख़बार की कटींग भी। जिसमे घर के बारे मे कई प्रकार की डीटेल शामिल है। साथ-साथ सरकारी फ़्लैट के बारे मे सारी बातें भी। किसी मे गाज़ियाबाद के फार्म हैं तो किसी मे दिल्ली के। ये हर जगह अपनी किश्मत आज़माने से नहीं चूकते।
"पूरे चार सालों के बाद में निकाले हैं सरकार ये जनता फ़्लैट, और अब देखो वो भी अटक गए। ना जाने क्या होगा हमारा तो?”
दक्षिणपुरी में इन दिनों पहली बार घर लेने और पाने की मारामारी छाई रही। इतनी बातें, इतनी इच्छाएँ और इतना जोश आज से पहले नहीं था। इसके कई कारण हो सकते हैं। पर तमन्ना एक ही होगी। ये क्रैज़ खाली बदलाव के तहत ही नहीं था बल्कि अब दक्षिणपुरी ने अपने आने वाले टाइम को देखना शुरू किया था और ये सब राजीव गांधी विकास के घरों को लेकर तो कुछ ज़्यादा ही था। सबसे पहले तो घर के फार्म खरीदने की मारामारी उसके बाद मे उसको छुपाकर भरने की होंश भी। ये बड़ी मज़ेदार वारदातों से बनती है। कई खेल हैं इनमे। अगर गली में किसी एक को पता चल जाता कि सरकार ने घर निकाले हैं गरीबों के लिए तो वो किसी और को अपने मुँह से नहीं बताता। इनका मानना ये रहता है कि जितना लोगों को पता चलेगा उतने ही उम्मीदवार बड़ जायेगें और हमारे चांस कम हो जायेगें। वैसे देखा जाये तो ये खाली अपने ही मन की बनाई बात रहती। पता यहाँ पर सबको रहता बस, सभी उसको छुपाने के तरीके तलाशते रहते।
यहाँ पर ये खेल हर गली, हर नुक्कड़, हर बसस्टेंड अथवा हर बस मे भी देखा जाता। हर कोई अपनी तरह से उसको नाटने की बात करता और ये समझाने की कोशिश करता की "ये हमारे लिए नहीं है" या ये कहता के "इसमे इतने रूपये भरे जायेगें, हमारे बस का नहीं है" और ज़्यादा से ज़्यादा बताते तो कोई ये कहता कि "ये निकलेगा ही नहीं।" ताकी लोग उस तरफ ना खिंचे।
मगर वो कहते है ना, बहकावे मे ना आओ, बस अपनी अकल लगाओ। यहाँ पर भी लोग कुछ ऐसा ही करते हैं। "हाँ-हूँ" के बाद तो कहानी कुछ अलग ही मोड़ ले लेती और सरकार की झाँसों भरी स्कीम भी पूरी हो जाती। सौ-सौ रुपये लिए दिल्ली की करोंड़ों पगली जनता घर-घर चिल्लाती हुई फार्म की खिड़कियों पर टूट पड़ती। और सरकारी खातों मे वे ही सौ-सौ के नोट जैसे अरबों रुपये की बारिश कर देते। ये सौ के नोट किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन सरकार के लिए बेहद बड़ी बात थी। ये एक भूख की तरह से होती जिसका नशा आदमी को कहीं भी, कभी भी नंगा खड़ा कर देता और क्यों ना हो भला आखिर सरकार भी तो हमारी है।
घर की तरफ मे भागमभाग दक्षिणपुरी मे आखिर क्यों हुआ? ये क्या दौर रहा है जो लोग खिंचे चले जा रहे हैं? ये पहले तो था ही नहीं। इनमे कई कारणों मे एक वज़ह ये भी है कि, नेमसिंह जी कि तरह यहाँ हजारों लोग और हैं जो टीवी, अख़बार और रेडियो पर अपने कान लगाये रखते हैं। खाली इसलिए ही नहीं की आठ फूट के दरवाजे पर हमारे नाम की तख़्ती हो या राशन कार्ड मे अपना भी नाम मुखिया की जगह हो। खाली यही नहीं है। यहाँ पर लोगों के पास मे साढ़े बाइस गज़ के मकान है। जो इंदिरा गांधी विकास से सन् 1975 मे मिले थे और आज की तारीख मे कितनों ने यहाँ खरीदे भी हैं। जिनको ऊँचा तो किया जा सकता है लेकिन फैलाया नहीं जा सकता। इसे दो या तीन, तीन या चार मंजिल बनाया जा सकता है। लेकिन जैसे-जैसे मकान ऊपर चड़ता जाता है उसकी चौड़ाई उतनी ही कम होती जाती है। कमरा एक और रहने वाले चार तो कैसे हो गुजारा? इस बड़ते परिवार की वज़ह से यहाँ पिछले साल कई मकान तो बिक भी गए हैं। मगर कुछ लोगों का कहना है कि जो यहाँ दक्षिणपुरी से बैक कर गया वो दिल्ली जैसे बड़े शहर मे बीस गज़ का भी मकान नहीं खरीद सकता। पर इसके बावज़ूद भी ये मैप अब बड़ा हो चला है। दक्षिणपुरी से दिल्ली की कई जगहें अब नजदीक हो गई हैं। संगम विहार, मीठापुर, जैतपुर, मेरठ, कंझावला तथा बदरपूर जैसी जगहें दक्षिणपुरी के मैप के साथ मे जुड़ गई हैं। बस, यहीं पर जगह मिल सकती है जिसमे चार लोगों के परिवार का गुजारा चल सकता है अथवा नहीं।
ये एक रेस है जो शुरू हो गई है जिसमे सभी भाग रहे हैं। ना जाने कौन जितेगा? पर यहाँ इस दौड़ मे सभी शामिल हैं। हाँ बस, फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि यहाँ इस दौड़ मे सभी एक-दूसरे से अंजान बनकर दौड़ रहे हैं।
"उषा देखले भगवान भी कुछ चाहता है तभी तो रिज़ल्ट दोबारा निकलवा रहा है। इस बार हमारा पक्का निकलेगा। हे माता रानी निकलवा दे तो नंगे पाँव तेरे दरवार मे आऊँगा। निकलवा दे।"
उनकी बीवी भी उनके पीछे-पीछे अपने हाथ जोड़ती हुई ऊपर वाले को देखने लगी, “आपको पता है जी विवेक के साथ क्या हुआ था? उसने सरकारी नौकरी का फार्म भरा था। उस सरकारी नौकरी का ड्रा निकाला गया तो उसमे उसका नाम नहीं आया। मगर बड़े अधिकारियों ने कहा की इसमे कुछ घपला किया गया है हम ये रिज़ल्ट दोबारा निकालेगें। बस, उसी मे उसका नाम निकल आया, सरकारी नौकरी लग गई उसकी। किसी को भी रिश्वत मे एक रुपये तक की चाय नहीं पिलाई उसने। आज देखो कितने चाव से नौकरी कर रहा है। हमारे साथ भी ऐसा ही हो तो मज़ा आ जाये। भगवान निकलवा दे।"
कुछ ऐसी ही कहानियाँ यहाँ दक्षिणपुरी की कई जगहों मे चल रही हैं। सभी का इन्तजार दोबारा से शुरू हो गया है। इतना तो शायद पास और फैल करवाने वाले स्कूल के रिज़ल्ट का भी नहीं होता। कोई बेसब्री नहीं है सब धैर्य बाँधे बैठे हैं। लगभग तीन दिन और टीवी के सामने मुँह गढ़ाये बैठे रहना होगा। सभी मनोंरजन की चीजें न्यूज़ चैनल मे तब्दील हो गई हैं। "काश के हमारा निकल आये"
ये नारा दुआओं और मांगो मे बदल गया है। उंमगें जैसे दोबारा से जीवित हो गई हैं।
लख्मी
अंजान शख़्स
माहौल ओस के कोहरे से ढका हुआ था। ठन्ड के तापमान को पिघलाता, कहीं से लपलपाती आग का धुंआ आ रहा था। कुड़ेदानों में कल रात का कचरा भरा पड़ा था। केक के डिब्बे, बीयर के पिचके हुए डिब्बे और बोतलें तो कहीं अभी भी खुशबू छोड़ते गैंदे और गुलाब के फूल जिसे गाय अपना चारा समझकर खा रही थी।
रातभर की इस्तमाल की गई चीजों को कूड़ेदान में फैंक दिया गया था। बची हुई खाने की झूठी चीजों को कुत्ते नौंच-नौंचकर खा रहे थे। उनका मुँह कचरे मे धसा हुआ था। इतने मे उस जगह में कोहरे को चीरकर कोई अंजान शख़्स अन्दर आया। बे-आवाज माहौल में जैसे तार से बज उठे। उसने अपने आप को फटे कम्बल से लपेट रखा था। उस के पैरों में मैले जूते थे। जो राख और मिट्टी मे सने हुए थे। चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। बस, हाथ और पाँव ही नज़र आ रहे थे। वो सड़क पर घूमते हुए हाथ मे एक डन्डा लेकर उसमे चुम्बक फँसाकर घसीटता हुआ चला आ रहा था। मिट्टी में शामिल छोटे-छोटे लोहे की चीजों के टुकड़े को उसके डन्डे में लगी चुम्बक खींच लेती।
सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था। समय का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था पर इस मुश्किल मे भी वो अपना काम करने आ गया। कमर पर झोले में उसने काफी सामान रखा हुआ था। वो पहले भी कई बार यहाँ दिखाई दिया था पर अकेला नहीं। आज वो अकेला ही आया था। उसके साथ कोई नहीं था। सड़क से गुजरने वाले स्कूटर, कार वगैहरा। कोई वाहन जब तेजी से वहाँ से निकल जाते तो हवा का झौंका माहौल को और भी ठन्डा कर देता और उसके हाथ-पैर से कपकपी छूटने लगती।
पुराने पार्क के साथ में बना ये कूड़ेदान जो सालो पुराना है। जिसमे ब्लॉक के हर घर का इस्तमाल कि हुई चीजों को फैंका जाता। इस रास्ते पर वो सालो से आता-जाता रहा है। उस का चुम्बकिये औजार उसका साथ देता रहता। जमीन पर उस चुम्बक को वो घसीटता हुआ लेकर चलता और जो भी चीजें उससे चुपकती। वो उन्हे अपने झोले मे रख लेता।
दिन मे अंगिनत बार वो इस तरह करता। न जाने कहाँ-कहाँ जाता। पूरे इलाके में घूमकर वो जमीन पर पड़े कीलों, बोतलों के ढक्कनों अन्य चीजों के बेकार हिस्सों को वो अपने पास इक्कठा करके उन्हे बैच देता और अपने लिए कुछ पैसे बना लेता। दिनभर गली-गली भटकने के बाद वो जैसे धूंध से भरे कोहरे को चीरकर आता। वैसे ही शाम जब जगह मे दस्तक देती तो वो धूंध में ही कहीं छूप जाता।वो कहाँ से आया और कहाँ गया। ये किसी को पता नहीं चलता। दक्षिणपूरी से कहीं दूर उसका बसेरा होगा। कुछ पता नहीं। लेकिन कुछ क्षणों के लिए वो जाना-पहचाना सा लगा। उसके जाते ही आसपास सब नज़र आने लगा।
तब शरीर को गर्मी देते शख़्स आग को चारों तरफ से घेरकर बैठे होते। रात के अंधेरे को खम्बों पर लगे बल्बों की रोशनियाँ मुँह चिड़ाती हुई होती। कहीं परछाई अपना ही समा बनाकर किसी नज़र की फिराक में होती।
राकेश
रातभर की इस्तमाल की गई चीजों को कूड़ेदान में फैंक दिया गया था। बची हुई खाने की झूठी चीजों को कुत्ते नौंच-नौंचकर खा रहे थे। उनका मुँह कचरे मे धसा हुआ था। इतने मे उस जगह में कोहरे को चीरकर कोई अंजान शख़्स अन्दर आया। बे-आवाज माहौल में जैसे तार से बज उठे। उसने अपने आप को फटे कम्बल से लपेट रखा था। उस के पैरों में मैले जूते थे। जो राख और मिट्टी मे सने हुए थे। चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। बस, हाथ और पाँव ही नज़र आ रहे थे। वो सड़क पर घूमते हुए हाथ मे एक डन्डा लेकर उसमे चुम्बक फँसाकर घसीटता हुआ चला आ रहा था। मिट्टी में शामिल छोटे-छोटे लोहे की चीजों के टुकड़े को उसके डन्डे में लगी चुम्बक खींच लेती।
सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था। समय का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था पर इस मुश्किल मे भी वो अपना काम करने आ गया। कमर पर झोले में उसने काफी सामान रखा हुआ था। वो पहले भी कई बार यहाँ दिखाई दिया था पर अकेला नहीं। आज वो अकेला ही आया था। उसके साथ कोई नहीं था। सड़क से गुजरने वाले स्कूटर, कार वगैहरा। कोई वाहन जब तेजी से वहाँ से निकल जाते तो हवा का झौंका माहौल को और भी ठन्डा कर देता और उसके हाथ-पैर से कपकपी छूटने लगती।
पुराने पार्क के साथ में बना ये कूड़ेदान जो सालो पुराना है। जिसमे ब्लॉक के हर घर का इस्तमाल कि हुई चीजों को फैंका जाता। इस रास्ते पर वो सालो से आता-जाता रहा है। उस का चुम्बकिये औजार उसका साथ देता रहता। जमीन पर उस चुम्बक को वो घसीटता हुआ लेकर चलता और जो भी चीजें उससे चुपकती। वो उन्हे अपने झोले मे रख लेता।
दिन मे अंगिनत बार वो इस तरह करता। न जाने कहाँ-कहाँ जाता। पूरे इलाके में घूमकर वो जमीन पर पड़े कीलों, बोतलों के ढक्कनों अन्य चीजों के बेकार हिस्सों को वो अपने पास इक्कठा करके उन्हे बैच देता और अपने लिए कुछ पैसे बना लेता। दिनभर गली-गली भटकने के बाद वो जैसे धूंध से भरे कोहरे को चीरकर आता। वैसे ही शाम जब जगह मे दस्तक देती तो वो धूंध में ही कहीं छूप जाता।वो कहाँ से आया और कहाँ गया। ये किसी को पता नहीं चलता। दक्षिणपूरी से कहीं दूर उसका बसेरा होगा। कुछ पता नहीं। लेकिन कुछ क्षणों के लिए वो जाना-पहचाना सा लगा। उसके जाते ही आसपास सब नज़र आने लगा।
तब शरीर को गर्मी देते शख़्स आग को चारों तरफ से घेरकर बैठे होते। रात के अंधेरे को खम्बों पर लगे बल्बों की रोशनियाँ मुँह चिड़ाती हुई होती। कहीं परछाई अपना ही समा बनाकर किसी नज़र की फिराक में होती।
राकेश
लेखन के तरीके क्या हैं?
इन दिनों मैं कुछ ऐसी रचनाये लिखने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे पास या नज़दीक की बिलकुल नहीं है और ना ही मैंने कभी सुनी है। लेकिन उस काल्पनिक दुनिया को कभी- किसी और ही तरह के जीवन से समझने की कोशिश की है। यानि के किसी के रहन-सहन के नतीजे से वे कई अनेको चित्र उभरें हैं। जिनको वास्तविक रूप मे देखा भी जा सकता है और उन्हे काल्पनिक करकर टाला भी जा सकता है। ये वे रूप भी है जिन्हे अपने मौज़ूदा रूप से बाँधा भी जा सकता है और उसे दूर भी फैंका जा सकता है। लेकिन इसमे जब मैं किसी ब्यौरे या शख़्स का बख़ान करता हूँ तो उसमे मेरा होना हमेशा मुझे बाधा मे डाल देता हैं मुझे लगता है कि मैं उस जीवन की जितनी भी परेशानियाँ या फैसलों को लिख रहा हूँ वे मेरे होने से क्या आकार लेती हैं या मैं उन्हे क्यों वे रूप दे रहा हूँ जो असल मे किसी रूप की पेशकश ही नहीं रखती।
कभी मैं उस जीवन को उनके घर के अन्दर से लिखता हूँ तो कभी बाहर मे खड़ा होकर, कभी मैं वो बन जाता हूँ तो कभी उससे कोसों की दूरी बना लेता हूँ। जहाँ से उसकी हलचल दिखती है लेकिन उसकी बैचेनी नहीं।
इस स्थिति मे मैं एक बेजान शब्द बनकर रह जाता हूँ जिसको जान उस छवि के हिलने, डुलने, बोलने, चलने, कहने या भाव से मिलेगी। उस जीवन से मेरा रिश्ता किस आधार का है? क्या वो दूर बैठा कोई ऐसा अक्स है जिसे किसी रूप की चेष्टा है या मेरे लिए वे एक ऐसी छवि है जिसका रूप मेरे अस्तित्व से ओझल है। मैं वहाँ पर इतना ताकतवर क्यों हूँ?
मेरा उसके जीवन से कोई या किसी भी प्रकार का नाता नहीं है। ना ही कभी बन सकता लेकिन फिर भी मैं उनके बीच मे खड़ा होकर ये बना पाता हूँ। जिसका आभाष मेरे लिए या मेरी सोच के लिए या फिर मेरे परिवेश के लिए एक चित्र की भांति उभरकर सामने चला आता है पर ये लेखन उस मूरत मे क्या फूँकता है जो मेरे हिस्से से है?
देखकर लिखना, बनकर लिखना, बोलकर लिखना, सुनकर लिखना या पहला केरेक्टर, दूसरा केरेक्टर या फिर तीसरा केरेक्टर बनकर लिखना उस दूर बैठी छवि या ज़िन्दगानी को मेरे समीप लाने की क्या इच्छाए जगाता है? मुझे कभी अपने से बहस जब करनी होती है तो मैं इस तरह के तरीके अपनाता हूँ जो की मेरे जीवन के, मेरे खुद से बनाये पात्रो से बेइन्तहा बहस करता है और टकराता भी है। इसे मैं और आप जुझना भी कह सकते हैं। जो शायद आखिरकार बहुत ऊंची सोच साबित होता है। कई बार किसी दूर बैठी ज़िन्दगी मे घूसने के तरीके हम ऐसे बनाते हैं जैसे किसी लेखन की रचना मे और उसे पेशकश की दुनिया का हिस्सेदार बना लेते हैं। कभी-कभी बीच मे खड़ा होकर दुनिया देखने का मज़ा उस दोनों तरफ़ खड़ी ज़िन्दगियों के लिए रोक या हदें बन जाता है। ये शायद ऐसा भी होता है जैसे-
कोई शख़्स है जो अपने परिवेश से बहस या समझौते करके जीवन व्यतित कर रहा है। जो पूरे दिन या समझौतों मे कुछ टाइम अपने लिए बचा लेता है। बस, तभी वे अपने लिए कुछ कर पाता है। नज़र उस बीच के समय पर चली जाती है। ना जाने हम कौन सा बिन्दू छेड़ देते हैं कि इच्छाए शब्द ले लेती हैं और उस परिवेश के सामने हम सीना ताने खड़े हो जाते हैं। वे दौर हमारे लिए बेहद कठोर, टक्कर, हादसा या सीधे शब्दों मे कहे तो वे हथियार बनकर हमारे सामने अपनी मूरत बना लेता है। हम चाहें तो हर चीज पर सवाल रखकर उसे नंगा कर सकते हैं पर बिना सवाल किए हम उस मूरत मे कैसे शामिल हो सकते हैं वे ही जीवन का आधार हैं।
मैं कभी दूर खड़ा जब किसी शख़्स या उसकी बैचेनी को देखता हूँ तो उसको अपने नजदीक लाना आसान सा लगता है लेकिन जब मैं वो बनकर उसकी बैचेनी को सोचता हूँ तो वे कठीन और जटिल बन जाता है। - जब मैं वही शख़्स बन जाता हूँ तो उसकी बैचेनी को महसूस करके लिखने मे मुझे लगता है कि वे मुझतक बेहद नज़दीकी पा रही है और जब मैं उससे दूरी बनाकर लिखता हूँ तो वे बैचेनी किसी टिप्पणी की भांति रहती है।
जब हम बीच मे रहकर किसी वस्तु को अपने समीप लाते हैं तो वे जान मांगती है। हम उसमे सांस और धड़कन भरने की कोशिश करते हैं और उसे सांस लेने के लिए छोड़ देते हैं। पर जब कोई शख़्स या जीवन को हम अपने समीप लाते हैं तो उसकी मांग हमारी ज़ुबानी मे कहाँ पर आकर रूकती है?
हम कभी-कभी दूरी व नजदीकी मे अपने शब्दों के आकार को समझ नहीं पाते। ये बिलकुल वैसे ही होता है जैसे कोई पेन्टर अपनी पेन्टिग बनाने मे मग़्न है और उसके रंग का भरपूर लुफ़्त ले रहा है। उसे ये तक पता नहीं होता की जब ये कोई रूप ले पायेगी तो क्या चेहरा होगा इसका। वे तो बस, लीन रहता है। कहीं खो जाता है। जब वे मूरत बनकर सामने आती है तो कोई ऐसा रूप लेकर रखती है जिसका अन्दाजा हमें व बनाने वाले को भी पता नहीं होता।
वैसे ही जब हम किसी शख़्स को लिख रहे होते हैं तो उसके जीवन की रचना मे हम अपने शब्दों को कुछ इस तरह से आजाद छोड़ देते हैं कि वे उस नज़र आने वाली छवि से कुछ और ही ताज़ेपन की बुनाई कर देते हैं। जो बनकर आता है वे वो दिखने वाली तस्वीर नहीं होती। वे किसी और ही रंग- लिबास का एक बहुत अच्छा खासा आकार होती है। लेकिन जब ये वापस उस परिवेश मे जाती है तो क्या उस रूप की सम्भावनायें उसे उस जगह का मानने के लिए तैयार होती है? हम उसे किस बहस के लिए तैयार कर पाये होते हैं?
मैंने कुछ किताबें पढ़ी जिसमे लेखन के तरीके व किसी के अन्दर दाखिल होने के तरीके किसी को दोहराने के अन्दाज से कम नहीं थे। वे चाहें कोई बेजान चीज हो या जीवित। जो उस रूप को बताने मे बेहद टाइट रहते हैं। उसके खेल या उससे खेल दोनों को समाज के बलबूते पर मजबूत बनाने के लिए तैयार करते हैं। लेख मे आने के तरीके भी अन्य तरह के होते हैं जो लेखक को खोजने की चेष्टा जगाते हैं। उसके पीछे जाने को कहते हैं। कुछ तलाश्ने को कहते हैं। कभी-कभी कोसते भी हैं कि ये अन्दाज क्या नहीं है तेरे पास।
इससे मगर वे जीवन अपने शरीर मे घुल जायेगा ये तय नहीं होता। या मैं घोलने की क्यों कह रहा हूँ वे भी शायद सवाल ही बन कर रह जाता है। किसी मे दाखिल होने के तरीके को कितना बेइन्तिहाइ बनाया जा सकता है। जो ज़्यादा की मांग ना रखे मगर ज़्यादा को भरपूर खेलने का मौका दे। यानि के ज़्यादा नज़दीक, ज़्यादा रूपक, ज़्यादा परिवेश, ज़्यादा समाजिक-बौद्धिक व ज़्यादा विवरण।
लख्मी
कभी मैं उस जीवन को उनके घर के अन्दर से लिखता हूँ तो कभी बाहर मे खड़ा होकर, कभी मैं वो बन जाता हूँ तो कभी उससे कोसों की दूरी बना लेता हूँ। जहाँ से उसकी हलचल दिखती है लेकिन उसकी बैचेनी नहीं।
इस स्थिति मे मैं एक बेजान शब्द बनकर रह जाता हूँ जिसको जान उस छवि के हिलने, डुलने, बोलने, चलने, कहने या भाव से मिलेगी। उस जीवन से मेरा रिश्ता किस आधार का है? क्या वो दूर बैठा कोई ऐसा अक्स है जिसे किसी रूप की चेष्टा है या मेरे लिए वे एक ऐसी छवि है जिसका रूप मेरे अस्तित्व से ओझल है। मैं वहाँ पर इतना ताकतवर क्यों हूँ?
मेरा उसके जीवन से कोई या किसी भी प्रकार का नाता नहीं है। ना ही कभी बन सकता लेकिन फिर भी मैं उनके बीच मे खड़ा होकर ये बना पाता हूँ। जिसका आभाष मेरे लिए या मेरी सोच के लिए या फिर मेरे परिवेश के लिए एक चित्र की भांति उभरकर सामने चला आता है पर ये लेखन उस मूरत मे क्या फूँकता है जो मेरे हिस्से से है?
देखकर लिखना, बनकर लिखना, बोलकर लिखना, सुनकर लिखना या पहला केरेक्टर, दूसरा केरेक्टर या फिर तीसरा केरेक्टर बनकर लिखना उस दूर बैठी छवि या ज़िन्दगानी को मेरे समीप लाने की क्या इच्छाए जगाता है? मुझे कभी अपने से बहस जब करनी होती है तो मैं इस तरह के तरीके अपनाता हूँ जो की मेरे जीवन के, मेरे खुद से बनाये पात्रो से बेइन्तहा बहस करता है और टकराता भी है। इसे मैं और आप जुझना भी कह सकते हैं। जो शायद आखिरकार बहुत ऊंची सोच साबित होता है। कई बार किसी दूर बैठी ज़िन्दगी मे घूसने के तरीके हम ऐसे बनाते हैं जैसे किसी लेखन की रचना मे और उसे पेशकश की दुनिया का हिस्सेदार बना लेते हैं। कभी-कभी बीच मे खड़ा होकर दुनिया देखने का मज़ा उस दोनों तरफ़ खड़ी ज़िन्दगियों के लिए रोक या हदें बन जाता है। ये शायद ऐसा भी होता है जैसे-
कोई शख़्स है जो अपने परिवेश से बहस या समझौते करके जीवन व्यतित कर रहा है। जो पूरे दिन या समझौतों मे कुछ टाइम अपने लिए बचा लेता है। बस, तभी वे अपने लिए कुछ कर पाता है। नज़र उस बीच के समय पर चली जाती है। ना जाने हम कौन सा बिन्दू छेड़ देते हैं कि इच्छाए शब्द ले लेती हैं और उस परिवेश के सामने हम सीना ताने खड़े हो जाते हैं। वे दौर हमारे लिए बेहद कठोर, टक्कर, हादसा या सीधे शब्दों मे कहे तो वे हथियार बनकर हमारे सामने अपनी मूरत बना लेता है। हम चाहें तो हर चीज पर सवाल रखकर उसे नंगा कर सकते हैं पर बिना सवाल किए हम उस मूरत मे कैसे शामिल हो सकते हैं वे ही जीवन का आधार हैं।
मैं कभी दूर खड़ा जब किसी शख़्स या उसकी बैचेनी को देखता हूँ तो उसको अपने नजदीक लाना आसान सा लगता है लेकिन जब मैं वो बनकर उसकी बैचेनी को सोचता हूँ तो वे कठीन और जटिल बन जाता है। - जब मैं वही शख़्स बन जाता हूँ तो उसकी बैचेनी को महसूस करके लिखने मे मुझे लगता है कि वे मुझतक बेहद नज़दीकी पा रही है और जब मैं उससे दूरी बनाकर लिखता हूँ तो वे बैचेनी किसी टिप्पणी की भांति रहती है।
जब हम बीच मे रहकर किसी वस्तु को अपने समीप लाते हैं तो वे जान मांगती है। हम उसमे सांस और धड़कन भरने की कोशिश करते हैं और उसे सांस लेने के लिए छोड़ देते हैं। पर जब कोई शख़्स या जीवन को हम अपने समीप लाते हैं तो उसकी मांग हमारी ज़ुबानी मे कहाँ पर आकर रूकती है?
हम कभी-कभी दूरी व नजदीकी मे अपने शब्दों के आकार को समझ नहीं पाते। ये बिलकुल वैसे ही होता है जैसे कोई पेन्टर अपनी पेन्टिग बनाने मे मग़्न है और उसके रंग का भरपूर लुफ़्त ले रहा है। उसे ये तक पता नहीं होता की जब ये कोई रूप ले पायेगी तो क्या चेहरा होगा इसका। वे तो बस, लीन रहता है। कहीं खो जाता है। जब वे मूरत बनकर सामने आती है तो कोई ऐसा रूप लेकर रखती है जिसका अन्दाजा हमें व बनाने वाले को भी पता नहीं होता।
वैसे ही जब हम किसी शख़्स को लिख रहे होते हैं तो उसके जीवन की रचना मे हम अपने शब्दों को कुछ इस तरह से आजाद छोड़ देते हैं कि वे उस नज़र आने वाली छवि से कुछ और ही ताज़ेपन की बुनाई कर देते हैं। जो बनकर आता है वे वो दिखने वाली तस्वीर नहीं होती। वे किसी और ही रंग- लिबास का एक बहुत अच्छा खासा आकार होती है। लेकिन जब ये वापस उस परिवेश मे जाती है तो क्या उस रूप की सम्भावनायें उसे उस जगह का मानने के लिए तैयार होती है? हम उसे किस बहस के लिए तैयार कर पाये होते हैं?
मैंने कुछ किताबें पढ़ी जिसमे लेखन के तरीके व किसी के अन्दर दाखिल होने के तरीके किसी को दोहराने के अन्दाज से कम नहीं थे। वे चाहें कोई बेजान चीज हो या जीवित। जो उस रूप को बताने मे बेहद टाइट रहते हैं। उसके खेल या उससे खेल दोनों को समाज के बलबूते पर मजबूत बनाने के लिए तैयार करते हैं। लेख मे आने के तरीके भी अन्य तरह के होते हैं जो लेखक को खोजने की चेष्टा जगाते हैं। उसके पीछे जाने को कहते हैं। कुछ तलाश्ने को कहते हैं। कभी-कभी कोसते भी हैं कि ये अन्दाज क्या नहीं है तेरे पास।
इससे मगर वे जीवन अपने शरीर मे घुल जायेगा ये तय नहीं होता। या मैं घोलने की क्यों कह रहा हूँ वे भी शायद सवाल ही बन कर रह जाता है। किसी मे दाखिल होने के तरीके को कितना बेइन्तिहाइ बनाया जा सकता है। जो ज़्यादा की मांग ना रखे मगर ज़्यादा को भरपूर खेलने का मौका दे। यानि के ज़्यादा नज़दीक, ज़्यादा रूपक, ज़्यादा परिवेश, ज़्यादा समाजिक-बौद्धिक व ज़्यादा विवरण।
लख्मी
Friday, January 2, 2009
ईश्वर को किस ने देखा
ईश्वर को किस ने देखा या किस ने पाया है? ये सवाल अजीब से हालात पैदा करता है। लेकिन इसकी बनावट कैसी है या ये कैसे पैदा हुआ है और इसकी वास्तविकता यानी होने को हम धारण कर के जीते हैं। तो कैसे क्योंकि ये माना गया है कि "ये परम सत्य है।"
आज लोग चाहें कितने भी धर्म बताये, कितने भी समाज बनाये पर उस का एक ही धर्म है। एक ही समाज है जिसके भीतर खुशहाल और अधिकार के साथ जीना है। भले ही धर्म के नाम पर इंसान को बाँट दिया हो लेकिन उसके वज़ूद को उसकी वास्तविकता से अलग नहीं कर सकते और उसकी वास्तविकता ये है की जब किसी को भूख लगती है तो भोजन की आवश्यकता को मानना ही पड़ता है।
इंसान को इंसान की जरूरत का अहसास सिर्फ़ रोटी, कपड़ा और मकान ही नहीं होता बल्कि अपने विचारों से उत्पन्न सम्भावनाओं और जिज्ञासाओं को गहरा करने की शिरकत करना भी जरूरी है। भूख तो जानवर को भी लगती है, नींद तो उसे भी आती है। ठिकाना तो उसे भी चाहिये होता है। इंसान और जानवर के बीच की दूरी शायद कोई तय नहीं कर सकता है। आखिर ये दूरी क्या है? और क्या कल्पना करती है?
जो इंसान और जानवर के लिए प्रेम और वात्शल्लायता बनकर एक माँ की तरह इस विभाजन को समझौता बना देती है जिसे अक्सर हम समझ नहीं पाते लेकिन अपना लेते हैं। नदी जितनी शान्त और निर्मल होती है वो उतनी ही गहरी भी होती है। ये हम मानते आये हैं। हमें हमारे अलग-अलग समाजों मे इसे अपनी-अपनी ज़ुबानों मे समझाने की कोशिस कि है। ये जरूरी नहीं है की इंसान किसी धर्म को अपनाकर समाज मे निर्भय होकर जी लेगा। वो जहाँ जायेगा उसके लिए डर बना रहेगा। क्योंकि कोई भी इंसान अपने मुताबिक नहीं जी सकता। उसे अपनी सीमाओं मे ही रहना होगा। ये तय कर दिया गया है। हम चाहकर भी अपने लिए जगह बनाने की कइ अनेकों कल्पनाए करते हैं, सोचते हैं, कोशिश करते हैं पर ये किसके लिए है?
समाज मे सब कुछ उल्टा ही दिखता है और कभी-कभी सीधा भी लेकिन, ये आप पर निर्भर है की आप किसे और कौन से दृष्टीकोण से माहौल को देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये भी सोच सकते हैं की आपके पास क्या नज़रिये और फ्रैम हैं? जिससे आप झाँकने कि फ़िराक मे हैं।
समाज मे जीने वाला हर इंसान, हर शख़्स एक तरह का उबाल लिए रहता है जिसका तापमान कभी बड़ जाता है तो कभी गिर जाता है। जो कभी इतनी जोरों से खौलता है की उसके आसपास तैर रही वायु भी उससे प्रभावित हो जाती है। इस उबाल को समझना जरा कठीन है। इससे पैदा होने वाली उष्मा को आप जगह-जगह रूपान्तरण होता पा सकते हैं। ये उष्मा तरह-तरह की है जिसका अवलोकन वायुमण्डल में होता रहता है। विज्ञान ईश्वर को शायद नकरात्मक सोच से देखता है। उसके पास ईश्वर की मौज़ूदगी के ऐसे ही समीकरण हैं जो तत्वों के मिलाप से ही बनते हैं पर असत्य है। इसको एक और विधी से जान सकते है जैसे- पारदर्शी शब्द बना कैसे, इस पर अगर तमाम चीजों पर खोज की जाये तो अधिकतर चीजें पारदर्शी निकल कर आयेगी और कई चट्टान की तरह ठोस।
हम और विज्ञान तीसरी आँख तलाशने के सदियों से शौध बना रहे हैं। बस, माध्यम अलग-अलग हैं। कोई पारिवार मे खोज जारी रखता है तो कोई पारिवार को त्याग कर ऑझाओं और फकीरों की भांती साधना मे लीन होकर दिव्यमान रोशनी को पाने के लिए समाज के सभी योगों से अलग अदभूत योग मे खोए हुए है।
वो अपने पूरक को तलाश्ने के लिए तप करने लग जाता है। क्योंकि वो किसी दिव्य आत्मा के महासागर के मंथन से निकला रत्न है। जो अपने प्रभू के आदेश को पाकर आया है। उस प्रभू ने अपने रूप से ही उसका शरीर बनाया है। उसमे अपनी आत्मा को उसमें बसाया है। जिसने देखने के लिए इंसान को तरह-तरह की इंद्रियाँ दी है। शरीर की हर बनावट को उस प्रभू ने सोच-सोच कर बनाया है।
धर्म तो केवल अपनी तरफ ले जाने वाला झुंड है जिसमें इंसान अपने को पूरा महसूस करता है और अपने को आइने में इतराकर देखता है और भूल जाता है की वो जिसका अंश है उसी का अलोचक बन गया है।
उसे के अस्तित्व को नकार रहा है। जिसने जीवन दिया है। पिता जैसे बच्चे के नामकर्ण और उस की पहचान जन्म से ही बना देता है वैसे ही हमारा जीवन भी उस पर्मपिता की असीम अनूकम्पा की देन है। फिर हम कौन होते है धर्म, जाति और सरहदों को बाँटने वाले।
एक फ़िल्म देखी उसमे फ़िल्म के शुरू मे ही कुछ डायलॉग हैं जो एक भगवान कह रहा है, वे कहता है:- "मैंने ये दुनिया बनाई, हवा बनाई, पानी बनाया, जीवन बनाना और इंसान बनाये, फिर उसके बाद इंसान ने मुझे बनाया, शायद मुझे पाने के लिए नहीं बल्कि मुझे दोश देने के लिए।"
ये लाइने हमारे लिए क्या है? ये एक नाटक है, जो शुरू हुआ और समाप्त हो गया। लोग क्या लेकर गए। या ये क्या सोचकर लिखे गए। सभी कह रहे हैं अपने-अपने लव्ज़ों अपने-अपने शब्द। जो कहीं खींचकर लेक जाने की कशिश मे हैं।
विश्व का हर इंसान हर शख़्स प्रभू के स्वरूपों को स्वीकारता है। ठीक उसी तरह जिस तरह बड़े से वर्गाकार मे अंधेरे में टिम-टिमाते जूगनू अपने से निकली रोशनी में एक-दूसरे से रू-ब-रू होते हैं और हमारे लिए कई देखने के फ़्रैम छोड़ते हैं।
राकेश
आज लोग चाहें कितने भी धर्म बताये, कितने भी समाज बनाये पर उस का एक ही धर्म है। एक ही समाज है जिसके भीतर खुशहाल और अधिकार के साथ जीना है। भले ही धर्म के नाम पर इंसान को बाँट दिया हो लेकिन उसके वज़ूद को उसकी वास्तविकता से अलग नहीं कर सकते और उसकी वास्तविकता ये है की जब किसी को भूख लगती है तो भोजन की आवश्यकता को मानना ही पड़ता है।
इंसान को इंसान की जरूरत का अहसास सिर्फ़ रोटी, कपड़ा और मकान ही नहीं होता बल्कि अपने विचारों से उत्पन्न सम्भावनाओं और जिज्ञासाओं को गहरा करने की शिरकत करना भी जरूरी है। भूख तो जानवर को भी लगती है, नींद तो उसे भी आती है। ठिकाना तो उसे भी चाहिये होता है। इंसान और जानवर के बीच की दूरी शायद कोई तय नहीं कर सकता है। आखिर ये दूरी क्या है? और क्या कल्पना करती है?
जो इंसान और जानवर के लिए प्रेम और वात्शल्लायता बनकर एक माँ की तरह इस विभाजन को समझौता बना देती है जिसे अक्सर हम समझ नहीं पाते लेकिन अपना लेते हैं। नदी जितनी शान्त और निर्मल होती है वो उतनी ही गहरी भी होती है। ये हम मानते आये हैं। हमें हमारे अलग-अलग समाजों मे इसे अपनी-अपनी ज़ुबानों मे समझाने की कोशिस कि है। ये जरूरी नहीं है की इंसान किसी धर्म को अपनाकर समाज मे निर्भय होकर जी लेगा। वो जहाँ जायेगा उसके लिए डर बना रहेगा। क्योंकि कोई भी इंसान अपने मुताबिक नहीं जी सकता। उसे अपनी सीमाओं मे ही रहना होगा। ये तय कर दिया गया है। हम चाहकर भी अपने लिए जगह बनाने की कइ अनेकों कल्पनाए करते हैं, सोचते हैं, कोशिश करते हैं पर ये किसके लिए है?
समाज मे सब कुछ उल्टा ही दिखता है और कभी-कभी सीधा भी लेकिन, ये आप पर निर्भर है की आप किसे और कौन से दृष्टीकोण से माहौल को देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये भी सोच सकते हैं की आपके पास क्या नज़रिये और फ्रैम हैं? जिससे आप झाँकने कि फ़िराक मे हैं।
समाज मे जीने वाला हर इंसान, हर शख़्स एक तरह का उबाल लिए रहता है जिसका तापमान कभी बड़ जाता है तो कभी गिर जाता है। जो कभी इतनी जोरों से खौलता है की उसके आसपास तैर रही वायु भी उससे प्रभावित हो जाती है। इस उबाल को समझना जरा कठीन है। इससे पैदा होने वाली उष्मा को आप जगह-जगह रूपान्तरण होता पा सकते हैं। ये उष्मा तरह-तरह की है जिसका अवलोकन वायुमण्डल में होता रहता है। विज्ञान ईश्वर को शायद नकरात्मक सोच से देखता है। उसके पास ईश्वर की मौज़ूदगी के ऐसे ही समीकरण हैं जो तत्वों के मिलाप से ही बनते हैं पर असत्य है। इसको एक और विधी से जान सकते है जैसे- पारदर्शी शब्द बना कैसे, इस पर अगर तमाम चीजों पर खोज की जाये तो अधिकतर चीजें पारदर्शी निकल कर आयेगी और कई चट्टान की तरह ठोस।
हम और विज्ञान तीसरी आँख तलाशने के सदियों से शौध बना रहे हैं। बस, माध्यम अलग-अलग हैं। कोई पारिवार मे खोज जारी रखता है तो कोई पारिवार को त्याग कर ऑझाओं और फकीरों की भांती साधना मे लीन होकर दिव्यमान रोशनी को पाने के लिए समाज के सभी योगों से अलग अदभूत योग मे खोए हुए है।
वो अपने पूरक को तलाश्ने के लिए तप करने लग जाता है। क्योंकि वो किसी दिव्य आत्मा के महासागर के मंथन से निकला रत्न है। जो अपने प्रभू के आदेश को पाकर आया है। उस प्रभू ने अपने रूप से ही उसका शरीर बनाया है। उसमे अपनी आत्मा को उसमें बसाया है। जिसने देखने के लिए इंसान को तरह-तरह की इंद्रियाँ दी है। शरीर की हर बनावट को उस प्रभू ने सोच-सोच कर बनाया है।
धर्म तो केवल अपनी तरफ ले जाने वाला झुंड है जिसमें इंसान अपने को पूरा महसूस करता है और अपने को आइने में इतराकर देखता है और भूल जाता है की वो जिसका अंश है उसी का अलोचक बन गया है।
उसे के अस्तित्व को नकार रहा है। जिसने जीवन दिया है। पिता जैसे बच्चे के नामकर्ण और उस की पहचान जन्म से ही बना देता है वैसे ही हमारा जीवन भी उस पर्मपिता की असीम अनूकम्पा की देन है। फिर हम कौन होते है धर्म, जाति और सरहदों को बाँटने वाले।
एक फ़िल्म देखी उसमे फ़िल्म के शुरू मे ही कुछ डायलॉग हैं जो एक भगवान कह रहा है, वे कहता है:- "मैंने ये दुनिया बनाई, हवा बनाई, पानी बनाया, जीवन बनाना और इंसान बनाये, फिर उसके बाद इंसान ने मुझे बनाया, शायद मुझे पाने के लिए नहीं बल्कि मुझे दोश देने के लिए।"
ये लाइने हमारे लिए क्या है? ये एक नाटक है, जो शुरू हुआ और समाप्त हो गया। लोग क्या लेकर गए। या ये क्या सोचकर लिखे गए। सभी कह रहे हैं अपने-अपने लव्ज़ों अपने-अपने शब्द। जो कहीं खींचकर लेक जाने की कशिश मे हैं।
विश्व का हर इंसान हर शख़्स प्रभू के स्वरूपों को स्वीकारता है। ठीक उसी तरह जिस तरह बड़े से वर्गाकार मे अंधेरे में टिम-टिमाते जूगनू अपने से निकली रोशनी में एक-दूसरे से रू-ब-रू होते हैं और हमारे लिए कई देखने के फ़्रैम छोड़ते हैं।
राकेश
चीजों का एकान्त
ऑटो का काम ख़त्म होने के बाद क्या करते कोई काम शायद बचा ही नहीं था। 35-40 की उम्र ऐसी होती है जिसमें शहर में कोई नौकरी नहीं होती तो क्या करते?
शिवराम जी की भी कुछ यही दिक्कत थी। अक्सर अपना ऑटो वो शमशान घाट के नल से आते पानी से धोया करते थे। सुबह 7 बजे से 8 बजे तक उनका यही काम रहता। इस दौरान शमशान घाट में भी बहुत शांती रहती। बहुत कम बार हुआ था कि इस वक़्त में कोई अर्थी आए। जब भी कभी आती तो वो अपनी सफ़ाई छोड़कर दो कदम उनके कदमों से मिला लेते और दूर से ही नमस्कार कर अपने काम मे वापस लग जाते।
शमशान घाट के पंडितजी के साथ में अच्छी जान-पहचान थी इनकी। शाम में काफी बार 4-5 घंटे साथ बिताए थे। अक्सर शाम में वो वापस आकर अपना ऑटो उसी नल के साथ खड़ा करते और ताला चैन के साथ उसी से बाँध देते। कोई भी शाम ऐसी ना थी जिसमें उन्होंने शमशान घाट में आग ना देखी हो। कभी कोई आग सुलघ रही होती तो कभी बहुत तेज़ उठ रही होती। कभी कोई उस आग के सामने खड़ा दिखता तो कभी वो अपने में एकान्त सुलघती रहती और किसी और के चले जाने का ज्ञात हो जाता।
सुबह और शाम का देखना अब बड़ा हो गया था। ऑटो का सी.एन.जी में तब्दील होना शिवराम जी के लिए तो छोटा ना था। चाहते ना चाहते उनको अपने ऑटो का काम बंद ही करना पड़ा। पूरा दिन बिताना अब आसान नहीं था। 35-40 की उम्र थी और शहर की गुंजाइशें ख़त्म पर थी। वो अपना पूरा दिन शमशान घाट में ही बिताने लगे। कुछ दिन तक वहाँ आते चढ़ावे में उनका हिस्सा रहता। वहाँ पर आए आटा, दाल, चावल, चीनी, और कपड़े और कई वो चीजें जो लोग अपने मर जाने वाले के नाम पर दे जाया करते थे उनको पंडितजी अपने घर में इस्तमाल कर लेते। बस, दोपहर का खाना तो शिवराम जी का वहीं से आ जाता। इस दोपहर के खाने के लिए उनको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता बस, आती हुई अर्थी को खाली जगह दिखाते और शमशान घाट के बनते पर्चे पर पंडितजी के साईन करवाते। यही काम था उनका यहाँ पर जिसकी उन्हे कोई तन्ख्या नहीं मिलती थी।
उनका अभी के दौर में तो घर से मेल-मिलाप नहीं था। वो रात में अक्सर वहीं सो जाया करते। घर के साथ में एक तन्ख्या का रिश्ता था जो अभी टूटा हुआ था। वो वहाँ अगर जाए तो क्या लेकर हाथ तो खाली थे उनके।
बस, अपना दिन बिताने के लिए वहीं मंदिर के पेड़ के नीचे बैठे शमशान घाट में अपनी नज़रे घुमाते रहते। दोपहर में कई लोग वहाँ आकार बैठते और सोते भी थे। अक्सर कूड़ा बिनने वाले बच्चे वहाँ कोनों में लगे रहते और कुछ लोग वहाँ किसी भी समाधी के ऊपर अपने पैर तानकर सो जाते। पेड़ की छाँव के नीचे बहुत शांति मिलती थी यहाँ लोगों को। वैसे यह जगह मशहूर भी शांति के लिए होती है। तो पूरा दिन उन्ही को देखकर उनका टाइम बितता रहा।
काफी टाइम से चल रहा है यह सब। अब तो जिनका कोई मर जाता वो इन्हे जगह दिखाने और चिता जलाने में मदद का कुछ दे भी जाते। वो अपने साथ से अलग से कुछ नहीं लाते हो भले ही पर जो अर्थी पर आता वो तो दिया ही जा सकता था।
एक औरत की अर्थी। बहुत लोग थे। लगता था जैसे कोई जवान और शादीशुदा औरत थी। कई साड़ियाँ चढ़ी थी उसपर। चूड़ियाँ, साड़ियाँ , सैंडिल, मेकप बोक्स, सारी दुल्हन का सामान चढ़ा था उस पर। काफी रोना धोना भी हुआ था। वो लकड़ियाँ अपने साथ ही लाए थे। यहाँ अंदर से कोई नहीं खरीदता और कोई क्यों खरीदे भला इतनी मंहगी जो देता है। मरने वाली औरत बहुत गोरी थी। उसका एक बच्चा भी था वो भी गोद का। एक आदमी जिसके हाथ में बच्चा था वो शायद उसका शोहर था। 9 नम्बर वाले मोक्षस्थल पर जलाने के लिए उसे रखा गया था। उनका अपना क्रियाक्रम का काम चलता रहा और उन्होंने सारे कपड़े और सामान एक तरफ पटक दिया और मृतक को लकड़ियों पर रख दिया गया। अपना सारा काम-वाम निबटाकर वो कुछ देर तो वहीं पर खड़े रहे और थोड़ी देर बाद वहाँ अस्थियों के कमरे के साथ आकर सीटों पर बैठ गए। लगभग दो घंटे वो बैठे रहे फिर एक-एक दो-दो करके वो चले गए मगर वो चिता जलती रही। सब कुछ ठंडा हो जाने की राह देखी जा रही थी जब राख मे से धुआँ और गर्मभाप निकलने लगी तो सारे कपड़े और गहने और सामान उठाने के लिए वहाँ कूड़ा उठाने वाले भागे। शिवराम जी ने उन्हे डाँटा और कहा, "ख़बरदार अगर किसी भी चीज को हाथ लगाया तो ?”
वो उन्हे देखकर पीछे हो गए। पहली बार उनकी आवाज़ निकली थी किसी को रोकने के लिए शायद ये आ गया था उनमे की अब मैं भी इस जगह को सम्भालता हूँ पंडित जी के साथ। शिवराम जी सारा समान उठाकर पंडित जी के घर ले गए। पंडित जी की पत्नी ने देखा और धोती-धोती उठाते हुए कहा, “ये मेरे काम कि है बाकी तू ले जा अपने घर।" हाथों में बाकि सारे कपड़े लेकर वो खड़े रहे और यही सोचते रहे की लेकर जाऊँ या नहीं। कहीं कोई 'हाये' तो साथ मे नहीं चली जायेगी? कोई परेशानी ना बढ़ जाये? नहीं-नहीं क्या करूँ का जाप उनके अन्दर मे घूमने लगा था। फिर भी समानों और चीजों को देखकर सोचा क्यों ना लेकर ही जाया जाये। सारी साड़ियों की तय लगाकर वो एक साफ़ पॉलिथीन में डालकर और मेकपबोक्स अपने हाथों में पकड़े वो अपने घर लेकर चल गए और एक रात के लिए शामशान घाट से गायब हो गए।
अगले दिन पंडिताई ने पहली ही नज़र में उन्हे देख कर कहा, “शिवराम क्या हुआ कैसी लगी साड़ियाँ तेरी औरत को?”
"अरे कहाँ पंडिताई जी सुसरी ने पूरी रात उन साड़ियों को बाहर उसी पॉलिथीन मे दरवाजे के बाहर ही पड़ा रखा कह रही थी की किसी माँगने वाली को दे देगी।"
कहते-कहते वो उसी 9 नम्बर के मोक्षस्थल पर जाकर अस्थियाँ को काले कपड़े मे भरने लगे। ये भरना वैसे हर किसी का नहीं होता पूरे एक दिन तक मरने वाले घरवालों का इन्तजार किया जाता है और जब वो नहीं आते तो खुद ही काले रंग के कपड़े में अस्थियों के फूलों को चूनकर भर लेते हैं और उसपर मोक्षस्थल, टाइम, लिंग लिखकर वहाँ पर अस्थियों के कमरे में टाँग देते हैं। जहाँ पर कई और अस्थियाँ पहले दे ही टगीं हुई हैं थैलियों की शक़्ल में और उनके साथ-साथ में कई कपड़े भी पड़े हैं।
पूरा कमरा काले रंग से भरा हुआ था। बिना पलस्तर के वो ख़ुर्दरी दिवारें बहुत डरावनी लग रही थी। कुछ भी नया नहीं था। कोनों में कई समान भरा और ख़ामोश पड़ा कई आग की भाप निकाल रहा था। लाल चूड़ियाँ, साड़ियाँ, जुतियाँ, मटके, हुक्के के ऊपर का कटोरा, छोटी चारपाइयाँ सभी की सभी कोनों में भरी हुई थी। किसी भी सामान को छूने का मन भी हो तो हाथ नहीं उठते थे। शिवराम जी वहाँ पर कोई खूटीं ढूँढ रहे थे एक और थैली टाँगने के लिए। काले धूँए की आड़ मे गहरा अंधेरा एक जगह की चूप्पी के सन्नाटे को और भी गहरा कर रहा था। कभी तो ये समानों का कमरा लगता तो कभी कई लोगों के शांत रहने का ठिकाना।
सभी सुबह के 11 ही बजे थे तब भी इसका एकान्त कठोर था। जैसे-जैसे रात गहरायेगी तो क्या होगा? शिवराम जी ने वहाँ पर चार और थैलियों के साथ मे उसे टाँगने के लिए जैसे ही डोरी निकाली तो उनकी नज़र उन थैलियों की तारीखों पर गई। चार मे से तीन थैलियाँ 2004 के सितम्बर के महिने की थी और उनके हाथ में लगी थैली 2007 की। वो यही सोचने लगे की यहाँ टाँगने के बाद में भूल गया था तो? यहाँ पर तो धूँए और मिट्टी में सारी थैलियों को सदियों पुराना कर दिया था।
अब वो देखने लगे लगभग सन 2000 और 2007 के मरने वालों की थैलियों को। वो उस कमरे के और अन्दर चले गए। अन्दर कोने की दीवार के साथ मे कई थैलियाँ टँगी थी। ऐसे जैसे किसी ने अपना कोई अनमोल समान याद रखने के लिए टाँगा हो या ऐसे जैसे भूत-प्रेत से बचने के लिए भवूती टाँगी हो।
उन्होंने अंदर की सभी थैलियों को देखा, तारीखें भी छुप गई थी। अपनी उंगलियों से उन्होंने सबकी तारीखें देखी उनपर 1998 , 1999, 1995, 1996, और 2001 लिखा था। देखकर वो वापस आने को हुए और जहाँ तक धूप आ रही थी वहाँ आकर एक लकड़ी ईंटो की दरारी मे फँसाई और अपने हाथ की थैली को वहाँ टाँग दिया। वहाँ खड़े वो पूरे कमरे को देखने लगे उनकी नज़र कमरे में ऐसे घूम रही थी जैसे हर चीज को पढ़ रही हो कोई और रंग ही नहीं था। बस, एक ही या दो ही अंतर थे सभी मे। कोई थैली साड़ी, धोती, या चाकू के साथ टंगी होती तो कोई मोटी या पतली और वो अंदाजा लगाते कि कौन औरत है और कौन मर्द और कौन पतला था और कौन मोटा। पहली बार था कि वो अपने कमरे में।
"कोने में रखी चीजों की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे उस कमरे मे। वो तो किसी ना किसी काम भी आ सकती है और इतना तो पता है कि सन 2000 मे कोई नहीं मरा। अगर कोई मरा है तो कोई यहाँ थैलियों में अकेला टंगा नहीं है। अपना मोक्ष पाने के लिए इतना इंतज़ार कैसे सहेगा कोई ? क्या रिवाज और क्या तारीख? मरने के बाद भी यहाँ अकेला होना क्या फायदा?” वो अपने मे बड़बड़ाते रहे।
जल्दी से जल्दी वो उस थैली को वहाँ टाँग कर बाहर आ गए और पंडित जी के पास जाकर बैठ गए। बहुत बार आऐ हैं यहाँ बल्कि यहाँ पर वो रहे भी हैं। कई लोगों के मरने पर वो इन कुर्सियों पर बैठे भी रहे हैं। सामने रखी ये वही कुर्सी है जो रमेश ने अपने पिता रामचरण के नाम पर यहाँ रखवाई थी। वो 1938 मे पैदा हुए थे और 1992 मे मरे थे। उनके नाम की यहाँ पता है सोने की सीढ़ी भी चड़ाई गई थी क्योंकि वो परदादा से भी ऊपर होकर स्वर्ग सिधारे थे। 3 पीढ़ियाँ देख ली थी उन्होंने। क्या बाजे- गाजे के साथ आए थे। यहाँ पर बैठकर उन चीजों को देखकर यही सब याद आ रहा था उन्हे। पर आज उन कमरे मे रखे सामान को देखकर कुछ भी याद नहीं आ रहा था बस, इतना ही दिमाग मे रहता कि मरने की तारीखों में कोई ना कोई टँगा है। वो पैदा कब हुआ कितनी पीढ़ियाँ देखी होंगी उसने वो कुछ नहीं था। आँखों के आगे वो चीजें ख़ामोश पड़ी थी जो रंगीन तो थी पर किसी की अपनी चीज। गठरियों मे बंधे कपड़े वहाँ पड़े थे और एक टूटी सी चारपाई जो शायद उसी की होगी जो मरा था।
दोपहर का खाना भी आ गया था। पंडिताई जी चावल-भात प्लेट में डाल लाई थी। शिवराम जी अपनी पाँचो उंगलियों को उसमे मिलाते हुए एक गस्सा जैसे ही खाते तो उन्हे उन्ही थैलियों की महक अपनी उंगलियों में महसूस होती। ज़रा सी भी हवा चलती तो पूरे शमशान घाट मे राख ही राख उड़ती नज़र आती और वो उंगलियों को घुमाते-घुमाते चावलों के गस्से पर गस्से खा रहे थे।
इतने में आवाज़ों का काफ़िला अंदर आने लगा। राम नाम सत्य है , सत्य बोलो गद्य है। इसी को दोहराते हुए काफी सारे लोग अंदर आते गए। पहले गाड़ियाँ आई और फिर अर्थी एकदम शांत। आवाज़ें लगाने वाले आगे निकल गए थे। वो आते ही बाहर वहीं कोने पर पानी के नाँद पर रुक गए। दो आदमी अंदर आए और जगह की पूछने लगे।
शिवराम जी प्लेट को नीचे रखते हुए बाहर की तरफ आए और 7 नम्बर वाले मोक्ष स्थल पर ले गए। वहाँ सुबह ही सफ़ाई की गई थी। उन्होंने वहीं अपने क्रियाक्रम का काम शुरू कर दिया और मरने वाले को विदाई देने लगे। मगर यहाँ पर कोई रोने की आवाज़ें नहीं थी। उसके साथ आया सामान जिसपर हमेशा पंडिताई की नज़र रहती थी जैसे नई दुल्हन क्या लाई है उसे देखने की चाह हो।
कोई आदमी था शायद। वहीं गठरी मे कपड़े थे, 4 जोड़ी जयपुरी जूतियाँ थी, आँखों के चश्मे थे और एक कुर्सी भी थी। वो अपने साथ ही लाए थे। सभी लोगों की तरह थोड़ा टाइम देना था और सामानों को वहीं छोड़ जाना था। लोग जब तक आग रहती तब तक वहाँ बनी समाधियों के नाम और तारीखें पढ़ने में लगे रहते और अपना टाइम बिताते। यहाँ पंडिताई और कूड़ा बिनने वालों की निगाह सामानों पर रहती और वहाँ खेलते बच्चों की लुटते खील-बताशो और पैसो पर। यहाँ पर खील-बताशे तो नहीं थे पर अर्थी पर गुब्बारे लगे थे और बैंड वाले भी थे। बच्चे तो गुब्बारों में लग गए और कूड़ा बिनने वाले उन गठरों में बंधे कपड़ो में।
शिवराम जी ने सारा काम करवाया अर्थी के बाँस को ज़मीन मे मारा और खेल ख़त्म। आज पहली बार वो अपने लिए यहाँ से चारों जोड़ी जूतियाँ और कुर्सी लेकर गए थे।
लख्मी
शिवराम जी की भी कुछ यही दिक्कत थी। अक्सर अपना ऑटो वो शमशान घाट के नल से आते पानी से धोया करते थे। सुबह 7 बजे से 8 बजे तक उनका यही काम रहता। इस दौरान शमशान घाट में भी बहुत शांती रहती। बहुत कम बार हुआ था कि इस वक़्त में कोई अर्थी आए। जब भी कभी आती तो वो अपनी सफ़ाई छोड़कर दो कदम उनके कदमों से मिला लेते और दूर से ही नमस्कार कर अपने काम मे वापस लग जाते।
शमशान घाट के पंडितजी के साथ में अच्छी जान-पहचान थी इनकी। शाम में काफी बार 4-5 घंटे साथ बिताए थे। अक्सर शाम में वो वापस आकर अपना ऑटो उसी नल के साथ खड़ा करते और ताला चैन के साथ उसी से बाँध देते। कोई भी शाम ऐसी ना थी जिसमें उन्होंने शमशान घाट में आग ना देखी हो। कभी कोई आग सुलघ रही होती तो कभी बहुत तेज़ उठ रही होती। कभी कोई उस आग के सामने खड़ा दिखता तो कभी वो अपने में एकान्त सुलघती रहती और किसी और के चले जाने का ज्ञात हो जाता।
सुबह और शाम का देखना अब बड़ा हो गया था। ऑटो का सी.एन.जी में तब्दील होना शिवराम जी के लिए तो छोटा ना था। चाहते ना चाहते उनको अपने ऑटो का काम बंद ही करना पड़ा। पूरा दिन बिताना अब आसान नहीं था। 35-40 की उम्र थी और शहर की गुंजाइशें ख़त्म पर थी। वो अपना पूरा दिन शमशान घाट में ही बिताने लगे। कुछ दिन तक वहाँ आते चढ़ावे में उनका हिस्सा रहता। वहाँ पर आए आटा, दाल, चावल, चीनी, और कपड़े और कई वो चीजें जो लोग अपने मर जाने वाले के नाम पर दे जाया करते थे उनको पंडितजी अपने घर में इस्तमाल कर लेते। बस, दोपहर का खाना तो शिवराम जी का वहीं से आ जाता। इस दोपहर के खाने के लिए उनको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता बस, आती हुई अर्थी को खाली जगह दिखाते और शमशान घाट के बनते पर्चे पर पंडितजी के साईन करवाते। यही काम था उनका यहाँ पर जिसकी उन्हे कोई तन्ख्या नहीं मिलती थी।
उनका अभी के दौर में तो घर से मेल-मिलाप नहीं था। वो रात में अक्सर वहीं सो जाया करते। घर के साथ में एक तन्ख्या का रिश्ता था जो अभी टूटा हुआ था। वो वहाँ अगर जाए तो क्या लेकर हाथ तो खाली थे उनके।
बस, अपना दिन बिताने के लिए वहीं मंदिर के पेड़ के नीचे बैठे शमशान घाट में अपनी नज़रे घुमाते रहते। दोपहर में कई लोग वहाँ आकार बैठते और सोते भी थे। अक्सर कूड़ा बिनने वाले बच्चे वहाँ कोनों में लगे रहते और कुछ लोग वहाँ किसी भी समाधी के ऊपर अपने पैर तानकर सो जाते। पेड़ की छाँव के नीचे बहुत शांति मिलती थी यहाँ लोगों को। वैसे यह जगह मशहूर भी शांति के लिए होती है। तो पूरा दिन उन्ही को देखकर उनका टाइम बितता रहा।
काफी टाइम से चल रहा है यह सब। अब तो जिनका कोई मर जाता वो इन्हे जगह दिखाने और चिता जलाने में मदद का कुछ दे भी जाते। वो अपने साथ से अलग से कुछ नहीं लाते हो भले ही पर जो अर्थी पर आता वो तो दिया ही जा सकता था।
एक औरत की अर्थी। बहुत लोग थे। लगता था जैसे कोई जवान और शादीशुदा औरत थी। कई साड़ियाँ चढ़ी थी उसपर। चूड़ियाँ, साड़ियाँ , सैंडिल, मेकप बोक्स, सारी दुल्हन का सामान चढ़ा था उस पर। काफी रोना धोना भी हुआ था। वो लकड़ियाँ अपने साथ ही लाए थे। यहाँ अंदर से कोई नहीं खरीदता और कोई क्यों खरीदे भला इतनी मंहगी जो देता है। मरने वाली औरत बहुत गोरी थी। उसका एक बच्चा भी था वो भी गोद का। एक आदमी जिसके हाथ में बच्चा था वो शायद उसका शोहर था। 9 नम्बर वाले मोक्षस्थल पर जलाने के लिए उसे रखा गया था। उनका अपना क्रियाक्रम का काम चलता रहा और उन्होंने सारे कपड़े और सामान एक तरफ पटक दिया और मृतक को लकड़ियों पर रख दिया गया। अपना सारा काम-वाम निबटाकर वो कुछ देर तो वहीं पर खड़े रहे और थोड़ी देर बाद वहाँ अस्थियों के कमरे के साथ आकर सीटों पर बैठ गए। लगभग दो घंटे वो बैठे रहे फिर एक-एक दो-दो करके वो चले गए मगर वो चिता जलती रही। सब कुछ ठंडा हो जाने की राह देखी जा रही थी जब राख मे से धुआँ और गर्मभाप निकलने लगी तो सारे कपड़े और गहने और सामान उठाने के लिए वहाँ कूड़ा उठाने वाले भागे। शिवराम जी ने उन्हे डाँटा और कहा, "ख़बरदार अगर किसी भी चीज को हाथ लगाया तो ?”
वो उन्हे देखकर पीछे हो गए। पहली बार उनकी आवाज़ निकली थी किसी को रोकने के लिए शायद ये आ गया था उनमे की अब मैं भी इस जगह को सम्भालता हूँ पंडित जी के साथ। शिवराम जी सारा समान उठाकर पंडित जी के घर ले गए। पंडित जी की पत्नी ने देखा और धोती-धोती उठाते हुए कहा, “ये मेरे काम कि है बाकी तू ले जा अपने घर।" हाथों में बाकि सारे कपड़े लेकर वो खड़े रहे और यही सोचते रहे की लेकर जाऊँ या नहीं। कहीं कोई 'हाये' तो साथ मे नहीं चली जायेगी? कोई परेशानी ना बढ़ जाये? नहीं-नहीं क्या करूँ का जाप उनके अन्दर मे घूमने लगा था। फिर भी समानों और चीजों को देखकर सोचा क्यों ना लेकर ही जाया जाये। सारी साड़ियों की तय लगाकर वो एक साफ़ पॉलिथीन में डालकर और मेकपबोक्स अपने हाथों में पकड़े वो अपने घर लेकर चल गए और एक रात के लिए शामशान घाट से गायब हो गए।
अगले दिन पंडिताई ने पहली ही नज़र में उन्हे देख कर कहा, “शिवराम क्या हुआ कैसी लगी साड़ियाँ तेरी औरत को?”
"अरे कहाँ पंडिताई जी सुसरी ने पूरी रात उन साड़ियों को बाहर उसी पॉलिथीन मे दरवाजे के बाहर ही पड़ा रखा कह रही थी की किसी माँगने वाली को दे देगी।"
कहते-कहते वो उसी 9 नम्बर के मोक्षस्थल पर जाकर अस्थियाँ को काले कपड़े मे भरने लगे। ये भरना वैसे हर किसी का नहीं होता पूरे एक दिन तक मरने वाले घरवालों का इन्तजार किया जाता है और जब वो नहीं आते तो खुद ही काले रंग के कपड़े में अस्थियों के फूलों को चूनकर भर लेते हैं और उसपर मोक्षस्थल, टाइम, लिंग लिखकर वहाँ पर अस्थियों के कमरे में टाँग देते हैं। जहाँ पर कई और अस्थियाँ पहले दे ही टगीं हुई हैं थैलियों की शक़्ल में और उनके साथ-साथ में कई कपड़े भी पड़े हैं।
पूरा कमरा काले रंग से भरा हुआ था। बिना पलस्तर के वो ख़ुर्दरी दिवारें बहुत डरावनी लग रही थी। कुछ भी नया नहीं था। कोनों में कई समान भरा और ख़ामोश पड़ा कई आग की भाप निकाल रहा था। लाल चूड़ियाँ, साड़ियाँ, जुतियाँ, मटके, हुक्के के ऊपर का कटोरा, छोटी चारपाइयाँ सभी की सभी कोनों में भरी हुई थी। किसी भी सामान को छूने का मन भी हो तो हाथ नहीं उठते थे। शिवराम जी वहाँ पर कोई खूटीं ढूँढ रहे थे एक और थैली टाँगने के लिए। काले धूँए की आड़ मे गहरा अंधेरा एक जगह की चूप्पी के सन्नाटे को और भी गहरा कर रहा था। कभी तो ये समानों का कमरा लगता तो कभी कई लोगों के शांत रहने का ठिकाना।
सभी सुबह के 11 ही बजे थे तब भी इसका एकान्त कठोर था। जैसे-जैसे रात गहरायेगी तो क्या होगा? शिवराम जी ने वहाँ पर चार और थैलियों के साथ मे उसे टाँगने के लिए जैसे ही डोरी निकाली तो उनकी नज़र उन थैलियों की तारीखों पर गई। चार मे से तीन थैलियाँ 2004 के सितम्बर के महिने की थी और उनके हाथ में लगी थैली 2007 की। वो यही सोचने लगे की यहाँ टाँगने के बाद में भूल गया था तो? यहाँ पर तो धूँए और मिट्टी में सारी थैलियों को सदियों पुराना कर दिया था।
अब वो देखने लगे लगभग सन 2000 और 2007 के मरने वालों की थैलियों को। वो उस कमरे के और अन्दर चले गए। अन्दर कोने की दीवार के साथ मे कई थैलियाँ टँगी थी। ऐसे जैसे किसी ने अपना कोई अनमोल समान याद रखने के लिए टाँगा हो या ऐसे जैसे भूत-प्रेत से बचने के लिए भवूती टाँगी हो।
उन्होंने अंदर की सभी थैलियों को देखा, तारीखें भी छुप गई थी। अपनी उंगलियों से उन्होंने सबकी तारीखें देखी उनपर 1998 , 1999, 1995, 1996, और 2001 लिखा था। देखकर वो वापस आने को हुए और जहाँ तक धूप आ रही थी वहाँ आकर एक लकड़ी ईंटो की दरारी मे फँसाई और अपने हाथ की थैली को वहाँ टाँग दिया। वहाँ खड़े वो पूरे कमरे को देखने लगे उनकी नज़र कमरे में ऐसे घूम रही थी जैसे हर चीज को पढ़ रही हो कोई और रंग ही नहीं था। बस, एक ही या दो ही अंतर थे सभी मे। कोई थैली साड़ी, धोती, या चाकू के साथ टंगी होती तो कोई मोटी या पतली और वो अंदाजा लगाते कि कौन औरत है और कौन मर्द और कौन पतला था और कौन मोटा। पहली बार था कि वो अपने कमरे में।
"कोने में रखी चीजों की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे उस कमरे मे। वो तो किसी ना किसी काम भी आ सकती है और इतना तो पता है कि सन 2000 मे कोई नहीं मरा। अगर कोई मरा है तो कोई यहाँ थैलियों में अकेला टंगा नहीं है। अपना मोक्ष पाने के लिए इतना इंतज़ार कैसे सहेगा कोई ? क्या रिवाज और क्या तारीख? मरने के बाद भी यहाँ अकेला होना क्या फायदा?” वो अपने मे बड़बड़ाते रहे।
जल्दी से जल्दी वो उस थैली को वहाँ टाँग कर बाहर आ गए और पंडित जी के पास जाकर बैठ गए। बहुत बार आऐ हैं यहाँ बल्कि यहाँ पर वो रहे भी हैं। कई लोगों के मरने पर वो इन कुर्सियों पर बैठे भी रहे हैं। सामने रखी ये वही कुर्सी है जो रमेश ने अपने पिता रामचरण के नाम पर यहाँ रखवाई थी। वो 1938 मे पैदा हुए थे और 1992 मे मरे थे। उनके नाम की यहाँ पता है सोने की सीढ़ी भी चड़ाई गई थी क्योंकि वो परदादा से भी ऊपर होकर स्वर्ग सिधारे थे। 3 पीढ़ियाँ देख ली थी उन्होंने। क्या बाजे- गाजे के साथ आए थे। यहाँ पर बैठकर उन चीजों को देखकर यही सब याद आ रहा था उन्हे। पर आज उन कमरे मे रखे सामान को देखकर कुछ भी याद नहीं आ रहा था बस, इतना ही दिमाग मे रहता कि मरने की तारीखों में कोई ना कोई टँगा है। वो पैदा कब हुआ कितनी पीढ़ियाँ देखी होंगी उसने वो कुछ नहीं था। आँखों के आगे वो चीजें ख़ामोश पड़ी थी जो रंगीन तो थी पर किसी की अपनी चीज। गठरियों मे बंधे कपड़े वहाँ पड़े थे और एक टूटी सी चारपाई जो शायद उसी की होगी जो मरा था।
दोपहर का खाना भी आ गया था। पंडिताई जी चावल-भात प्लेट में डाल लाई थी। शिवराम जी अपनी पाँचो उंगलियों को उसमे मिलाते हुए एक गस्सा जैसे ही खाते तो उन्हे उन्ही थैलियों की महक अपनी उंगलियों में महसूस होती। ज़रा सी भी हवा चलती तो पूरे शमशान घाट मे राख ही राख उड़ती नज़र आती और वो उंगलियों को घुमाते-घुमाते चावलों के गस्से पर गस्से खा रहे थे।
इतने में आवाज़ों का काफ़िला अंदर आने लगा। राम नाम सत्य है , सत्य बोलो गद्य है। इसी को दोहराते हुए काफी सारे लोग अंदर आते गए। पहले गाड़ियाँ आई और फिर अर्थी एकदम शांत। आवाज़ें लगाने वाले आगे निकल गए थे। वो आते ही बाहर वहीं कोने पर पानी के नाँद पर रुक गए। दो आदमी अंदर आए और जगह की पूछने लगे।
शिवराम जी प्लेट को नीचे रखते हुए बाहर की तरफ आए और 7 नम्बर वाले मोक्ष स्थल पर ले गए। वहाँ सुबह ही सफ़ाई की गई थी। उन्होंने वहीं अपने क्रियाक्रम का काम शुरू कर दिया और मरने वाले को विदाई देने लगे। मगर यहाँ पर कोई रोने की आवाज़ें नहीं थी। उसके साथ आया सामान जिसपर हमेशा पंडिताई की नज़र रहती थी जैसे नई दुल्हन क्या लाई है उसे देखने की चाह हो।
कोई आदमी था शायद। वहीं गठरी मे कपड़े थे, 4 जोड़ी जयपुरी जूतियाँ थी, आँखों के चश्मे थे और एक कुर्सी भी थी। वो अपने साथ ही लाए थे। सभी लोगों की तरह थोड़ा टाइम देना था और सामानों को वहीं छोड़ जाना था। लोग जब तक आग रहती तब तक वहाँ बनी समाधियों के नाम और तारीखें पढ़ने में लगे रहते और अपना टाइम बिताते। यहाँ पंडिताई और कूड़ा बिनने वालों की निगाह सामानों पर रहती और वहाँ खेलते बच्चों की लुटते खील-बताशो और पैसो पर। यहाँ पर खील-बताशे तो नहीं थे पर अर्थी पर गुब्बारे लगे थे और बैंड वाले भी थे। बच्चे तो गुब्बारों में लग गए और कूड़ा बिनने वाले उन गठरों में बंधे कपड़ो में।
शिवराम जी ने सारा काम करवाया अर्थी के बाँस को ज़मीन मे मारा और खेल ख़त्म। आज पहली बार वो अपने लिए यहाँ से चारों जोड़ी जूतियाँ और कुर्सी लेकर गए थे।
लख्मी
नाचती परछाईयाँ
नये साल का पहला कदम, नये साल कि पहली शुभकामनायें
बीते दिनों को न कभी भूलाया जाता है और न कभी उनसे मुँह मोड़ा जा सकता है। जीवन के खालीपन को यानी रिक़्त स्थान को भरने के लिये उन्हें फिर से दोहराने की जरूरत होती है फिर चाहें वो किसी तरह के वाद-विवाद के हादसे हो या मनोरंजन खुशी के अवसरों का माहौल।
हमारी यादें हमें बहुत तरह से जीने को प्रेरित करती हैं। वो कहती है की जो तुम कर चुके हो उससे जीने का कोई एक अंकुर फूटता है। उसे सींचने का ढ़ग बनाओ जिससे आप को वो अंकुर कभी पेड़ बनकर फल और छाया दे। जब आप अपने साथ कुछ करने के बाद चीजों को दोबारा सोचें तो उसमें फ़र्क करके देखे जिससे पता चले की आप कहाँ तक कमजोर रहे। किस तरह की गलतियाँ आपने की, जो भविष्य में दोहराई न जाये।
ये आपको हर कामयाबी के शिख़र तक ले जाने मे सक्षम होगा। मेरा कुछ ऐसा मानना है। आपकी चेतनाशक्तियाँ आपके अन्दर ही निवास करती हैं। उसे जगाने की आवश्यकता है। जब आप जागोगे तो आप को पता चलेगा की तुम कहाँ-किस गड्डे मे जा गिरे हो और कहाँ फँस गए हो? इस तरह आप अपने विचारों को अपनी मन की शीलता से खुद का वास्तविक रूप देख सकते हो। जो आप के जीवन का सच्चा स्वरूप है।
इस बीते वक़्त मे हमने कई काम अधूरे छोड़े हैं और कई बार चालाकी से खुद के लिए आसान रास्ते बनाये हैं। किसी का दिल दुखाया तो किसी को हँसाया है। इसी को तो कहते है,"दर्दे डिस्कों।"
जीवन चक्र में न जाने क्या-क्या न उलझ गया, जिससे हम जीनें का साफ़-सुथरा ढ़ग ही भूल गए। बस, याद रहा तो अपनी खुशी और अपना मज़ा। जहाँ एक तरफ ये सफ़र हादसों और घटनाक्रमों से गुज़रा। वही कहीं हमने अपने लिए अपनी ज़िन्दगी से क्या सीखा। ये समझना भी तो जरूरी है।
भगती-दौड़ती इस शहरी ज़िन्दगानी मे विकास एक मह्तवपूर्ण कड़ी है जिससे बसेरों के निमार्ण और खासी जगहों का निर्माण उसके साथ-साथ व्यवस्थित ढ़ग से जीने की प्रथा तो आई है। मगर भीड़ से भरे स्थानों में वही खीचा-तानी, वही हो-हल्ला मचता दिखाई देता। जिसे आज भी जब बीती हुई ज़िन्दगी याद करती है तो वो बेपरवाह शहर मे ख़ामोशी के बीच डरावना नाच नाचती परछाईयाँ तो शरीर के तमाम तारों को झिंजोड़कर रख देती है। जब रोजाना मे कई तबको के शख़्सों को हम घूमते-फिरते देखते हैं। उनकी हालात को देखकर ही खाया-पिया मुँह को आ जाता है। जीना क्या है? ये सवाल को हम बड़ा आसान बना देते हैं। हमारे दैनिक जीवन मे भी कई वो शख़्स जुड़े होते हैं जो हमें नहीं जानते और जिन्हों से हम भी अंजान हैं। लेकिन शहर की हवा में हम मिलकर सांस लेते हैं। जैसे ठन्ड के मौसम में आग की गर्माहट सब को ही चाहिये ही होती है और उसी मौसम मे एक धुंए की तरह अफ़वाहें उड़ती हैं और शहर के हर चप्पे-चप्पे मे समा जाती हैं। अफ़वाहें हमारी अपनी होती हैं पर वो बनती दूसरों के लिए हैं। रहस्यमय आलम बनाने के लिए। जिसके सम्पर्क मे आने वाला शख़्स अपनी आँखों पर भी भरोसा नहीं करता और वो कहीं किसी घटना का शिकार हो जाता है।
मेरे मन की ये किस्सागोही मेरे लिए बीते दिनों को याद करने की गुंजाइश है। लेकिन मैं अगले कदम पर लेकर क्या जाऊँ? क्या इन्ही को लेकर चलता बनू? या फिर किसी और ही दुनिया की उम्मीद लगाऊँ? ये तो बीते कुछ ऐसे विवरण हैं जिन्हे कब तक मैं अपने मे समाता चलूँ? क्या इससे कुछ नया ले पाऊँगा मैं?
ये तो गया, दर्दे डिस्कों भी हो गया। अब इस बीते कणों मे विदा कैसे किया जाये? क्या कोई नई जगह बनाई जायें या फिर पुरानी को ताज़ा किया जायें?
राकेश
बीते दिनों को न कभी भूलाया जाता है और न कभी उनसे मुँह मोड़ा जा सकता है। जीवन के खालीपन को यानी रिक़्त स्थान को भरने के लिये उन्हें फिर से दोहराने की जरूरत होती है फिर चाहें वो किसी तरह के वाद-विवाद के हादसे हो या मनोरंजन खुशी के अवसरों का माहौल।
हमारी यादें हमें बहुत तरह से जीने को प्रेरित करती हैं। वो कहती है की जो तुम कर चुके हो उससे जीने का कोई एक अंकुर फूटता है। उसे सींचने का ढ़ग बनाओ जिससे आप को वो अंकुर कभी पेड़ बनकर फल और छाया दे। जब आप अपने साथ कुछ करने के बाद चीजों को दोबारा सोचें तो उसमें फ़र्क करके देखे जिससे पता चले की आप कहाँ तक कमजोर रहे। किस तरह की गलतियाँ आपने की, जो भविष्य में दोहराई न जाये।
ये आपको हर कामयाबी के शिख़र तक ले जाने मे सक्षम होगा। मेरा कुछ ऐसा मानना है। आपकी चेतनाशक्तियाँ आपके अन्दर ही निवास करती हैं। उसे जगाने की आवश्यकता है। जब आप जागोगे तो आप को पता चलेगा की तुम कहाँ-किस गड्डे मे जा गिरे हो और कहाँ फँस गए हो? इस तरह आप अपने विचारों को अपनी मन की शीलता से खुद का वास्तविक रूप देख सकते हो। जो आप के जीवन का सच्चा स्वरूप है।
इस बीते वक़्त मे हमने कई काम अधूरे छोड़े हैं और कई बार चालाकी से खुद के लिए आसान रास्ते बनाये हैं। किसी का दिल दुखाया तो किसी को हँसाया है। इसी को तो कहते है,"दर्दे डिस्कों।"
जीवन चक्र में न जाने क्या-क्या न उलझ गया, जिससे हम जीनें का साफ़-सुथरा ढ़ग ही भूल गए। बस, याद रहा तो अपनी खुशी और अपना मज़ा। जहाँ एक तरफ ये सफ़र हादसों और घटनाक्रमों से गुज़रा। वही कहीं हमने अपने लिए अपनी ज़िन्दगी से क्या सीखा। ये समझना भी तो जरूरी है।
भगती-दौड़ती इस शहरी ज़िन्दगानी मे विकास एक मह्तवपूर्ण कड़ी है जिससे बसेरों के निमार्ण और खासी जगहों का निर्माण उसके साथ-साथ व्यवस्थित ढ़ग से जीने की प्रथा तो आई है। मगर भीड़ से भरे स्थानों में वही खीचा-तानी, वही हो-हल्ला मचता दिखाई देता। जिसे आज भी जब बीती हुई ज़िन्दगी याद करती है तो वो बेपरवाह शहर मे ख़ामोशी के बीच डरावना नाच नाचती परछाईयाँ तो शरीर के तमाम तारों को झिंजोड़कर रख देती है। जब रोजाना मे कई तबको के शख़्सों को हम घूमते-फिरते देखते हैं। उनकी हालात को देखकर ही खाया-पिया मुँह को आ जाता है। जीना क्या है? ये सवाल को हम बड़ा आसान बना देते हैं। हमारे दैनिक जीवन मे भी कई वो शख़्स जुड़े होते हैं जो हमें नहीं जानते और जिन्हों से हम भी अंजान हैं। लेकिन शहर की हवा में हम मिलकर सांस लेते हैं। जैसे ठन्ड के मौसम में आग की गर्माहट सब को ही चाहिये ही होती है और उसी मौसम मे एक धुंए की तरह अफ़वाहें उड़ती हैं और शहर के हर चप्पे-चप्पे मे समा जाती हैं। अफ़वाहें हमारी अपनी होती हैं पर वो बनती दूसरों के लिए हैं। रहस्यमय आलम बनाने के लिए। जिसके सम्पर्क मे आने वाला शख़्स अपनी आँखों पर भी भरोसा नहीं करता और वो कहीं किसी घटना का शिकार हो जाता है।
मेरे मन की ये किस्सागोही मेरे लिए बीते दिनों को याद करने की गुंजाइश है। लेकिन मैं अगले कदम पर लेकर क्या जाऊँ? क्या इन्ही को लेकर चलता बनू? या फिर किसी और ही दुनिया की उम्मीद लगाऊँ? ये तो बीते कुछ ऐसे विवरण हैं जिन्हे कब तक मैं अपने मे समाता चलूँ? क्या इससे कुछ नया ले पाऊँगा मैं?
ये तो गया, दर्दे डिस्कों भी हो गया। अब इस बीते कणों मे विदा कैसे किया जाये? क्या कोई नई जगह बनाई जायें या फिर पुरानी को ताज़ा किया जायें?
राकेश
बस, वक़्त मरहम है
कितनी जल्दी चीजें हमसे छूटती जाती हैं और हम उन चीजों को पल भर भी अपने से दूर जाने का वियोग नहीं करते। कुछ वियोग दिल को तस्ल्ली नहीं दे पाते हैं तो उनको ज़ुबान पर लाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। शायद यही बात है। वक़्त को हम इस तरह से जीते आए हैं कि वो कोई मरहम है। जो हमारी छूटी गई चीजों या बुनियादों के घावों को भर देगा। बस, कदमों को खिसकाते चलते हैं। आखिरकार कुछ पा ही जायेंगे।
जीवन को जिन कल्पनाओं और रचनाओं से बनाया था। जिस वक़्त की वो रहनवाज़ बनी उसमे वो रचनाओं भरा जीवन कई नये पैमानों का हकदार बनता है। अपने उसी वक़्त को एक खुशी में महसूस किया जाता रहा है। मगर डर रहता है उस खुशी के किनारों से। जिसमे उस खुशी के जाहिर होने की छवि कहीं नज़र नहीं आती। ऐसा बिलकुल नहीं है की उसका दम नहीं है उसके किनारों पर, बहुत दम है। जो खेल और नाच के कोनों पर खड़े उसे हर पैतरें को या नाच के हर स्टैप को देखकर कोई बात अपने से मुँह से निकालते आए हैं। अगर वो ही कहीं खो जाये तो भी गम नहीं देता। बस, वो वक़्त के चकक्कर मे कहीं ठहर जाता है। क्यों वो कल्पनाये कोई वज़न नहीं ले पाती उस दौर मे जब हम अपने परिवार और पहचान के दस्तावेज़ बना रहे होते हैं? क्यों वो रचनाये कोई आकार नहीं ले पाती उस वक़्त के पन्नों मे? इतना आसान क्यों होता है उनका लुप्त जो जाना और वो एक दम से ही किसी ख़ास दिनचर्या में अपना अक्श क्यों नहीं दिखा पाती?
बस वक़्त मरहम है।
वक़्त जिसमें हमारी पहचान अलग-अलग तरह से ही उभर आई है। कभी वो हमारी अन्दर की कल्पनाओं से अपनी तस्वीर बनाती है तो कभी अपने से जुड़े रिस्तों से। वक़्त जिसमे उभरना, भूलना, पाना और जूझना हर पैमाने में पर चलता है। कभी हमें देखकर हमें दर्शाया गया है तो कभी हमें सुनकर। इन दोनों परिस्थितियों मे हमारी कोई ना कोई छवि तैयार ही हो रही होती है। जो कभी अपनी कल्पनाओं से जाने जाते थे वो आज अपने काम और रिस्तों से अपनी तस्वीरें बनाते हैं।
ये एक बदलाव है - एक गहरा बदलाव।
इसमे परिवर्तित होना किसी आम शख़्स की किस ओर की दुनिया को बनाने की कोशिश में है? क्या घवराहट नहीं होती इस बदलाव को जानकर? उस आम शख़्स को उसकी कल्पनाओं को शहर मे किस छवि के जरिये उतारा जायेगा?
"वक़्त कैसे बदला वो हमें मालूम नहीं मगर इतना मालूम है की लोगों की और परिवार की नज़रों ने हमें बदलने पर मजबूर कर दिया।"
ये कहकर वो अपनी चूप्पी को साध गए। कहीं और के हो गए।
"एक वक़्त था जब झूमकर नाचने पर इतनी वाह-वाही मिलती थी कि उन्हे समेटना मुश्किल होता था और आज वो जो भी समेट पाये थे उसे भी खर्च करने मे डर लगता है।"
उन्हे देखकर कोई ये अन्दाजा भी नहीं लगा सकेगा की ये वो शख़्स हैं जो कभी महफ़िलों की शान हुआ करते थे। जिसके एक गीत की लाइन कई लोगों को गीतों के अन्तरे के शब्द दे दिया करती थी। जिसमें लोग रात-रात भर महफ़िलों में मदहोस होकर अपने मे और धूनों में डूब जाया करते थे। बस, एक ही आलम हुआ करता था नशे का। जिसमे ढोलक पर पहली बार चल रहे हाथ भी ऐसे लगते थे की जैसे कई पैरों में मैखाने का नशा भर देते होगें। कोई ना नाचने वाला भी अपने पैरों को उठाने लगता होगा और जोश ही जोश में झूम भी जाया करता होगा।
आज भी उनके होठों से निकलने वाली बातों मे इन्ही महफ़िलों की चाँदनियों को अपने इर्द-गिर्द महसूस किया जा सकता है। मन मे बस, एक इच्छा सी जाग उठती थी कि काश मैं भी होता उन महफ़िलों में और झूम रहा होता। हर सुनने वाले की ज़ूबान पर ये आ ही जाता था की क्या वो महफ़िलें दोबारा नहीं आ सकती?
तो वो बस, उसकी तरफ में देखकर हँस जाया करते और इस कदर बेगाने हो जाते है उस बात से की वो कोई किसी ख़त्म होती नाटकिये लीला का गिरा हुआ परदा हो। बस, ये ही अदा उनकी उन्हे वो सारी चाँदनियाँ भूल जाने में सहयोग देती थी। जो वो अक्सर वहाँ उन सवालों या बातों से हट जाने में सफ़ल हो जाया करते।
लम्बे-तगड़े और शॉल औड़े वो गली के कोने पर खड़े आती जाती सड़क को ताकते रहते हैं और कोई ना कोई उनकी बातों मे लीन जरूर होता है। ज़्यादातर उनके छोटे भाई पिछली रात मे गाए गए गीत या किसी थाप की कसे होने को लेकर बात कर रहे होते।
ये ही अकेले हैं इनके हमसफ़र जिनके साथ मे कई रातों मे बिताए वो पल याद हैं। जिनको ये आज भी गीतों के ज़रिये दोहराते रहते हैं। बस, शाम चलते ही ये दूनिया अपने इशारे लिए अपनी चाँदनियों भरी दूनिया ने चले जाते। कोई भी रात ऐसी नहीं गुज़रती जिसमें ये फ़नकर अपना फ़न ना दिखाए सोते भी हो। बस, अब जगह तलाश्नी नहीं पड़ती वो तो चुनली गई है। मगर इस चुनी हुई जगह में वो बात कहाँ? वो रस़ कहाँ? जो अंधेरा होते ही आँखों पर छा जाया करता था। जिसके एक-एक घूँट में कई गीतों की मदहोसी बयाँ होती।
अब तो ये दूनिया एक कोने में खिलते उस रात की रानी के उस फूल की तरह हो गई है। जो रात मे खिलता है, महकता है, हवा में झूमता है, चाँदनी को ताकता है और सुबह का सूरज देखते ही अपना दम तोड़ देता है। इसके बावज़ूद भी इसमे जीने की उम्मीद कम नहीं होती। वो और, और, और भी गहरी होती जाती है।
काश की इन महफ़िलों में जीने वालों की उम्र कभी बढ़ती ही नहीं। वो रात की रानी के फूल की ही तरह से हर रात मे खिलते, महकते, हवा में झूमते, चाँदनी को ताकते और सुबह होते ही वापस डूब जाते और दूसरी रात फिर से एक और ताज़ी महक लिए खिलते। काश के ऐसा होता हो कितना मज़ा आता।
ये काश के सपने दिखाती दूनिया अब कब अपनी रोनक दिखायेगी वो तो तय नहीं किया गया है और कौन तय करेगा ये भी जाहिर नहीं हुआ है। इसी दूनिया के है वो "सज्जन जी" जो तैर रहे हैं।
"सज्जन जी" की दूनिया भी इसी काश की ओड़नी ओड़ चूकी है। अपनी जगह भी चून चूकी है। जगह है अपनी ही गली के किनारे के मकान की सातवीं मन्जिल। जहाँ तक किसी की आँख नहीं पँहुचती और फ़नकार के खिलते फूल को कोई भी नज़र नहीं लगा सकता। वहाँ पर "सज्जन जी" अपने अन्दर दबी कला को अपने से बाहर लाते हैं। एक ऐसी दूनिया में खो जाते हैं जहाँ पर सारे रिश्ते-नाते अपनी ज़िन्दगी के सारे पल्लुयों को छोड़ देते हैं। आदमी को कहीं उड़ने के लिए।
"सज्जन जी" के भाई ढोलक की थाप पर थाप पिटते जाते हैं और ये मदहोसी के सारे नियमों को तोड़ जाते हैं। नियमों में पड़ी अपनी उम्र को जो आज पचास से पच्पन साल की सीढ़ी चड़ चूकी है उसे पायदान पर ले आते हैं। अपने नृत्य के हर स्टैप को जीते हैं। जिसमें लगने वाला हर ठुमका आदमी या औरत की पुष्टी नहीं करता बस, किसी भी फ़नकार के शरीर मे थिरकन ले आता है जिससे वो झूमने लगता है।
"सज्जन जी" की ज़िन्दगी मे बदलाव कोई झटके से नहीं आया। ये बदलाव हल्के-हल्के वक़्त मे जमा। आज वो अपनी उम्र को अपनी ज़िन्दगी का सबसे बड़ा और गहरा बदलाव का ज़रिया मानते हैं। जो अलग-अलग तरह की ज़ुबानों में प्रस्तृत होता आया है। जिसमें उनकी कला और अपनी मदहोसी सब इस बदलाव मे सबसे ज़्यादा शतिग्रहस्त होने वाली दूनिया थी।
कुछ ऐसे नाम थे जो इस शतिग्रहस्त बदलाव मे उभर गए। 'नचकईया, गवईया, मशख़रा जैसे। ये वो पहचान बने जिनको साथ मे लेकर चलना इनके परिवार के बस मे नहीं था। ये नाम ही कलाओं के लिए एक अभिशाप की भांति पैदा हुए। शायद इन अभिशापो से आने वाली दूनिया 'काश' जैसे परदो मे रची जायेगी।
ये कुछ अन्दाजन नहीं था। मगर "सज्जन जी" का अन्दाजा इसी से विरोध मे रहा। जहाँ पर रची जाने वाली दूनिया अपने कोने में ही इतनी गतिशील थी के वो उस सातवीं मन्जिल को हमारे और आपके सामने किन्ही शब्दों में उभार देती है।
ये जगहे हमारे लिए कुछ गहरे सवाल छोड़ती है और उन्ही सवालों में जीती भी है। जहाँ पर गीत और मदहोसी एक-दूसरे को बिना किसी बटन के सर्च करते है और वो सामने हाज़िर हो जाती है। वो सातवीं मन्जिल आज भी तैयार है।
लख्मी
जीवन को जिन कल्पनाओं और रचनाओं से बनाया था। जिस वक़्त की वो रहनवाज़ बनी उसमे वो रचनाओं भरा जीवन कई नये पैमानों का हकदार बनता है। अपने उसी वक़्त को एक खुशी में महसूस किया जाता रहा है। मगर डर रहता है उस खुशी के किनारों से। जिसमे उस खुशी के जाहिर होने की छवि कहीं नज़र नहीं आती। ऐसा बिलकुल नहीं है की उसका दम नहीं है उसके किनारों पर, बहुत दम है। जो खेल और नाच के कोनों पर खड़े उसे हर पैतरें को या नाच के हर स्टैप को देखकर कोई बात अपने से मुँह से निकालते आए हैं। अगर वो ही कहीं खो जाये तो भी गम नहीं देता। बस, वो वक़्त के चकक्कर मे कहीं ठहर जाता है। क्यों वो कल्पनाये कोई वज़न नहीं ले पाती उस दौर मे जब हम अपने परिवार और पहचान के दस्तावेज़ बना रहे होते हैं? क्यों वो रचनाये कोई आकार नहीं ले पाती उस वक़्त के पन्नों मे? इतना आसान क्यों होता है उनका लुप्त जो जाना और वो एक दम से ही किसी ख़ास दिनचर्या में अपना अक्श क्यों नहीं दिखा पाती?
बस वक़्त मरहम है।
वक़्त जिसमें हमारी पहचान अलग-अलग तरह से ही उभर आई है। कभी वो हमारी अन्दर की कल्पनाओं से अपनी तस्वीर बनाती है तो कभी अपने से जुड़े रिस्तों से। वक़्त जिसमे उभरना, भूलना, पाना और जूझना हर पैमाने में पर चलता है। कभी हमें देखकर हमें दर्शाया गया है तो कभी हमें सुनकर। इन दोनों परिस्थितियों मे हमारी कोई ना कोई छवि तैयार ही हो रही होती है। जो कभी अपनी कल्पनाओं से जाने जाते थे वो आज अपने काम और रिस्तों से अपनी तस्वीरें बनाते हैं।
ये एक बदलाव है - एक गहरा बदलाव।
इसमे परिवर्तित होना किसी आम शख़्स की किस ओर की दुनिया को बनाने की कोशिश में है? क्या घवराहट नहीं होती इस बदलाव को जानकर? उस आम शख़्स को उसकी कल्पनाओं को शहर मे किस छवि के जरिये उतारा जायेगा?
"वक़्त कैसे बदला वो हमें मालूम नहीं मगर इतना मालूम है की लोगों की और परिवार की नज़रों ने हमें बदलने पर मजबूर कर दिया।"
ये कहकर वो अपनी चूप्पी को साध गए। कहीं और के हो गए।
"एक वक़्त था जब झूमकर नाचने पर इतनी वाह-वाही मिलती थी कि उन्हे समेटना मुश्किल होता था और आज वो जो भी समेट पाये थे उसे भी खर्च करने मे डर लगता है।"
उन्हे देखकर कोई ये अन्दाजा भी नहीं लगा सकेगा की ये वो शख़्स हैं जो कभी महफ़िलों की शान हुआ करते थे। जिसके एक गीत की लाइन कई लोगों को गीतों के अन्तरे के शब्द दे दिया करती थी। जिसमें लोग रात-रात भर महफ़िलों में मदहोस होकर अपने मे और धूनों में डूब जाया करते थे। बस, एक ही आलम हुआ करता था नशे का। जिसमे ढोलक पर पहली बार चल रहे हाथ भी ऐसे लगते थे की जैसे कई पैरों में मैखाने का नशा भर देते होगें। कोई ना नाचने वाला भी अपने पैरों को उठाने लगता होगा और जोश ही जोश में झूम भी जाया करता होगा।
आज भी उनके होठों से निकलने वाली बातों मे इन्ही महफ़िलों की चाँदनियों को अपने इर्द-गिर्द महसूस किया जा सकता है। मन मे बस, एक इच्छा सी जाग उठती थी कि काश मैं भी होता उन महफ़िलों में और झूम रहा होता। हर सुनने वाले की ज़ूबान पर ये आ ही जाता था की क्या वो महफ़िलें दोबारा नहीं आ सकती?
तो वो बस, उसकी तरफ में देखकर हँस जाया करते और इस कदर बेगाने हो जाते है उस बात से की वो कोई किसी ख़त्म होती नाटकिये लीला का गिरा हुआ परदा हो। बस, ये ही अदा उनकी उन्हे वो सारी चाँदनियाँ भूल जाने में सहयोग देती थी। जो वो अक्सर वहाँ उन सवालों या बातों से हट जाने में सफ़ल हो जाया करते।
लम्बे-तगड़े और शॉल औड़े वो गली के कोने पर खड़े आती जाती सड़क को ताकते रहते हैं और कोई ना कोई उनकी बातों मे लीन जरूर होता है। ज़्यादातर उनके छोटे भाई पिछली रात मे गाए गए गीत या किसी थाप की कसे होने को लेकर बात कर रहे होते।
ये ही अकेले हैं इनके हमसफ़र जिनके साथ मे कई रातों मे बिताए वो पल याद हैं। जिनको ये आज भी गीतों के ज़रिये दोहराते रहते हैं। बस, शाम चलते ही ये दूनिया अपने इशारे लिए अपनी चाँदनियों भरी दूनिया ने चले जाते। कोई भी रात ऐसी नहीं गुज़रती जिसमें ये फ़नकर अपना फ़न ना दिखाए सोते भी हो। बस, अब जगह तलाश्नी नहीं पड़ती वो तो चुनली गई है। मगर इस चुनी हुई जगह में वो बात कहाँ? वो रस़ कहाँ? जो अंधेरा होते ही आँखों पर छा जाया करता था। जिसके एक-एक घूँट में कई गीतों की मदहोसी बयाँ होती।
अब तो ये दूनिया एक कोने में खिलते उस रात की रानी के उस फूल की तरह हो गई है। जो रात मे खिलता है, महकता है, हवा में झूमता है, चाँदनी को ताकता है और सुबह का सूरज देखते ही अपना दम तोड़ देता है। इसके बावज़ूद भी इसमे जीने की उम्मीद कम नहीं होती। वो और, और, और भी गहरी होती जाती है।
काश की इन महफ़िलों में जीने वालों की उम्र कभी बढ़ती ही नहीं। वो रात की रानी के फूल की ही तरह से हर रात मे खिलते, महकते, हवा में झूमते, चाँदनी को ताकते और सुबह होते ही वापस डूब जाते और दूसरी रात फिर से एक और ताज़ी महक लिए खिलते। काश के ऐसा होता हो कितना मज़ा आता।
ये काश के सपने दिखाती दूनिया अब कब अपनी रोनक दिखायेगी वो तो तय नहीं किया गया है और कौन तय करेगा ये भी जाहिर नहीं हुआ है। इसी दूनिया के है वो "सज्जन जी" जो तैर रहे हैं।
"सज्जन जी" की दूनिया भी इसी काश की ओड़नी ओड़ चूकी है। अपनी जगह भी चून चूकी है। जगह है अपनी ही गली के किनारे के मकान की सातवीं मन्जिल। जहाँ तक किसी की आँख नहीं पँहुचती और फ़नकार के खिलते फूल को कोई भी नज़र नहीं लगा सकता। वहाँ पर "सज्जन जी" अपने अन्दर दबी कला को अपने से बाहर लाते हैं। एक ऐसी दूनिया में खो जाते हैं जहाँ पर सारे रिश्ते-नाते अपनी ज़िन्दगी के सारे पल्लुयों को छोड़ देते हैं। आदमी को कहीं उड़ने के लिए।
"सज्जन जी" के भाई ढोलक की थाप पर थाप पिटते जाते हैं और ये मदहोसी के सारे नियमों को तोड़ जाते हैं। नियमों में पड़ी अपनी उम्र को जो आज पचास से पच्पन साल की सीढ़ी चड़ चूकी है उसे पायदान पर ले आते हैं। अपने नृत्य के हर स्टैप को जीते हैं। जिसमें लगने वाला हर ठुमका आदमी या औरत की पुष्टी नहीं करता बस, किसी भी फ़नकार के शरीर मे थिरकन ले आता है जिससे वो झूमने लगता है।
"सज्जन जी" की ज़िन्दगी मे बदलाव कोई झटके से नहीं आया। ये बदलाव हल्के-हल्के वक़्त मे जमा। आज वो अपनी उम्र को अपनी ज़िन्दगी का सबसे बड़ा और गहरा बदलाव का ज़रिया मानते हैं। जो अलग-अलग तरह की ज़ुबानों में प्रस्तृत होता आया है। जिसमें उनकी कला और अपनी मदहोसी सब इस बदलाव मे सबसे ज़्यादा शतिग्रहस्त होने वाली दूनिया थी।
कुछ ऐसे नाम थे जो इस शतिग्रहस्त बदलाव मे उभर गए। 'नचकईया, गवईया, मशख़रा जैसे। ये वो पहचान बने जिनको साथ मे लेकर चलना इनके परिवार के बस मे नहीं था। ये नाम ही कलाओं के लिए एक अभिशाप की भांति पैदा हुए। शायद इन अभिशापो से आने वाली दूनिया 'काश' जैसे परदो मे रची जायेगी।
ये कुछ अन्दाजन नहीं था। मगर "सज्जन जी" का अन्दाजा इसी से विरोध मे रहा। जहाँ पर रची जाने वाली दूनिया अपने कोने में ही इतनी गतिशील थी के वो उस सातवीं मन्जिल को हमारे और आपके सामने किन्ही शब्दों में उभार देती है।
ये जगहे हमारे लिए कुछ गहरे सवाल छोड़ती है और उन्ही सवालों में जीती भी है। जहाँ पर गीत और मदहोसी एक-दूसरे को बिना किसी बटन के सर्च करते है और वो सामने हाज़िर हो जाती है। वो सातवीं मन्जिल आज भी तैयार है।
लख्मी
Subscribe to:
Posts (Atom)